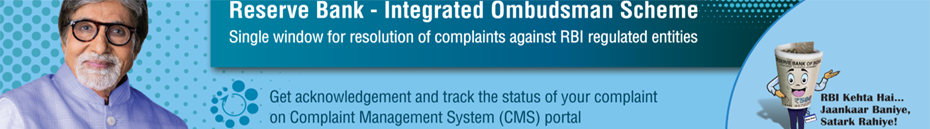भारतीय मनीषा ने मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में काम को भी स्थान दिया है, परंतु इसे पश्चिम की तरह स्वच्छंदता की मान्यता नहीं दी। काम प्राकृतिक रूप में जीवन से अभिन्न है। इसलिए इसका दमन करके कोई छुटकारा नहीं पा सकता। जो लोग अपने को आजीवन ब्रह्मïचारी कहते हैं, वे या तो नपुंसक होते हैं या वे अपने को और समाज को धोखा दे रहे होते हैं। ब्रह्मïचर्य का अर्थ केवल दैहिक संभोग से विरत रहना नहीं है। काम का मानसिक चिन्तन करने वाले को भी हम ब्रह्मïचारी नहीं कह सकते। अत: पूर्ण ब्रह्मïचर्य तो एक कोरी कल्पना है। हां, धीरे- धीरे काम के माध्यम से ही काम को वश में अवश्य किया जा सकता है। जब यौवनावस्था में काम का उद्दाम वेग होता है, तब नारी पुरुष की और पुरुष नारी की कामना करने लगता है। यदि यह संयोग नहीं हो पाता तो वह कृत्रिम रूप में काम-तृप्ति करता है। उसके मन में काम इस प्रकार छा जाता है कि वह स्वप्न में भी यौन-क्रिया अचेतन रूप में करने लगता है।
पहले यौन-तृप्ति के कृत्रिम साधन एक पक्षीय होने से यौन-क्रिया में वह आनंद नहीं मिल पाता था जो सजीव स्त्री- पुरुष के संभोग में होता है, परंतु अब स्त्री और पुरुष के ऐसे कृत्रिम विग्रह बन गए हैं, जो सजीव स्पर्श-सुख न देते हुए भी यौन- क्रिया में लगभग वैसे ही आनंद की अनुभूति कराते हैं, जैसी सजीव स्त्री-पुरुष के बीच होती है। इससे स्त्री की पुरुष पर और पुरुष की स्त्री पर यौन निर्भरता कम हो गयी है, परंतु चेतन और अचेतन का जो अंतर है, उसे भला कौन मिटा सकता है। इसलिए नारी और पुरुष का आकर्षण एवं उनका संयोग अनिवार्य बन जाता है।
भारत में काम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने के लिए चार आश्रमों की व्यवस्था की गयी और गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठï बताया गया। इसमें स्त्री और पुरुष यौवनावस्था में विवाह करके काम-तृप्ति से निश्चिंत हो जाते हैं और समाज, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा करते हैं। अपने जीवन-यापन और देह-धर्म का पालन ही मनुष्यत्व नहीं है। इसलिए कहा गया है –
आहार, निद्रा, भय मैथुनं च सामान्य एतत्ï पशुर्भिराणाम्ï।
धर्मोति तेषाम्ïअधिको विशेषो, धर्मेण हीन: पशुभि: समान:॥
पशुओं से मनुष्य को अलग करने वाला उसका धर्म है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात्ï देह-धर्म का पालन तो पशु भी करते हैं। मनुष्य को पशु से अलग करने वाला धर्म क्या है? यह मानव-धर्म है, जिसमें उदात्त वृत्तियां, करणीय कर्म, चरित्र और त्याग को महत्व दिया जाता है। इसमें अपने से अधिक समाज, राष्ट्र और मानवता को वरेण्य माना जाता है। बड़े हित के लिए छोटे हित का त्याग ‘महाभारत’ में इस प्रकार वर्णित है –
त्यज्द्देकं कुलस्वार्थे ग्रामस्वार्थो कुलं त्यजेत।
ग्रामं जनपदस्वार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत॥
उपनिषद् भी इसी धारणा की पुष्टि करते है। त्याग करके भोग करना अर्थात् अनासक्त होकर संसार में रहना, जीवन धारण करना और करणीय कर्म करना प्रकृति और निवृत्ति के समन्वय का यह आदर्श ही मानव-जीवन को सार्थक बनाने में समर्थ है।
बिना काम-क्रिया के अनुभव के अपने को ब्रह्मïचारी, योगी या संन्यासी घोषित करने वाला पाखण्डी होता है। बड़े-बड़े महापुरुष जिनको हम ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं, जो योगेश्वर और सांसारिक सुखों से निर्मित थे, जिन्होंने राष्टï्र और मानवता की महान सेवा की, उनमें भी कामेच्छा सहज रूप में विïद्यमान थी। पुष्पवाटिका में जब राम-सीता के आभूषणों की ध्वनि सुनकर उन्हें देखते हैं, तब उनके मन में काम की हलचल होने लगती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है –
कंकण किंकिंण नूपुर ध्वनि सुनि, कहत लखन सम राम हृदय गुनि।
मानहुं मदन दुंदुभी दीन्हीं, मनसा विस्व विजय कहं कीन्हीं।
तात जनक तनया यह सोई, धनुष जज्ञ जेहि कारन होई॥
राम ने सीता से विवाह किया, परंतु वे काम से बंधे नहीं। वे राष्ट्र-हित के लिए सब कुछ त्याग कर वनवास के लिए तैयार हो गए। यह बात दूसरी है कि सीता के हठ के कारण वे सीता को भी साथ ले गये। यह सीता का अधिकार भी था, जिसकी उपेक्षा वे नहीं कर सकते थे। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। उन्होंने गोपियों के साथ रास भी किया और बाद में विवाह भी किया। अपनी प्रियतमा राधा की काम-तृप्ति के संबंध में सूरदास ने सुरति का वर्णन किया है –
हरषि पिय तिय अंग लीन्हीं।
उलट धरि भुजभि भरि सुरति रति पूरि अति निबल कीन्हीं॥
कृष्ण ने दैहिक और मानसिक क्रिया से राधा की यौनेच्छा को अत्यंत क्षीण कर दिया, क्योंकि काम को कोई समूल नष्ट नहीं कर सकता। बीज अथवा कारण में ही जो सूक्ष्म शरीर छिपा रहता है, उसी में काम भी विद्यमान रहता है। इसलिए वह आजीवन और जन्म-जन्मान्तर तक रहता है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि कोई प्रेतात्मा किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में सवार होकर संभोग करके चली जाती है। इसका स्त्री और पुरुष को अहसास भर होता है। योगी भी अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करके उसके द्वारा यौन-क्रिया करके अपने शरीर में वापस आ सकता है। कृष्ण का ऐसा ही खेल था। वे काम से बंधे नहीं थे और संसार से भी अनासक्त थे। इसलिए ब्रज छोडऩे के बाद वे वहां वापस नहीं लौटे। मथुरा से भी वे दूर चले गए और राष्ट्र-हित में किसी का भी वध करने या करवाने से नहीं चूके। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। गांधीजी ने काम का दामन न छोड़ते हुए भी अनासक्त भाव से राष्ट्र की सेवा की।
भारत में लाखों की संख्या में साधु-संन्यासी हैं। इन्होंने काम को अपने वश में कर लिया हो या न कर सकने के बावजूद वश में करने का पाखण्ड कर रहे हों, परंतु इनसे समाज, राष्ट्र और मानवता का क्या हित होता है? ये अपने मोक्ष के लिए अपने देह-धर्म का पालन करते हैं, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो समष्टि या विराट चेतना में विलय से होती है। ‘स्व’ या ‘अहं’ मिटाना पड़ता है। सृष्टि के सभी प्राणियों में वही आत्मा है, जो उसमें है, ऐसा भाव होने पर ही यह अहं समाप्त होता है। ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ के रूप में मानकर कोई समाज, राष्ट्र, मानवता एवं समष्टि से निरपेक्ष कैसे रह सकता है? यह बात ठीक है कि वह स्वयं अनासक्त हो, परंतु सबके हित-साधन में ही उसकी मुक्ति संभव है। पूजा-पाठ, व्रत, स्नान, भजन, तप आदि तो केवल अहं के विसर्जन और विराट परमात्मा को समझने के साधन मात्र हैं। कोई व्यक्ति, कोई पुराण की कथा करवाकर या मंदिर में नित्य आरती करके मोक्ष नहीं पा सकता। प्रवचनों से मुक्ति नहीं मिलती। वे सब साधन मात्र हैं।
काम के मोह को क्षीण करके ये विराट चेतना की ओर ले जाते हैं। भक्ति में भी काम का भाव रहता है। काम भक्ति की बाधा नहीं है। संभोग से समाधि तक का दर्शन इसी से उत्पन्न हुआ है। बस उचित सामंजस्य की आवश्यकता है।