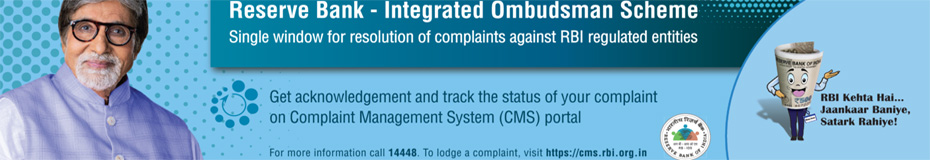निरंतर लागत बढ़ती चले जाने से हमारे देश में खेती संकट के दौर से गुजर रही है। एक ओर खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली आदि का खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान की आय सिमटती जा रही है। जलवायु संकट के दौर में अनिश्चित मौसम और कीटनाशकों के बढ़ते प्रकोप ने भी खेती के संकट को बढ़ा दिया है। देश के विभिन्न भागों के वह किसान चर्चा में हैं, जो पारंपरिक देसी बीजों को अपना कर नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। क्या बदहाल खेती के दौर में पारंपरिक देसी बीजों के जरिए हालात को बदला जा सकता है, इस प्रश्न पर आज चर्चा हो रही है। बड़ा सवाल है कि क्या पारंपरिक देसी बीज खेती में नई क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं?
खेती में बीजों की गुणवत्ता का मुद्दा बहुत बड़ा है। नकली एवं अमानक बीजों के कारण किसानों को जिस तरह नुकसान झेलना पड़ रहा है, वह चिंता का विषय है। सरकार भी नया बीज कानून लाने की कवायद में जुटी है। इसी बीच पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल और संरक्षण कर रहे किसानों की कहानियां विकल्प सुझा रही हैं। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की एक आदिवासी बस्ती की निवासी 27 वर्षीय लहरी बाई अपने छोटे से घर में 150 से अधिक दुर्लभ और विलुप्त प्राय देसी बीजों को सहेज रही हैं। लहरी बाई ये बीज स्थानीय हाटों और आसपास के किसानों से एकत्र करती हैं। फिर उन्हें साफ करके, सुखाकर, सुरक्षित रखती हैं और जरूरत पडऩे पर दूसरे किसानों को दे देती हैं। यह कोई सरकारी परियोजना नहीं है, न ही इसके पीछे कोई बड़ी फंडिंग है। यह काम भरोसे और जरूरत से चलता है। इस महिला के लिए बीज केवल खेती का साधन नहीं बल्कि जीवन का भरोसा हैं। उनके लिए बीज केवल फसल का जरिया नहीं है बल्कि संस्कृति, स्वाद और आत्म निर्भरता भी है।
लहरी बाई को ‘मिलेट वुमन’ या ‘मिलेट एम्बेसडर’ कहा जाता है लेकिन असल में वे उस ज्ञान की प्रतिनिधि हैं जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में लगभग भुला दिया है। इस पारंपरिक ज्ञान के जानकार बीज को खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं बल्कि साझा धरोहर मानते थे। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग पंजाब के बरनाला जिले के वाहेगुरुपुरा गांव में किसान अमृत चहल कर रहे हैं। अमृत देसी बीज और प्राकृतिक खेती पर आधारित एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जो यह दिखाता है कि पारंपरिक बीज केवल भावनात्मक या अतीत से जुड़ा विषय नहीं हैं बल्कि आज के समय में भी वह आर्थिक रूप से टिकाऊ हो सकता है। सहकारी ज्ञान और मार्केटिंग के सहारे उन्होंने यह साबित किया है कि किसान केवल खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं है बल्कि अपनी मिट्टी, अपने बीज और अपने बाजार का मालिक भी बन सकता है। उन्होंने कुछ लोगों को स्थाई रोजगार दिया है जो इस बात का संकेत है कि देसी बीजों पर आधारित खेती आजीविका का भी ठोस आधार बन सकती है। इस किसान ने 2023 में बेंगलुरू की एक संस्था के सहयोग से देसी बीज बैंक की स्थापना की। इस बीज बैंक में केवल अनाज ही नहीं हैं बल्कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, शलगम, मूली, घीया, तोरी आदि सब्जियों के साथ-साथ गेहूं, धान, बाजरा, मक्की और हरे चारे के पुराने देसी बीज भी संरक्षित हैं। कुल मिलाकर 35-40 फसलों की लगभग 150 किस्मों के बीज उनके यहां मौजूद हैं जो फसल विविधता की याद दिलाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी खेती कभी एकरूप नहीं थी। हर इलाके, हर मौसम और हर समाज के अनुसार उसकी अपनी पहचान थी। आज कृषि वैज्ञानिक जिस फसल विविधता पर जोर देते हैं, हमारे पुरखे उसे स्वाभाविक रूप से अपनाए हुए थे।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासी इलाकों में बीज संरक्षण की यह पहचान आज भी जीवित है। वहां की आदिवासी महिलाएं फसल के सबसे अच्छे और पहले पकने वाले दानों को चिन्हित करती हैं। कभी उन पर राखी बांध दी जाती है, कभी उन्हें अलग कपड़े में सुरक्षित रखा जाता है ताकि कटाई के समय उनकी अलग से पहचान संभव हो सके। सहेज कर रखे गए यही दाने अगले मौसम के बीज बनते हैं। देसी मक्का, बाजरा, और रागी जैसे छोटे अनाज बांसवाड़ा के आदिवासियों के लिए केवल फसल नहीं बल्कि जीवन की रीढ़ हैं। यह ज्ञान पीढिय़ों के अनुभव से उपजा है। ऐसे और भी उदाहरण हैं।
इन तमाम उदाहरणों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पारंपरिक बीजों के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब हरित क्रांति के बाद अपनाए गए कृषि मॉडल में मिलता है। उच्च उत्पादक किस्मों और संकर बीजों ने पैदावार तो बढ़ाई लेकिन इसके साथ खेती को रासायनिक खाद, कीटनाशकों और बाजार के ‘मानक बीजों’ से बांध दिया। इससे धीरे-धीरे फसल विविधता सिमटती चली गई और किसान बीज कंपनियों पर निर्भर होता गया।
संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1900 के बाद से दुनिया भर में खेती में इस्तेमाल होने वाली लगभग 75 फीसद फसल विविधता समाप्त हो चुकी है। भारत में भी तस्वीर इससे अलग नहीं है। आज देश की लगभग 60 फीसद कृषि भूमि पर केवल धान, गेहूं और मक्का जैसी चंद फसलें हावी हैं। यह एकरूपता खेती को जितना सरल दिखाती है, उतना ही असुरक्षित भी बनाती है। इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ा है। देश में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि आज किसान की कुल लागत का 35-40 फीसद हिस्सा केवल बीज, खाद और कीटनाशकों पर खर्च हो जाता है। इससे जाहिर है कि फसल बोने से पहले ही किसान की मेहनत का बड़ा हिस्सा बाजार के हवाले हो चुका होता है। अगर ऐसे में बीज नकली या अप्रमाणिक निकल जाएं तो पूरी फसल ही दांव पर लग जाती है। कई राज्यों में नकली बीजों के कारण 20-30 प्रतिशत तक फसल नुकसान की शिकायतें सामने आती रही हैं।
कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या पारंपरिक बीज कोई चमत्कारी समाधान दे सकते हैं। इसका सीधा जवाब है-नहीं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पारंपरिक बीज खेती को कम जोखिम वाला और अधिक आत्म निर्भर बना सकते हैं। ये बीज स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुरूप विकसित हुए हैं, इसलिए सूखा, कम वर्षा या कीट प्रकोप जैसी परिस्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर टिकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि किसान इन्हें सहेज सकता है जिससे बीज पर होने वाला खर्च लगभग समाप्त हो जाता है। कीट प्रकोप कम होने से रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता घटती है और सीधे तौर पर खेती की कुल लागत में कमी आती है।
पारंपरिक बीजों से खेती करना हमारे पुरखों की पहचान रही है लेकिन हरित क्रांति के दौर में यह मान लिया गया कि देसी बीज कम उत्पादन देते हैं। इसी सोच ने खेती को केवल प्रति एकड़ पैदावार के चश्मे से देखने की आदत डाली जबकि असली सवाल यह है कि कम लागत, कम जोखिम और अनिश्चित मौसम में खेती कितनी टिकाऊ है। इसी कसौटी पर पारंपरिक बीज आज भी प्रासंगिक साबित होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मोटे अनाज कम पानी में उग जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। आज जब पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, तब यह बात और ज्यादा अहम हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 60 प्रतिशत खेती बारिश पर निर्भर है। धान जैसी के उत्पादनों में बहुत ज्यादा पानी लगता है जबकि बाजरा और ज्वार जैसे देसी अनाज बहुत कम पानी में भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए पारंपरिक बीज केवल खेती का तरीका नहीं हैं बल्कि पानी बचाने का उपाय भी हैं। इन्हें इसी रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। सरकार ने भी हाल के वर्षों में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी बहुत कम है। राजस्थान देश का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला प्रदेश है लेकिन यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोग बाजरे को स्वीकार नहीं कर रहे। जहां बाजरे का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, वहीं इसे आहार में शामिल करने की भी आवश्यकता है। सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला है। धरातल पर परिवर्तन तभी संभव है,जब स्थानीय पारंपरिक बीजों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
पारंपरिक देसी बीजों की बात केवल खेती या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। पारंपरिक बीजों का मुद्दा खेती के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। नए-नए और मानक कहे जाने वाले बीजों के साथ फसल की अनिश्चितता जुड़ी है जबकि पारंपरिक बीज निश्चित उत्पादन देते आए हैं। निश्चित उत्पादन होगा तो खाद्य सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्त हुआ जा सकता है। देश में पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल और संरक्षण कर रहे किसान सिर्फ बीज नहीं बचा रहे, वह ऐसा करके भविष्य को बचाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने और उनकी बात को देश भर के किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। सरकारों, वैज्ञानिकों, किसान संगठनों और आम लोगों को सामूहिक रूप से देसी बीजों की प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि पारंपरिक बीजों को गुजरे जमाने की चीज न मानकर भविष्य की जरूरत समझा जाए। अगर बीज बचेंगे तो ही लोग बचेंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है।
अमरपाल सिंह वर्मा