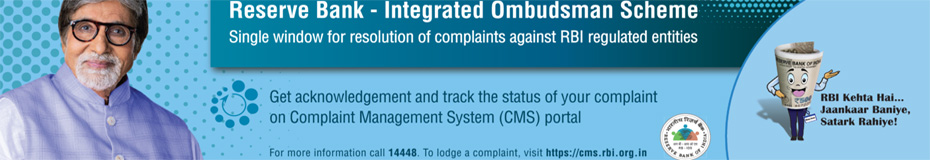राष्ट्रीय स्मारक: विरासत का सम्मान या वैचारिक वर्चस्व की जंग?
Focus News 31 December 2025 0
दो दिन पहले लखनऊ में 25 दिसंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण किया तो यह केवल एक भव्य इमारत का उद्घाटन नहीं था। यह उस निरंतर चल रहे ‘स्मृति-युद्ध’ (Memory War) का एक और अध्याय था, जो पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति के केंद्र में है। 65 एकड़ में फैला और लगभग 320 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्मारक परिसर सत्ताधारी दल के लिए अपनी वैचारिक जड़ों को सींचने का स्थान हो सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र के सामने कुछ गंभीर और मौलिक प्रश्न भी छोड़ता है। क्या हमारे राष्ट्रनायकों का सम्मान अब केवल उनके ‘कद’ पर नहीं बल्कि मौजूदा सत्ता के साथ उनकी ‘वैचारिक ट्यूनिंग’ पर निर्भर करेगा?
भव्यता का अर्थशास्त्र और सादगी का अंत
इस स्मारक ने वित्तीय पैमानों पर भी एक नई बहस छेड़ी है। सबसे पहला और सीधा सवाल इसके आर्थिक पैमाने को लेकर है। भाजपा अक्सर पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर मायावती और कांग्रेस पर ‘मूर्तियों और स्मारकों’ के नाम पर जनता की कमाई लुटाने का आरोप लगाती रही है लेकिन लखनऊ का यह ‘प्रेरणा स्थल’ उसी राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है।
यदि हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो एक चौंकाने वाला अंतर नजर आता है। दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि 1948-1951 के बीच मात्र 10 लाख रुपये में बनी थी जिसकी आज की मुद्रास्फीति के हिसाब से कीमत लगभग 10-12 करोड़ रुपये बैठती है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का ‘शांतिवन’ और इंदिरा गांधी का ‘शक्तिस्थल’ भी तत्कालीन समय में बेहद सीमित खर्च और अत्यधिक सादगी के साथ बनाए गए थे। ये स्मारक केवल पत्थर के ढेर नहीं थे बल्कि उस कालखंड की सादगी और राष्ट्र निर्माण के प्रति गंभीरता के प्रतीक थे। इसके विपरीत अकेले करीब 65 एकड़ में फैले लखनऊ के इस परिसर पर 320 करोड़ रुपये खर्च करना क्या वाकई न्यायोचित है? जब देश महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा हो, तब क्या अटल जी जैसे सादगी पसंद नेता के लिए कंक्रीट का यह भव्य महल बनाना उनके ही सिद्धांतों के साथ न्याय है? स्पष्ट है कि स्मारक निर्माण के बजट और भव्यता के पैमाने बदल गए हैं।
‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ और नेहरू की विरासत का प्रश्न
यही प्रवृत्ति हमें दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में भी दिखाई देती है। ‘नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी’ (NMML) को बदलकर ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ (PMML) करने का फैसला केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं था। नेहरू, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक थे, उनके ऐतिहासिक निवास को एक सामान्य गैलरी में बदल देना उनकी विशिष्ट विरासत को धुंधला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय में अपनी भी एक गैलरी सुरक्षित कर ली है। इतिहास हमेशा किसी व्यक्तित्व के विदा होने के बाद उसकी समीक्षा करता है और फिर उसे स्मारक में स्थान मिलता है लेकिन जीवित रहते हुए ही खुद का स्मारक बनवाना एक ऐसी परिपाटी है जो लोकतंत्र से ज्यादा व्यक्ति-पूजा की ओर संकेत करती है। क्या सत्ता को यह डर है कि भविष्य में आने वाली सरकारें उनकी स्मृतियों को वह स्थान नहीं देंगी जो वे आज खुद तय कर रहे हैं?
चयनात्मक स्मृति: कौन अपना, कौन पराया?
प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण में ‘सबका सम्मान’ करने का दावा किया और कांग्रेस पर ‘परिवारवाद’ का आरोप लगाया लेकिन जब हम ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ को देखते हैं, तो वहां केवल भाजपा की वैचारिक त्रिमूर्ति—वाजपेयी, मुखर्जी और उपाध्याय—नजर आते हैं। यदि यह वाकई ‘राष्ट्र’ का प्रेरणा स्थल है तो इसमें उत्तर प्रदेश की धरती से निकले अन्य महापुरुषों जैसे राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या वीपी सिंह, कांशी राम, मुलायम सिंह आदि को स्थान क्यों नहीं मिला? क्या नेहरू-गांधी परिवार को कोसते हुए हम खुद भी उसी ‘चयनात्मक राजनीति’ का शिकार नहीं हो रहे हैं? फिर तो इसे राष्ट्र का प्रेरणा स्थल नहीं, भाजपा का प्रेरणा स्थल कहा जाना चाहिए।
भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल मुरली मनोहर जोशी का योगदान भी कम नहीं है लेकिन उनकी उपस्थिति इन प्रतीकों में कहीं नहीं दिखती। यह स्पष्ट करता है कि इन स्मारकों का उद्देश्य श्रद्धा कम और राजनीतिक संदेश देना ज्यादा है।
डॉ. मनमोहन सिंह और स्मारक का नया ‘ट्रस्ट मॉडल’
दोहरा मापदंड तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के प्रति दिखाए गए व्यवहार की तुलना करते हैं। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट (एक सामान्य श्मशान) पर किया गया जबकि परंपरा के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए दिल्ली में विशेष समाधि स्थल आवंटित होते रहे हैं। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाने के लिए भूमि एक ट्रस्ट को आवंटित की जाएगी हालाँकि, इस स्मारक निर्माण के लिए अब तक कोई विशेष केंद्रीय बजट आवंटन सार्वजनिक नहीं हुआ है और ये पहले के सीधे सरकारी निर्माण के मॉडल से भिन्न है।
यहाँ सवाल यह है कि वाजपेयी जी या अन्य नायकों के लिए सैकड़ों करोड़ का सरकारी बजट, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए ‘निजी ट्रस्ट’ का रास्ता क्यों? क्या यह एक मूक संदेश नहीं है कि जो नायक हमारी विचारधारा के सांचे में फिट नहीं बैठते, उनके सम्मान की जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं, बल्कि उनके समर्थकों या निजी संस्थाओं की होगी?
विचारधारा का अंतर्विरोध
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय भाजपा की नींव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन क्या वर्तमान भाजपा वाकई उनके सिद्धांतों पर चल रही है? मुखर्जी ने ‘एक देश, दो विधान’ की बात की थी लेकिन आज भी पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग झंडे और पहचान की मांगें सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने ‘समग्र मानववाद’ का दर्शन दिया, जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सम्मान और समावेशी समाज की वकालत करता है लेकिन जब सत्ताधारी दल के मंचों से ‘बंटोगे तो कटोगे’ जैसे विभाजनकारी नारे उछाले जाते हैं, तो उपाध्याय जी का ‘एकात्म मानववाद’ कहीं कोने में खड़ा सिसकता हुआ महसूस होता है।
एक राष्ट्रीय नीति की अनिवार्य आवश्यकता
इन विसंगतियों का समाधान केवल एक ही है—एक पारदर्शी ‘राष्ट्रीय स्मारक नीति’।
अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं: संस्थागत बनाम राजनीतिक
विकसित लोकतंत्रों में इस तरह के स्मृति-स्थलों का निर्माण अक्सर स्पष्ट कानूनी ढांचे में होता है। उदाहरण के लिए,दुनिया के कई विकसित लोकतंत्रों में स्मारकों का निर्माण किसी प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं, बल्कि एक तय कानून के तहत होता है।
· अमेरिकी मॉडल: वहां ‘प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एक्ट, 1955’ है। हर राष्ट्रपति के लिए एक लाइब्रेरी बनती है, जिसका निर्माण निजी फंड से होता है और बाद में उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार संभालता है। वहां कोई भी राष्ट्रपति खुद की गैलरी सरकारी खर्चे पर नहीं बनवाता।
· भारतीय आवश्यकता: भारत को भी एक ऐसी बहुदलीय समिति की आवश्यकता है जो यह तय करे कि किस नेता का स्मारक कहां, कितनी लागत में और कितनी जमीन पर बनेगा। इसमें विपक्ष की राय अनिवार्य होनी चाहिए ताकि स्मारक ‘दलगत अखाड़े’ के बजाय ‘राष्ट्रीय एकता’ के प्रतीक बन सकें।
अंततः, स्मारक पत्थरों से नहीं, उन महापुरुषों के विचारों से जीवंत होते हैं। यदि हम भव्य प्रतिमाएं तो खड़ी कर लें लेकिन उनके विचारों को अपनी राजनीति में जगह न दें तो ये 320 करोड़ के परिसर केवल कंक्रीट के ढांचे बनकर रह जाएंगे। एक परिपक्व लोकतंत्र वही है जो अपने नायकों को विचारधारा के चश्मे से नहीं, बल्कि उनके राष्ट्र के प्रति योगदान के चश्मे से देखे। ये सभी घटनाएँ एक बड़े सत्य की ओर इशारा करती हैं: भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के चयन, निर्माण, वित्तपोषण और रखरखाव के लिए कोई समग्र, पारदर्शी और बहुदलीय सहमति से बनी राष्ट्रीय नीति नहीं है। जब तक ऐसी नीति नहीं बनेगी जो स्पष्ट मानदंड तय करे, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करे और एक बहु-दलीय समिति के जरिए निर्णय ले, तब तक ये स्मारक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कम और दलगत राजनीति के नए अखाड़े अधिक बनते रहेंगे। एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान यह है कि वह अपने सभी योगदानकर्ताओं को, उनकी विचारधारा से परे, गरिमामय ढंग से याद करने का एक संस्थागत तरीका विकसित करे।
ओंकारेश्वर पांडेय
ओंकारेश्वर पांडेय वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के संपादक रहे हैं और सामयिक विषयों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं।