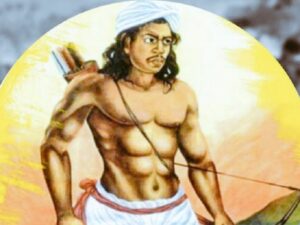मोहन मंगलम
बाबू बालमुकुंद गुप्त खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। राष्ट्रीय नवजागरण एवं साहित्य-सृजन में वे काफी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्यादा समृद्ध नहीं थी, लेकिन स्वाध्याय, चिंतन और अनुभव के बल पर वे कई अखबारों में संपादक रहे और अपने संपादकीय लेखों तथा चर्चित स्तंभ ‘शिवशंभु का चिट्ठा’ के माध्यम से अपने समय के सर्वाधिक कद्दावर पत्रकार के रूप में स्थापित हो गए।
बालमुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवम्बर 1865 को तत्कालीन पंजाब के रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियानी में हुआ था। उनके पिता का नाम पूरनमल गोयल था। बालमुकुंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी लिपि सीखी।
प्रारम्भिक शिक्षार्जन के बाद उनका सम्पर्क झज्जर की संस्था ‘रिफाहे आम सोसाइटी’ के साथ हुआ। यह संस्था समस्यापूर्ति का केन्द्र स्थल थी। गुप्त जी भी समस्यापूर्ति करने लगे और शनै: शनै: उर्दू में काव्य रचना की ओर बढ़े।
बालमुकुन्द गुप्त ने उर्दू पत्रकारिता से शुरुआत की। वे ‘रिफाहे आम’ अखबार और उर्दू मासिक ‘मथुरा समाचार’ में दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहे थे। उसके बाद वे चुनार के उर्दू अखबार ‘अखबारे चुनार’ के दो वर्ष संपादक रहे। 1888-1889 में लाहौर के उर्दू पत्र ‘कोहेनूर’ का संपादन किया। उन्होंने प्रतापनारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी के पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपना काव्यगुरु स्वीकार किया। गुप्त जी ने अपने घर गुड़ियानी में रहकर मुरादाबाद के ‘भारत प्रताप’ उर्दू मासिक का संपादन किया और इस बीच अंग्रेजी का अध्ययन करते रहे। 1893 में ‘हिंदी बंगवासी’ के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए और छह वर्ष तक काम किया। 1899 में ‘भारत मित्र’ कलकत्ता के वे संपादक भी रहे थे। वे ‘हिन्दी बंगवासी’ और ‘भारत मित्र’ को बुलन्दियों पर लेकर गए।
बाबू बालमुकुन्द गुप्त के पास राष्ट्रवादी-जनवादी पत्रकार की पैनी दृष्टि थी और कवि का संवेदनशील हृदय। इससे वे जनता के दु:ख-तकलीफों को महसूस कर सके और उन्हें निर्भीकता से व्यक्त भी किया। उन्होंने अपनी कविताओं में तत्कालीन राजनीतिक सवालों को उठाया। उनकी कविताओं का स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, वे जनता की भावनाओं को शब्द प्रदान करती थीं और देशभक्तों में नई ऊर्जा का संचार करती थीं। उन्होंने तत्कालीन जनता की हीनभावना को यथासम्भव दूर करने का प्रयास किया। उनकी कविताओं में किसानों के शोषण की प्रक्रियाओं का जैसा वर्णन है, उसके दर्शन महान कथाकार प्रेमचन्द के कथा साहित्य में होते हैं।
समूचे भारत के मानस के चितेरे बाबू बालमुकुंद गुप्त में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपने निबन्धों के द्वारा तत्कालीन भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल देशभक्ति की भावना पर ही बल नहीं दिया बल्कि व्यंग्यात्मक शैली द्वारा ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों पर भी प्रहार किया। वे सम्पूर्ण भारतवर्ष को स्वतन्त्र देखना चाहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश शासक कभी भी भारतवासियों का भला नहीं कर सकते। उनका विचार था कि देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ सामाजिक जागरण भी नितान्त आवश्यक है। वे अपने लेखों में समाज को सुधारने की बात पर भी बल देते थे। उन्होंने नारी सुधार पर बल दिया और सामाजिक कुरीतियों पर करारे व्यंग्य किए।
गुप्त जी के साहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। वे गांधी के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि सिद्धान्तों में पूर्ण विश्वास करते थे। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि हमें विदेशी माल को ठुकराकर स्वदेशी माल का प्रयोग करना चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की पैरोकारी करते हुए अपनी कविता ‘आशीर्वाद’ में वे लिखते भी हैं- “
“अपना बोया आप ही खावें, अपना कपड़ा आप बनावें।
बढ़े सदा अपना व्यापार, चारों दिस हो मौज बहार।
माल विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावें।
कभी न भारत हो मुँहताज, सदा रहे टेसू का राज”
बालमुकुन्द गुप्त ने सहज, सरल एवं व्यावहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। वस्तुतः उनकी भाषा तत्कालीन हिन्दी भाषा है। उनके निबन्धों में उर्दू तथा सामान्य बोलचाल वाले शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है फिर भी उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। उन्हें लोकगीतों से विशेष प्रेम था और उन्हीं की तर्ज पर उन्होंने तीखी राजनीतिक कविताएं लिखी थीं। अपनी निर्भीकता से उन्होंने दूसरों में यह मनोबल उत्पन्न किया कि वे भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बोलें।
बालमुकुन्द गुप्त ने हिन्दी के उत्थान में विशेष योगदान दिया। वे जनभाषा के पक्षधर थे। उन्होंने जनभाषा को साहित्य में अपनाने पर जोर दिया। इसी कारण से उनकी कविताओं में विभिन्न भाषाओं के शब्द धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं। उनका ध्यान भाषा की सजावट पर उतना नहीं था, जितना कि संप्रेषण पर। संप्रेषण ही उनकी भाषा की कसौटी थी। उन्होंने हिन्दी कविता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा और जनता की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कविता की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य व पद्य के विकास में भरपूर योगदान दिया।
कलकत्ता की जलवायु तथा काम की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जलवायु बदलने के लिए वे तत्कालीन बिहार में वैद्यनाथ धाम भी गए, परन्तु स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण वे गुड़ियानी के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने पर उनके सम्बन्धियों ने इलाज के लिए रोक लिया। कई वैद्यों ने इलाज के प्रयास किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 18 सितम्बर, 1907 को महज 42 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। आज भी जब देश की पत्रकारिता, हिन्दी भाषा के उन्नयन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्ने पलटें तो लगेगा बाबू बालमुकुंद गुप्त के जिक्र के बिना यह इतिहास अधूरा है।