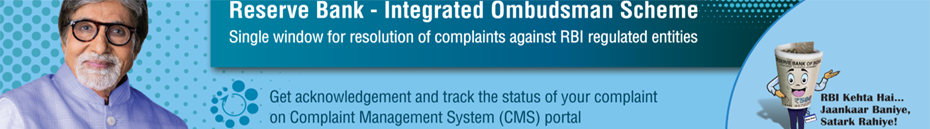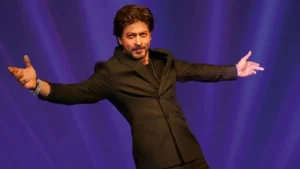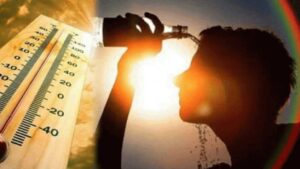हमारे देश में हजारों सालों से परंपरागत स्वदेशी ज्ञान की अविरल धारा बहती आ रही है। हमारे पुरखों ने कृषि, औषधि, वास्तु, हस्तशिल्प, योग और पर्यावरण संतुलन जैसे विविध क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान विकसित किया था, वह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। यदि मौजूदा संदर्भ में इन परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाए तो इससे बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। स्वदेशी ज्ञान के जरिए हम आत्म निर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
भारत की परंपरागत तकनीकों में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग करने की गहरी समझ है। अतीत में यह ज्ञान न केवल हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता रहा है बल्कि सतत विकास को भी सुनिश्चित करता आया है। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जाना पड़ता। यह ज्ञान अपने गांव में या गांव के आसपास ही सहज रूप से मिल जाता है।
स्वदेशी ज्ञान का अर्थ सीमित नहीं है बल्कि यह व्यापक रूप लिए हुए है। इसमें पारंपरिक कौशल के साथ-साथ पुरखों के अनुभवों का निचोड़ शामिल है जो लोगों को छोटी उम्र से ही विभिन्न काम-धंधों में हुनरमंद बना देता है। हमारे समाज में बर्तन निर्माण, खेती, भवन निर्माण, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण, खाना बनाना, खिलौने बनाना, अचार-मुरब्बे बनाना, पारंपरिक औषधियों का निर्माण, वास्तु कला, और हस्तशिल्प जैसे उद्योग-धंधे परंपरागत ज्ञान से ही विकसित हुए हैं। हम सदियों से इस ज्ञान के माध्यम से जल से ऊर्जा उत्पादन कर आ रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी इसी ज्ञान पर आधारित रहा है।
प्राचीन समय में इसी ज्ञान पर आधारित काम-धंधों के बूते पर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। हमारा देश ‘सोने की चिडिय़ा’ कहलाता था। औपनिवेशिक शासकों और विदेशी आक्रांताओं ने न केवल हमारी धन सम्पदा को लूटा बल्कि हमारे कुटीर उद्योग भी खत्म कर दिए। आजादी के बाद स्वदेशी ज्ञान आधारित काम धंधों को पनपाने के लिए अपेक्षित काम नहीं किया गया, जिससे पारंपरिक काम धंधे खत्म हो रहे हैं। इसका परिणाम बढ़ती बेरोजगारी और लोगों की घटती आमदनी के रूप में सामने आ रहा है।
एक ओर जहां आजादी के बाद हमने अपनी ज्ञान परंपराओं को बिसरा दिया, वहीं चीन ने अपने यहां की ऐसी ही परंपराओं के बल पर पांव पसारे और दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। चीन ने जहां बढ़ती आबादी पर रोक लगाई, वहीं अपने लोगों को पारंपरिक ज्ञान के आधार पर काम धंधों में जुटने के लिए प्रेरित किया। 1980 में चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल कर आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय चीन की प्रति व्यक्ति आय 307 डॉलर और भारत की प्रति व्यक्ति 580 डॉलर थी। इसके विपरीत, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई और स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, संसाधन कम पड़ गए और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई। 2024 के आंकड़ों के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग 12,500 अमेरिकी डॉलर है जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2500 अमेरिकी डॉलर ही है। यह अंतर दर्शाता है कि भारत को परंपरागत ज्ञान को पुनर्जीवित करने की कितनी आवश्यकता है।
अगर हम इन परंपराओं को अपनाए रखते तो उनमें छिपा अनुभवों का खजाना हमारी नई पीढिय़ों तक पहुंचता रहता लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इन परंपराओं को अपना कर जहां हम समाज में स्थिरता बनाए रख सकते हैं वहीं इसकी बदौलत आर्थिक विकास को भी पंख लग सकते हैं। समय की मांग है कि हम अपने स्वदेशी ज्ञान और आर्थिक विकास के अन्तर्सम्बंधों पर दृष्टिपात करें।
हमारा ये ज्ञान सदियों से आजमाया हुआ समाज की सामूहिक सहभागिता पर आधारित ऐसा सिस्टम है, जो आज भी स्थानीय जरूरतों पर खरा है। यह सिस्टम न केवल संबंधित भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय की जरूरतों के अनुकूल होता है बल्कि इसका स्वरूप स्थानीय पर्यावरण एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप भी तय होता है। सतत विकास के लिए बनाए इस सिस्टम में हमेशा से प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को प्राथमिकता दी जाती रही है।
हमने अपने को आधुनिक बनाने की होड़ में अपनी हर चीज को रूढि़वादी बताकर तज दिया है. इसमें हमारा ये ज्ञान भी है। अब वक्त है हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। यह ज्ञान पुराना हो सकता है मगर अनुपयोगी नहीं। अगर उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए कहीं जरूरत लगती है तो हमें पारंपरिक ज्ञान में नूतन तकनीकी ज्ञान को मिला लेना चाहिए। इससे हमारी आय और उत्पादन वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। पर्यावरण पर से दबाव घटेगा। अगर हम पहले की तरह पारंपरिक बीजों, गोबर खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी खेती फिर से लाभकारी हो जाएगी क्योंकि खेती पर लागत घटेगी और किसानों के लाभ में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ-साथ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी इस ज्ञान को अंगीकार करे। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस विषय को पढ़ाया जा सकता है। हस्तशिल्प और कृषि आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
औद्योगिकीकरण के चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढऩे से समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरत लोगों को उनके गांव में ही काम देने की है। उदाहरण के रूप में साइकिल के कारखाने लुधियाना में हैं तो वे लुधियाना में ही सबको काम दे रहे हैं। अगर ऐसे सभी उद्योग अपनी जरूरत के पार्ट्स बनाने के लिए गांवों में छोटी-छोटी इकाइयां स्थापित कर दें तो लोगों को गांवों में ही काम मिलेगा, वे खुशहाल होंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी विकास के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। इससे पलायन रुकेगा और शहरों पर दबाव कम होगा।
यह ज्ञान जहां लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। यह सराहनीय है कि मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें आयुर्वेद, योग, और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में ‘ज्ञान भारतम मिशन’ की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत एक करोड़ प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। कभी हमारा देश हथियारों के आयात पर निर्भर था, पर अब हमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर भारत ने अनेक स्वदेशी मिसाइलें और अन्य स्वदेशी हथियार बनाए हैं। भारत ने चन्द्रयान और मंगल यान मिशन के जरिए अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी क्षमता सिद्ध की है।
हमारा यह ज्ञान अपने में विपुल संभावनाएं समेटे हुए है। इससे जैविक खेती, पारंपरिक बीजों का उपयोग, और पंचगव्य जैसे स्वदेशी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देकर लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। खादी, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक कपड़े और हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना संभव है। हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से जहां स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान संभव है, वहीं इससे चिकित्सकों और औषधि निर्माताओं के जरिए भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। स्वदेशी कला, संगीत, नृत्य और परंपरागत आयोजनों को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जा सकता है। अगर हम आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम कर स्थानीय रूप से उत्पादन बढ़ाते हैं तो इससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प और कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय कारीगरों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे स्टार्टअप्स को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम किए बिना हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति नहीं पकड़ सकती। स्वदेशी ब्रांडों को बढ़ावा देकर ही इसे बदला जा सकता है। पतंजलि इसका सशक्त उदाहरण है। इस कंपनी ने पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक उत्पादन और मार्केटिंग रणनीतियों से जोड़ा, जिससे यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती से स्थापित हुई। पतंजलि ने दिखाया कि भारतीय उद्यमी यदि अपनी जड़ों से जुडक़र नवाचार करें तो वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
यदि हम पारंपरिक ज्ञान को परिष्कृत कर सही रूप में अपनाएं तो इससे आय और उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आएंगे, पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा और भविष्य की पीढिय़ों को एक समृद्ध भारत मिलेगा। अब समय आ गया है कि हम अपने समृद्ध स्वदेशी ज्ञान और आर्थिक विकास के बीच संबंध को पहचानें और इसे पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।