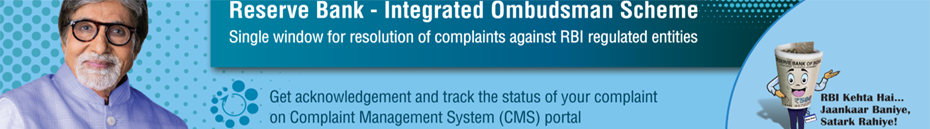आंबेडकर : समानता को लेकर उनका दृष्टिकोण आज भी भारत को प्रेरित करता है
Focus News 14 April 2025 0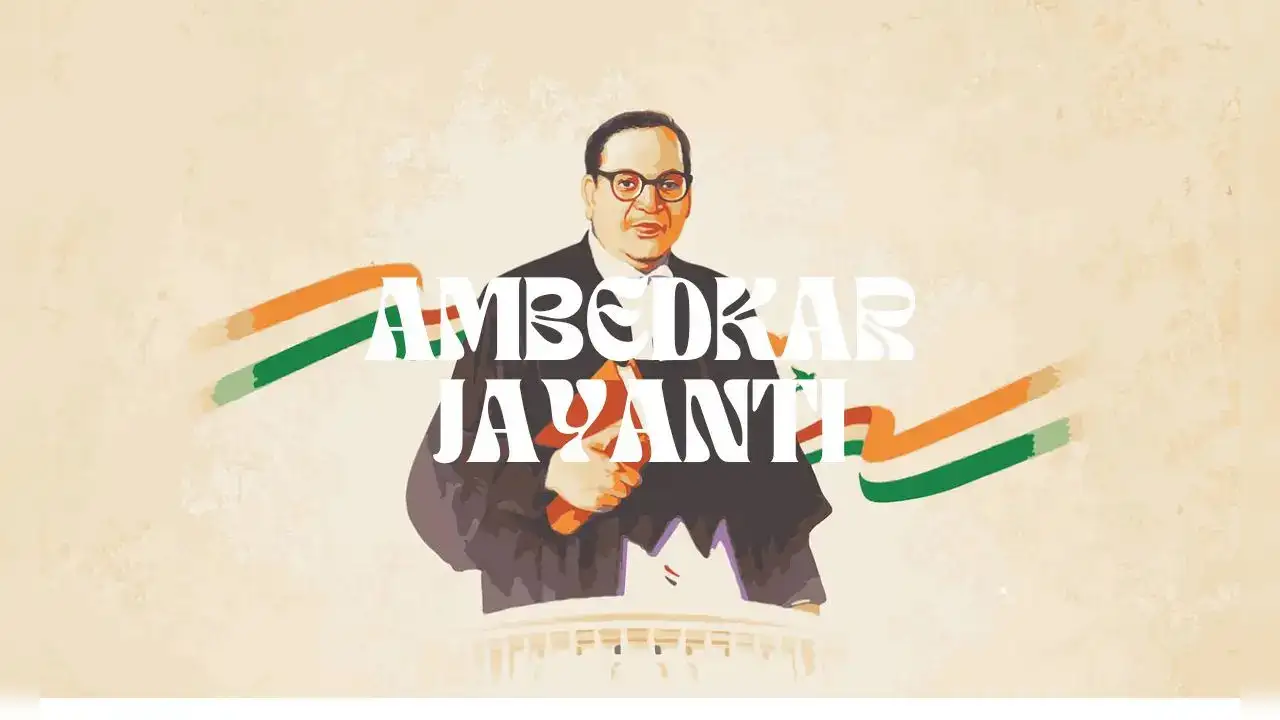
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) भारत सोमवार को डॉ. बीआर आंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। आंबेडकर के विचार केवल इतिहास की किताबों या औपचारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रमों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रतिरोध की परिभाषा को आकार दे रहे हैं और अदालतों से लेकर कक्षाओं, विरोध-प्रदर्शनों और साइबर संसार तक में गूंज रहे हैं, जहां जाति, समानता एवं लोकतंत्र के बारे में बहस अब भी जारी है।
संविधान निर्माता के रूप में विख्यात आंबेडकर एक विधिशास्त्री से कहीं अधिक थे। वह एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिनका समतावादी और जाति व्यवस्था मुक्त भारत का दृष्टिकोण देश के समकालीन सामाजिक-राजनीतिक विमर्श के लिए आज भी बेहद प्रासंगिक है।
दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सूरज येंगड़े के मुताबिक, आंबेडकर की छवि का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था की उनकी कड़ी आलोचना को स्वीकार किए बिना।
डॉ. येंगड़े ने अपनी किताब ‘कास्ट मैटर्स’ में लिखा है, “आंबेडकर की छवि का इस्तेमाल किसी भी मुद्दे पर दलितों के आक्रोश को दबाने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पीड़कों को फायदा मिलता है, जो आंबेडकर को घृणा और हिंसा के अपने क्रूर एजेंडे में शामिल करके बहुत खुशी महसूस करते हैं।”
उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे नेताओं ने 2024 के आम चुनावों के दौरान संविधान को एक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया।
डॉ. येंगड़े के अनुसार, “उन्हें (नेताओं को) सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान और श्रमिक वर्ग की सुरक्षा जैसे पारंपरिक मुद्दों के बजाय संविधान की ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित करना ज्यादा लाभदायक लगा।”
वर्ष 1891 में मध्यप्रदेश के महू में एक दलित परिवार में जन्मे आंबेडकर को कम उम्र से ही सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी सहित शिक्षा के लिए उनके अथक प्रयास ने उन्हें भारत के सबसे प्रखर बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों में से एक बना दिया।
आंबेडकर ने जाति व्यवस्था की सबसे तीखी आलोचना 1936 में प्रकाशित अपने निबंध ‘जाति का विनाश’ में की थी, जो मूलतः एक भाषण के रूप में लिखा गया था। हालांकि, भाषण की विषय-वस्तु के कारण उन्हें सार्वजनिक मंच पर इसे देने का मौका कभी नहीं मिला।
‘जाति का विनाश’ में आंबेडकर ने लिखा था, “जाति श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। यह एक पदानुक्रम है, जिसमें श्रमिकों के विभाजन को एक के ऊपर एक वर्गीकृत किया जाता है।” ये शब्द कक्षाओं, विरोध-प्रदर्शनों और जाति, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतिगत बहसों में आज भी गूंजते हैं।
समय के साथ आंबेडकर की विरासत की प्रासंगिकता बढ़ी है, न केवल सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं और चित्रों के माध्यम से, बल्कि लोकप्रिय संस्कृति, अकादमिक विद्वत्ता और विरोध की राजनीति के जरिये भी। आंबेडकर की जयंती पर भले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन संविधान निर्माता की विरासत की उनकी व्याख्याएं व्यापक रूप से अलग होती हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि “विकसित और समावेशी भारत” का निर्माण आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगा।
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना को आंबेडकर की समानता की चाह से जोड़ते हुए लगातार इसकी वकालत कर रहे हैं।
राहुल ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, “जाति जनगणना असमानता और भेदभाव की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे इसके विरोधी उजागर नहीं होने देना चाहते।”
उन्होंने लिखा था, “बाबासाहेब का सपना अभी भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आज की भी लड़ाई है और हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे।”
बावजूद इसके, कई विद्वानों का तर्क है कि आंबेडकर को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि भले ही कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने जिस ढांचागत जाति-आधारित अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसकी जड़ें अभी भी गहराई से व्याप्त हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ अपराध के कुल 57,582 मामले दर्ज किए गए।
आंबेडकर ने जाति-आधारित अपराधों से जुड़े खतरों को पहले ही भांप लिया था और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में इसे लेकर आगाह किया था।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन और भाषण (बीएडब्ल्यूएस) के खंड 13 के अनुसार, आंबेडकर ने कहा था, “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता, जब तक कि उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो… एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है।”
जाति के अलावा आर्थिक न्याय, शिक्षा, लैंगिक अधिकार और राज्य नियोजन को लेकर भी आंबेडकर का व्यापक दृष्टिकोण था। अफ्रीकी-अमेरिकी विचारक डब्ल्यूईबी डु बोइस के साथ उनके पत्राचार में उनके संघर्ष के वैश्विक आयाम प्रतिबिंबित होते हैं।
बीएडब्ल्यूएस के खंड 10 के मुताबिक, आंबेडकर ने 1946 में लिखा था कि भारत में अछूतों की स्थिति और अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकियों की स्थिति में बहुत समानता है।
डॉ. येंगडे ने जाति चेतना के बारे में आंबेडकर के विश्लेषण की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है।
उन्होंने ‘कास्ट मैटर्स’ में लिखा है, “आंबेडकर की दूरदर्शिता इस बात से झलकती है कि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जाति अपने आप में एक राष्ट्र है, जिससे राष्ट्रीय भाईचारे की भावना विकसित करने में मदद नहीं मिली।”
लोकतांत्रिक पतन पर बहस के बीच संघवाद और सत्ता के केंद्रीकरण पर नियंत्रण की आंबेडकर की वकालत का आज भी जिक्र किया जाता है।
संविधान सभा में 1949 में दिए गए भाषण में कही गई आंबेडकर की यह बात कि “लोकतंत्र मूलतः अलोकतांत्रिक भारतीय भूमि पर केवल एक ऊपरी आवरण है” बहुसंख्यकवाद पर होने वाली चर्चाओं में अक्सर उद्धृत की जाती है।
राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जैफरलॉट ने 2003 में प्रकाशित अपनी किताब ‘इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन’ में लिखा है कि कैसे आंबेडकर ने सामाजिक समानता के बिना लोकतंत्र के खतरों को पहले ही भांप लिया था, एक चेतावनी जो आज भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर छाई हुई है।
आंबेडकर का यह दृष्टिकोण 2025 में भी प्रासंगिक है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना लोकतंत्र फल-फूल नहीं सकता।
आज जब जाति, वर्ग और सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है, तब ‘जाति के विनाश’ में लिखी आंबेडकर की यह बात प्रेरित करना जारी रखती है कि “राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है, वह सरकार की अवहेलना करने वाले नेता की तुलना में अधिक बहादुर व्यक्ति है।”