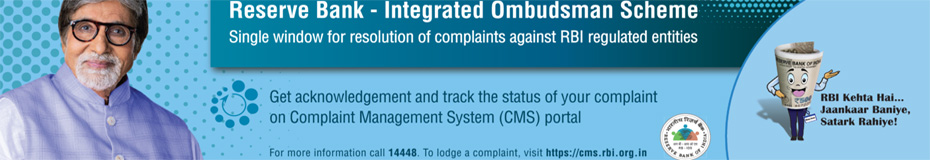हाल ही में दरभंगा की महारानी कुसुम देवी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय फिर से चर्चा में आया है जिसे लंबे समय तक लगभग भुला दिया गया था। वर्ष 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान दरभंगा राजपरिवार द्वारा राष्ट्ररक्षा के लिए किए गए असाधारण योगदान की स्मृतियाँ एक बार फिर सामने आई हैं। उपलब्ध विवरणों के अनुसार दरभंगा राजपरिवार ने 15 मन अर्थात लगभग 600 किलोग्राम सोना भारत सरकार को समर्पित किया था । यह दान इंद्र भवन मैदान, दरभंगा में सार्वजनिक रूप से किया गया—एक निजी संपत्ति को राष्ट्र को अर्पित करने का स्पष्ट और साहसी निर्णय ।
इसी कालखंड में कच्छ के महाराजा मदन सिंह जडेजा का योगदान भी सामने आता हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 100 टन (1,00,000 किलोग्राम) सोना राष्ट्र को दान किया—इतनी विशाल मात्रा कि उसे राष्ट्रीय कोष तक पहुँचाने के लिए रेलवे के आठ डिब्बों की आवश्यकता पड़ी । भले ही इन आँकड़ों पर ऐतिहासिक बहस संभव हो परंतु इस योगदान के आकार, नीयत और राष्ट्रहित को नकारा नहीं जा सकता । ये केवल दो नाम हैं जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। ऐतिहासिक संकेत बताते हैं कि देशभर के 100 से अधिक राजघरानों ने 500 किलोग्राम या उससे अधिक सोना 1962 के युद्ध के दौरान भारत सरकार को दान किया। यह वह समय था जब भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर था, सैन्य तैयारी अपर्याप्त थी और राष्ट्रीय मनोबल गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था। फिर भी, इतने बड़े योगदान सामूहिक स्मृति से लगभग गायब हो चुके हैं किन्तु, इन ऐतिहासिक उदाहरणों के सामने कुछ असहज लेकिन आवश्यक प्रश्न स्वतः उभरते हैं— क्या “सब कुछ त्याग देने” का अर्थ भारत के किसी भी इतिहास-ग्रंथ, स्मारक, प्रतिमा या सामूहिक स्मृति-पटल पर आज भी विद्यमान है, या फिर इसे सचेत रूप से भुला दिया गया है? भारत की संप्रभुता के लिए किए गए सर्वोच्च दान के बदले क्या मिला? क्या उसका मूल्य सम्मान, स्मृति और कृतज्ञता के रूप में चुकाया गया—या फिर विमर्श के स्तर पर उसे तिरस्कार, वर्गीय अपराधबोध और दलित-विरोधी छवि के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया गया?
भारत में इतिहास को अक्सर कुछ तयशुदा खाँचों में बाँटकर देखा गया है—औपनिवेशिक बनाम राष्ट्रवादी, सामंती बनाम लोकतांत्रिक, शासक वर्ग बनाम जनता । इस दृष्टि में राजा, पारंपरिक शासक वर्ग और शासक जाति प्रायः सामंत, ठाकुर का कुआँ जैसे प्रतीकों में सीमित कर दिए जाते हैं । इन आलोचनाओं में आंशिक सत्य अवश्य है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में अनेक स्थानीय शासकों और रियासतों ने विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध किया, जबरन धर्मांतरण का विरोध किया, स्थानीय संस्कृति, भाषा और शिक्षण संस्थानों को संरक्षित किया और समाज को संसाधन उपलब्ध कराए—उस समय, जब आधुनिक राष्ट्र–राज्य की संरचनाएँ अस्तित्व में भी नहीं थीं । कई मामलों में, ये शासक समाज की पहली सुरक्षा–रेखा थे । 1962 का युद्ध इसी ऐतिहासिक जटिलता को उजागर करता है । जब नवस्वतंत्र भारतीय राज्य संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, तब कई राजघरानों ने बिना किसी राजनीतिक सौदेबाज़ी के अपनी निजी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दी।
यह विमर्श जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल को कमतर आँकने के लिए नहीं है अपितु, नेहरू के नेतृत्व में हुए 1962 के भारत–चीन युद्ध के उस पक्ष को सामने लाने का प्रयास है जो अक्सर सार्वजनिक स्मृति से ओझल रह जाता है—वह पक्ष, जहाँ देश के अत्यंत कठिन समय में अनेक नागरिकों और राजपरिवारों ने अपनी निजी संपत्तियाँ, यहाँ तक कि सब कुछ, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस त्याग और नेतृत्व के प्रति सम्मान निर्विवाद है। वहीँ दूसरी ओर क्या 1962 के युद्ध के दौरान दान किए गए विशाल संसाधनों का पूर्ण, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग हुआ? यदि हुआ, तो उसके दस्तावेज़ और सार्वजनिक स्मृति कहाँ हैं; और यदि नहीं हुआ तो उस पर प्रश्न क्यों नहीं उठाए गए ? और क्यों कुछ चयनात्मक प्रेरणा बार-बार स्मरण किए जाते हैं—पाठ्यपुस्तकों, स्मारकों और राष्ट्रीय विमर्श में—जबकि अन्य बलिदान धीरे-धीरे इतिहास के हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं मानो उनका अस्तित्व ही असुविधाजनक हो?
ये प्रश्न किसी एक विचारधारा, व्यक्ति या कालखंड के विरुद्ध नहीं हैं। ये प्रश्न उस ऐतिहासिक न्याय की माँग हैं, जो राष्ट्र की स्मृति को चयनात्मक नहीं बल्कि संपूर्ण और ईमानदार बनाता है। इन प्रश्नों का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संदेह करना नहीं है अपितु । इसके विपरीत, ये प्रश्न इतिहास को अधिक समावेशी, ईमानदार और बहुस्तरीय बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम हैं।
भारत का इतिहास केवल शासक बनाम शोषित, नैतिक बनाम भौतिक, या लोकतंत्र बनाम परंपरा जैसे सरल द्वैतों में नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रनिर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया रहा है—जिसमें नैतिक नेतृत्व, जनआंदोलन, सैन्य साहस, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक त्याग, सभी ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है। इतिहास तब अधिक सशक्त होता है, जब वह किसी एक दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि साझी स्मृति और साझा उत्तरदायित्व का दस्तावेज बनता है। इतिहास तब असहज लगता है जब वह चयनात्मक स्मृति को चुनौती देता है। भारत का राष्ट्रनिर्माण केवल एक विचारधारा, एक वर्ग या एक आंदोलन का परिणाम नहीं रहा। यह विभिन्न प्रकार के साहस—नैतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक—का संयुक्त परिणाम है । राजघरानों के योगदान को स्मरण करना न तो राजशाही का महिमामंडन है, न ही लोकतंत्र का विरोध । यह उस समय की राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना को पहचानना है, जब वैचारिक मतभेदों से ऊपर राष्ट्र का अस्तित्व था।
आज, जब किसी राष्ट्रीय संकट में सरकार नागरिकों से सहयोग की अपील करती है, तो समाज का एक हिस्सा तत्काल अविश्वास, उपहास या राजनीतिक विरोध में उतर आता है। आलोचना लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है परंतु निरंतर नकारात्मकता सामूहिक उत्तरदायित्व को कमजोर कर सकती है। भारत की संप्रभुता एक साझा विरासत है, जिसमें राजपरिवारों के बलिदानों ने भी आकार दिया है। इन भूले-बिसरे अध्यायों को स्मरण करना हमें न केवल इतिहास, पूर्वजों के प्रति ईमानदार बनाता है, बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय संकटों के समय सामूहिक कर्तव्यबोध को भी पुनर्जीवित कर सकता है। इतिहास श्रद्धा नहीं, संतुलन माँगता है। और कभी-कभी वह हमें असहज करता ह—क्योंकि वही असहजता परिपक्व राष्ट्रीय चेतना की पहली सीढ़ी होती है।
गजेंद्र सिंह
लोक नीति विश्लेषक