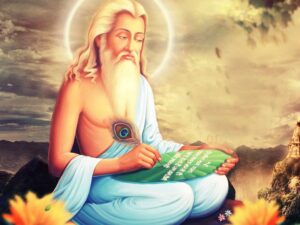पांच हजार वर्ष पूर्व भारत के क्षितिज पर भादों की अंधेरी अमावस अपनी गहरी कालिमा के साथ छा गई थी। तब भी भारत में जन था, धन था, शक्ति थी, साहस था, कला और कौशल क्या नहीं था? सब कुछ था पर एक अकर्मण्यता भी थी, जिससे सभी कुछ अभिभूत और मोहाच्छन्न थे। महापुरुष अनेक हुए हैं पर लोकनीति और आध्यात्म को समन्वय के सूत्र में गूंथकर ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनÓ का पांत्र्चजन्य फूंकने वाले श्रीकृष्ण ही थे।
आर्य जीवन का सर्वांगीण विकास हम श्रीकृष्ण में पाते हैं। राजनीति और धर्म, आध्यात्म और समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में श्रीकृष्ण को हम एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं। यदि हम राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें महाभारत के पन्ने टटोलने होंगे। महाभारत आर्य जाति के पतन का युग कहा जाता है। उस समय भारतवर्ष में छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्य थे। इन छोटे-छोटे राज्यों का एक संगठन नहीं था। एक चक्रवती सम्राट के न होने से कई राजा अत्याचारी और उच्छृंखल हो गए थे। मगध का जरासंध, चेदी देश का शिशुपाल, मथुरा का कंस और हस्तिनापुर के कौरव सभी दुष्टï, विलासी और दुराचारी हो गए थे। श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत राजनैतिक चातुर्य द्वारा इन सभी राजाओं का मूलोच्छेद कराया और युधिष्ठिïर का एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया।
यदि श्रीकृष्ण स्वयं चाहते तो इतने बड़े राज्य के शासक बनकर संसार के सुखों का उपभोग कर सकते थे, परंतु उनका यह लक्ष्य नहीं था। समस्त राष्टï्र का कल्याण सोचने वाले श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिïर को चक्रवर्ती सम्राट के आसन पर अभिषिक्त किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। उनकी इसी उदार भावना के कारण जब राजसूय यज्ञ में अग्रपूजा के लिए किस व्यक्ति को चुना जाए, यह प्रश्न आया, तब भीष्म पितामह ने श्रीकृष्ण का नाम प्रस्तुत किया और सर्वानुमति से उनकी अग्रपूजा की गई।
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि युधिष्ठिïर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण जी ने अपने लिए सब आगतों के पाद प्रक्षालन का काम ही चुना था। यह नम्रता की पराकाष्ठïा थी।
मानव जाति ने श्रीकृष्ण के समान राजनीति निपुण व्यक्ति कम ही पैदा किए हैं। महाभारत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पथ प्रदर्शक विष्णुगुप्त अर्थात् चाणक्य में भी हम इसी विलक्षण प्रतिभा का दर्शन करते हैं। ‘सूच्यम नैव रास्यामि बिना युद्धेन केशव:Ó की गर्वोक्ति करने वाले दुर्याेधन का नाश करवाना श्रीकृष्ण जैसे विलक्षण पुरुष का ही काम था। यदि श्रीकृष्ण पाण्डव पक्ष में न होते तो उनकी विजय में संदेह ही किया जा सकता है।
श्रीकृष्ण ने न केवल भारत राष्टï्र की अखण्डता की ही रक्षा की, अपितु उन्होंने गिरे हुए भारतीय समाज को भी उद्बोधन दिया। उस समय स्त्रियों और शूद्रों की अत्यधिक अवनति हो गई थी। स्त्रियों और शूद्रों का मोक्ष में अधिकार नहीं माना जाता था।
वर्ण व्यवस्था गुण-कर्म की अपेक्षा जन्म से मानी जाने लगी थी और इसी कारण सूत पुत्र कर्ण को पाण्डवों द्वारा अपमानित होना पड़ा था। ब्राह्मïणों ने अपनी वृत्ति छोड़ दी थी। द्रोणाचार्य सरीखे विद्वान भी शस्त्र विद्या सिखाकर जीवन निर्वाह करते थे। लोगों का अत्यधिक नैतिक पतन हो गया था। भीष्म जैसे धर्मात्मा पुरुष भी अपने को दुर्योधन के अन्न से पालित समझकर अन्याय का पक्ष ग्रहण कर लेते थे। उस समय उनकी विद्या, बुद्धि और धर्मभीरूता सब ताक पर धरी रह जाती थी।
जिस समय समाज का इस प्रकार अत्यधिक पतन हो गया था, तब श्रीकृष्ण ने एक नूतन संदेश दिया। गीता द्वारा उन्होंने चारों वर्णों को गुण कर्मानुसार घोषित किया और यह स्पष्टï कर दिया कि इस व्यवस्था की नींव गुण, कर्म और स्वभाव पर है, जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ‘चातुर्वणं मया सृष्टïं गुणकर्मविभागश:Ó इसी स्पष्टïोक्ति की घोषणा है। गीता में ही श्रीकृष्ण ने स्त्रियों और शूद्रों को मोक्षाधिकार का विधान किया-
मां हि पार्थ व्यपालिश्रत्य, येऽपि स्यु: पापयोनय:।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तऽपियान्ति परां गतिम्ï॥
हे पार्थ ! अत्यंत नीच वंश में उत्पन्न मनुष्य हो, स्त्री हो, वैश्य हो और शुद्र हो, जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, उनको उत्तम गति मिलती है। उच्च कुल में जन्म लेकर गोप-ग्वालों के साथ प्रेम दिखाना और उनके साथ मैत्री भाव रखना, श्रीकृष्ण की उदारता और सदाशयता का ही सूचक है।
श्रीकृष्ण केवल राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक ही नहीं थे, एक उच्चकोटि के आध्यात्मवादी योगी भी थे। जहां उन्होंने धर्म के एक अंग अभ्युदय का संपादन किया था, वहीं उन्होंने नि:श्रेयस्ï मार्ग को भी उतना ही महत्व दिया था। आर्य धर्म की सदा से ही यह विशेषता रही है कि इसके अनुयायी इस लोक की सिद्धि के साथ-साथ पारलौकिक सुधार की ओर अत्यंत ध्यान देते रहे हैं। यदि आर्य संस्कृति से अनजान व्यक्ति इसे पलायन मनोवृत्ति कहें तो यह उनकी अनभिज्ञता का ही सूचक है। आर्य जीवन का लक्ष्य सांसारिक उन्नति के साथ-साथ नि:श्रेयस् तथा मोक्ष प्राप्ति भी माना जाता है।
श्रीकृष्ण ने आर्य जीवन के इस पहलू पर भी अधिक जोर दिया है परंतु उन्होंने मनुष्य जीवन को दु:ख का पर्याय नहीं मान लिया था, इसके विपरीत उन्होंने संसार को सच्ची कर्मभूमि बतलाया है। फल की आशा छोड़कर निष्काम कर्म करना ही सच्चा कर्म योग है। आर्य धर्म का यही निचोड़ है। गीता की यही मुख्य शिक्षा है।
श्रीकृष्ण की आध्यात्मिक शिक्षाओं का परिचय हमें गीता द्वारा मिलता है। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म, ज्ञान और कर्म का समन्वय, स्थितप्रज्ञ मनुष्यों के लक्षण, वर्ण व्यवस्था आदि-आदि विषयों पर सांगोपांग विचार यदि हम देखना चाहें तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता को यदि भारतीय आर्य धर्म का विश्वकोश कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गीता में ही श्रीकृष्ण का वास्तविक चरित्र प्रस्फुटित हुआ है। गीता के श्रीकृष्ण हमारे सामने जगद् गुरु के रूप में आते हैं। ‘नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणिÓ द्वारा आत्मा की अमरता के बताते हुए श्रीकृष्ण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं :-
यदुच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्ï।
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्॥
इस श्लोक द्वारा श्रीकृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्षत्रिय के लिए धर्म-युद्ध ही स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और आततायियों के नाश के लिए शस्त्र उठाना पाप नहीं है। आवश्यकता है कि श्रीकृष्ण चरित्र का आज के युग में अधिक से अधिक पठन और मनन किया जाए। न केवल मनन ही वरन् उनकी शिक्षा के अनुसार चलने का भी प्रयत्न करें।
श्रीकृष्ण की शिक्षा में ही देश का कल्याण निहित है। आज जब आर्य जाति पर चतुर्मुखी आक्रमण हो रहे हैं, श्रीकृष्ण की शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। गीता के अंत में कही गई संजय की निम्न पंक्ति में हमें अद्भुत सत्य के दर्शन होते हैं:-
यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर:।
तत्र श्रीर्विजयो, भूतिध्र्रुवा नीतिर्मतिर्मम् ॥