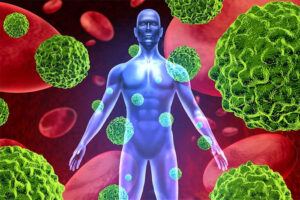जून से सितम्बर के समय में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी तो पड़ती ही है, वर्षा भी खूब होती है। इस मौसम में वातावरण में उमस के साथ-साथ नमी भी काफी रहती है। पसीने की अधिकता और वायुमंडल की नमी से अधोवस्त्रा (जैसे कच्छा, बनियान, जांघिए आदि) पूरी तरह सूख नहीं पाते और उनमें नमी बनी रहती है, जिससे प्रायः फंगस या फफूंद रोग उत्पन्न होने की संभावना 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
इस से शरीर के जोड़ वाले उन स्थानों पर जहां त्वचा कोमल होती है व अधिक मांस होने से आपस में रगड़ खाने व नमी में जीवाणु पैदा हो जाने से, त्वचा की ऊपरी परत छिल कर संक्रमण हो जाता है और प्रायः जांघों, कांख, पैरों की उंगलियों में हल्की-सी खुजली के साथ परेशानी शुरू होती है। पर्याप्त सफाई न रखने से मैल में छिपे कीटाणु एवं जीवाणु इस खुजली को बढ़ा देते हैं तथा परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि दाद या एग्जिमा तक का रूप धारण कर लेती है।
एलोपैथी में इस बीमारी को फंगल इंफेक्शन के नाम से जाना जाता है तथा त्वचा की एलर्जी से संबंधित ट्रीटमेंट (उपचार) दिया जाता है। आरम्भिक अवस्था में होने पर बेटनोवेट एन, या बेटनोवेट जी एम अथवा बेटनोवेट सी जैसी बीटामेथासोन वेलरेट और माइकोनाजोल नाइट्रेट तथा जेंटामायसीन मिश्रित क्रीम लगाने को दी जाती है। इनमें बीटामेथासोन और नाइटेªट एण्टी एलर्जिक का कार्य करते हैं जो त्वचा की संक्रमित कोशिकाओं को पुनः ठीक अवस्था में लाने के लिए बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो जेण्टामाईसीन एण्टीबायोटिक के रूप में रोग को बढ़ने से रोकते हैं।
होम्योपैथ डॉ प्रदीप वर्मा बताते हैं कि इस खाज-खुजली से बचने का सबसे अच्छा उपचार तो यह है कि इसे होने ही न दिया जाए। डॉ वर्मा के अनुसार हमें अपने अंदरूनी वस्त्रों को नमी से मुक्त रखना चाहिए। यदि वर्षा, बादलों की वजह से खुली धूप न निकले तो अधोवस्त्रों को अच्छी तरह प्रेस करके सुखा लेना चाहिए। जांघों आदि के बीच मैल इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए तथा स्नान के बाद रोएंदार तौलिये से हल्के-हल्के पोंछना चाहिए।
नायसिल या बोरोप्लस जैसे किसी भी अच्छे प्रिक्ली हीट पाउडर का छिड़काव भी संक्रमित होने की आशंका वाले स्थानों पर करना भी अच्छा रहता है। यदि फफूंदी हो ही जाए, तब बनियान और जांघिए आदि को जीवाणुमुक्त करने के लिए उन्हें पानी में अच्छी तरह उबाल कर धोना चाहिए। कपड़ा खराब होने का डर हो तो डिटॉल की कुछ बूंदें धोने वाले पानी में डाल लेनी चाहिएं। संक्रमित स्थानों को भी डिटॉल मिश्रित पानी या पोटेशियम परमेगनेन्ट मिश्रित पानी से साफ करना चाहिए।
ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के संधिकाल में अनेक जीवाणु एवं विषाणु (वायरस) वायुमंडल में आ जाते हैं। ऐसे ही विषाणुओं में से एक है रोटा वायरस। यह वायरस वायु एवं जल दोनों ही माध्यमों से हमला करने में महारत रखता है। जैसे ही यह वायरस हमला करता है, पीडि़त व्यक्ति के शरीर में भारी सिरदर्द, बदन दर्द, आंखों में भारीपन तथा तेज बुखार का हमला हो जाता है। कई बार शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री तक भी पहुंच जाता है तथा रोगी बेहोश भी हो सकता है। यह बुखार 6-7 घंटे बाद पुनः हमला करता है। यह क्रम छह सात दिन तक लगातार चलता है। पहले 3-4 दिन तक यह बुखार हर बार तीव्रतर होता चला जाता है। ऐसी अवस्था में कई बार रोगी सर्दी से कांपने भी लगता है तथा बेहोशी में बड़बड़ाता भी है।
वस्तुतः इस वायरल को काबू में करने में चिकित्सा विज्ञान अभी पूरी तरह सफल नहीं रहा है। चिकित्सक प्रायः रोगी को पेरासिटामोल (पी. सी. एम) एवं सी. पी. एम. का सात रोज का कोर्स कराते हैं प्रतिरोधी दवाइयों के रूप में रोगी के शरीर की प्रकृति के अनुसार एमोक्सीसीलीन या एम्पीसीलीन अथवा अन्य एण्टीबायोटिक औषधि देते हैं। उल्टी की स्थिति में फेनारगन, रेगलॉन, या पैरीनोर्म आदि की उचित एम. जी. देते हैं। सात दिन में यह वायरस स्वयंमेव कमजोर पड़ जाता है परन्तु बुखार न उतरने पर यह कोर्स दोहराया जा सकता है।
होम्योपैथी में डॉ वर्मा के मतानुसार रह्सलॉक्स, गैल्सुमियम, परफोलियम आदि दवाईयों की खुराकें दिन में हर चार या छह घण्टे बाद देना लाभदायक सिद्ध होता है। पुनः डॉ वर्मा कहते हैं कि वायरल बुखार खतरनाक भी हो सकता है और समय पर उपचार उपलब्ध न होने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः वायरल के लक्षण दिखते ही रोगी को डाक्टर के पास जाना चाहिए।
स्वयं ही दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि विशेषज्ञ डॉ आपके लक्षण देखकर ही औषधि एवं उसकी मात्रा का निर्धारण करता है, साथ ही साथ पथ्य अपथ्य की भी सलाह देता है। वायरल के हमले से बचने के लिए ताजा व स्वच्छ भोजन लेना चाहिए। ठंडे बासी खाने से व प्रदूषित जल से भी बचना चाहिए। वायरल के रोगी से विशेषकर बच्चों को दूर ही रखना चाहिए।