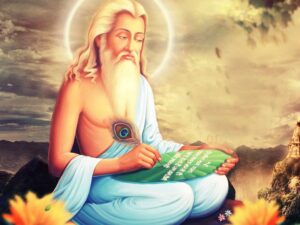आज जिधर भी दृष्टि पसार कर देखा जाए, उधर अभाव, असंतोष, चिंता, क्लेश एवं कलह का ही बाहुल्य दिखाई पड़ता है। यूं तो वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ अगणित प्रकार के सुविधा-साधन बढ़ गए हैं पर उनसे न व्यक्ति की शांति बढ़ी और न ही समाज की प्रगति हुई। विज्ञान की उपलब्धियों पर विचार करें तो प्रतीत होता है कि आज से हजार वर्ष पहले के मनुष्य की अपेक्षा अब की सुविधा-सामग्री इतनी अधिक है, जितनी मनुष्यलोक एवं देवलोक के बारे में कल्पित की जा सकती है। पूर्वकाल में रेल, मोटर, डाक-तार, बिजली, प्रेस, रेडियो, मशीनें, कल-कारखाने, जहाज आदि कहां थे? साबुन, माचिस से लेकर फाउण्टेन पैन, साइकिल तक दैनिक जीवन में अनेक चीजें विज्ञान की देन हैं।
चिकित्सा एवं शिक्षा के साधन बहुत बढ़ गए हैं। इस सब के साथ-साथ मनुष्य की सुविधा एवं प्रसन्नता बढऩी चाहिए थी। आर्थिक विकास भी इन हजार-पांच सौ वर्षों के भीतर आश्चर्यजनक हुआ है। इसका लाभ मिलने से मानसिक सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, पर दिखता है कि उलटी और कमी ही हुई है। लोग अपने आपको अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिन्तित, एकाकी असहाय एवं समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति को देखते हुए लगता है कि पिछले हजार वर्षों में हम बहुत अधिक संपन्न हो गए हैं पर बारीकी से विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस अवधि में हम कही अधिक पिछड़े, गिरे, बिगड़े हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष एवं आंतरिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में भारी अवसाद एवं गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टिï से आज की सुविधा-संपन्नता और पूर्वकाल की असुविधा भरी परिस्थितियों की तुलना की जाए तो लगता है कि वे असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी एवं संतुष्टï थे। तब की और अब की परिस्थितियों में उतना ही अंतर आ गया है, जितना स्वर्ग और नरक में माना जाता है। वस्तुत: आज हमें नारकीय परिस्थितियों में ही रहना पड़ रहा है।
यह नरक कहीं अन्यत्र से उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ने ही इसे पैदा किया है। निश्चित रूप से हमारी भली-बुरी परिस्थितियों के उत्तरदायी हम स्वयं ही हैं। उनका दोषारोपण किसी दूसरे पर करके झूठा मन-संतोष कर लेना निरर्थक है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं, केवल उत्कृष्टï और निकृष्टï दृष्टिïकोण की प्रतिक्रिया मात्र है। आज व्यक्ति और समाज पर जो दु:ख और दारिद्रय की काली घटाएं घुमड़ रही हैं, उनका कारण भावनात्मक स्तर में अवांछनीय प्रवृत्तियों का आ जाना ही है। इसका समाधान-निराकरण यदि अभीष्टï हो तो अमुक समस्या के अमुक सामयिक समाधान से काम न चलेगा वरन् सुधार वहीं करना होगा जहां से कि ये विभीषिकाएं उत्पन्न होती हैं।
लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह गिरता चला जा रहा है, रुग्णता और दुर्बलता ने हर शरीर में अपना अड्डा जमा लिया है। चारपाई पर पड़े कराहते रहने की स्थिति भले ही न आ पाई हो पर किसी-न-किसी प्रकार की रुग्णता ने घेर जरूर रखा होगा। स्वस्थ व्यक्ति में जितनी कार्यक्षमता होनी चाहिए, उतनी आज कितने व्यक्तियों में है? टूटे-फूटे स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं।
इस स्थिति का कारण बहुमूल्य पौष्टिïक भोजन का न मिलना नहीं है। भील और वनवासी, किसान और मजदूर जिन्हें बहुत घटिया किस्म का भोजन मिलता है, अपेक्षाकृत अधिक सशक्त एवं निरोग दिखते हैं। यदि आहार में पौष्टिïकता ही आरोग्य का आधार रही होती तो संपन्न लोगों में हर एक बलिष्ठ और निर्धनों में से हर एक रुग्ण, अस्वस्थ दिखाई पड़ता। आरोग्य संकट का एकमात्र कारण है हमारा आहार विहार संबंधी भ्रष्टïाचार। असंयमी और उच्छृंखल रीति-नीति अपनाकर हम प्रकृति से जितने ही दूर हटे हैं, उतने ही अस्वस्थ होते चले गये हैं। यह भूल दवा-दारू की लीपा-पोती से नहीं सुधर सकती। हमें प्रकृति की शरण में लौटना पड़ेगा। आहार-विहार संबंधी संयम अपनाना होगा। यह कार्य दृष्टिïकोण के परिवर्तन से ही संभव है।
मानसिक अस्वस्थता आंखों में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए लोग उसके संबंध में प्राय: बेखबर रहते हैं पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो शरीर से भी कही अधिक रुग्ण एवं दुर्बल मन पाए जाएंगे। अनिद्रा, सिरदर्द, स्मरण शक्ति की कमी, मूढ़ता, उन्माद जैसे मस्तिष्कीय रोगों की बाढ़ तो आ ही रही है। चिंता, भय, निराशा, आवेश, अधीरता, हड़बड़ी, सनक, शक्कीपन, अव्यवस्था, निरुत्साह जैसे मनोविकार अधिकतर लोगों को अपना शिकार तथा अनेक व्यक्तिगत जीवनों को पतनोन्मुख बनाए हुए हैं। भावनात्मक अस्वस्थता के कारण अधिकांश लोग प्रफुल्लता, उल्लास, साहस, पुरुषार्थ, उदारता, वीरता, सहृदयता, सज्जनता जैसे मानवोचित गुणों से वंचित हो रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उसकी जीवात्मा पाशविक स्तर का जीवन-यापन कर रही है। ईश्वरप्रदत्त महान् महत्ताओं से वह तनिक भी लाभ नहीं उठा पाता और कीट-पतंगों जैसा आहार, निद्रा प्रधान हेय जीवन जी कर इस संसार से विदा हो जाता है। जिन लोगों के साथ उसका सम्पर्क रहता है, वे कुढ़ते, पछताते और असंतोष ही प्रकट करते रहते हैं। न उसे किसी से संतोष, न उससे किसी को संतोष। ऐसे निरर्थक एवं निंदनीय जीवन स्तर बने रहने का कारण भावनात्मक अस्वस्थता ही है। काश, मनुष्य की भावनाएं उदात्त एवं उत्कृष्टï रही होतीं तो सामान्य परिस्थितियों और सामान्य साधनों के रहते हुए भी उसने महापुरुषों जैसा नररत्नों जैसा प्रकाश एवं आनंद भरा जीवन जिया होता।
यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि अमुक सुविधा या परिस्थिति का होना न होना मानसिक अस्त-व्यस्तता का कारण नहीं है। सही बात यह है कि मानसिक अस्त-व्यस्तता ही जीवन में अभाव एवं विपन्नता की परिस्थिति उत्पन्न करती है। प्राय: प्रत्येक महापुरुष विपन्न परिस्थितियों में जन्मा अथवा रहा है, उसने अपने मनोबल से ही अनुकूलता उत्पन्न की और साधन जुटाए। इस प्रकार का मनोबल प्राप्त करने के लिए हमें सारा ध्यान अपनी मनोभूमि के निरीक्षण, संशोधन, सुधार एवं विकास में लगाना होगा। यह प्रयोजन जितना-जितना पूरा होता चलेगा, हम आंतरिक दृष्टिï से उतने ही सशक्त-समर्थ होते चले जाएंगे तथा मानसिक स्वस्थता का इतना अधिक लाभ एवं आनंद उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर यह जीवन और यह संसार स्वर्ग जैसा मंगलमय एवं उल्लासपूर्ण अनुभव होने लगे।
सामाजिक, राष्टï्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो विकृतियां दृष्टिïगोचर हो रही हैं, वे कहीं आकाश से नहीं टपकीं हैं, वरन् हमारे अग्रणी, बुद्धिजीवी एवं प्रतिभा संपन्न लोगों की भावनात्मक दुष्टïता ने उन्हें उत्पन्न किया है। जनमानस में छाए हुए अविवेक एवं अवसाद के कारण ही वे दुष्टïप्रवृत्तियां पनप और फलफूल रही हैं। यदि मान्यताओं और विचारणाओं की दिशा बदल जाए तो संसार में फैली हुई अशांति के अगणित स्वरूप देखते-देखते समाप्त हो जाएं।
विवाह-शादियों के नाम पर होने वाला फूहड़ दिखावा एवं अपव्यय व्यक्ति की आर्थिक और नैतिक नींव को बुरी तरह खोखला कर रहा है। जाति-पांति के नाम पर अमुक वंश में पैदा होने के कारण एक मनुष्य दूसरे से ऊंचा या नीचा समझा जाए, यह मान्यता कितनी अविवेकपूर्ण एवं अन्यायमूलक है, इसे कोई भी विचारशील सहृदय व्यक्ति सहज ही स्वीकार कर लेगा, फिर भी हमारे समाज में यह मूढ़ता अपनी गहरी जड़े जमाए बैठी है।
धर्म के नाम पर करोड़ों व्यक्ति आलस्य और प्रमाद का जीवन जी रहे हैं। मंदिर, मठ, तीर्थ एवं दान-पुण्य के नाम पर समय और धन का जितना व्यय होता है, यदि उसका ठीक तरह उपयोग होने लगे तो हमारी सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति इतनी गतिशील हो जाए कि प्राचीनकाल का गौरव पुन: प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई शेष न रह जाए।
हमारे धार्मिक नेता अलग-अलग संप्रदाय चलाकर अपनी-अपनी अलग पूजा-प्रतिष्ठïा का गोरखधंधा छोड़ दें और एक ही मंच से सारे समाज को संगठित एवं समर्थ बनाने में लग जाएं तो इतना बड़ा परिणाम सामने आए, जिसे देखकर संसार आश्चर्यचकित रह जाए। हमारे राजनेता अपना व्यक्तिगत वर्चस्व बनाए रखने के लिए भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद की अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। फूट और विघटन के बीज बो रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न रहकर राजनेता सरकारी मशीन और जनता को अपने अनुकरण के लिए प्रोत्साहन देकर देश में विविध-विधि भ्रष्टïाचार का सृजन कर रहे हैं। यदि इनका दृष्टिïकोण सुधर जाए और वे अशोक, राम, युधिष्ठिïर, जनक, अश्वघोष, चाणक्य जैसे निस्पृह राजनेताओं का उदाहरण प्रस्तुत करने लगें तो राजनैतिक स्थिति का स्वरूप ही बदल जाए।
गांधी, पटेल, सुभाष, नेहरू, मालवीय, लाजपतराय, तिलक जैसे राजनेता स्वाधीनता का वरदान दिला गए, उसी प्रकार का उच्च भावनासंपन्न नेतृत्व यदि आज भी हमारे पास रहा होता तो राम-राज्य को वे अपने सामने मूर्तरूप होता देख रहे होते, जिसे गांधीजी ने कोमल कल्पनाओं के साथ संजोया था। राजनैतिक गुत्थियां जो आज उठ खड़ी हुई हैं, वे छिट-पुट आयोगों, उपायों एवं समझौतों से नहीं सुलझेंगी। अग्रणी नेतृत्व को सद्भावनासंपन्न बनाना ही एकमात्र उपाय है, जिससे देश की वास्तविक एवं सुस्थिर प्रगति संभव हो सकती है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लागू होती है। विश्वनेता विश्वमंच बनाकर सारी दुनिया का एक राज्य परिवार बना लें।
देश-देश के बीच होने वाले आक्रमणों एवं संघर्षों की संभावना समाप्त कर दें। विश्वन्यायालय, विश्वसेना बना लें। संपत्ति, भूमि और ज्ञान का उचित वितरण कर दें तो अकाल, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा जैसे कष्टïों का संसार से अंत हो जाए। जितनी जनसंख्या सेना में भर्ती है, अस्त्र-शस्त्र तथा सेना-सामग्री बनाने में जितना धन खर्च होता है, वह सब मानव-कल्याण के कामों में लगने लगे, तो समस्त संसार में स्वर्गीय सुख-शांति की स्थापना में देर न लगे। वह कार्य युद्धों में एक-दूसरे को जीतने नहीं वरन् सार्वभौम विचार करने की शैली बदलने से संभव होगा।
इन दिनों परमाणु अस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की तैयारी हो रही है। अंतर्राष्टï्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाएं इस दिशा में संलग्र हैं। तीसरा सर्वनाशी महायुद्ध अणु-आयुधों से हुआ तो वैज्ञानिक आइन्सटीन की यह भविष्यवाणी अक्षरश: सत्य होकर रहेगी कि ‘चौथा युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा।Ó तब चिरसंचित मानवीय सभ्यता का एक प्रकार से लोप हो जाएगा और मनुष्य को अपना विकास आदिमयुग की जंगली अवस्था से फिर आरंभ करना होगा। इन तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से किसी भी विचारशील को एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्त समस्याओं, कठिनाइयों, उलझनों, विपत्तियों का एकमात्र कारण उसका दृष्टिïकोण, भावनास्तर विकृत हो जाना ही है। इसे सुधारे बिना अन्य समस्त छिटपुट उपचार, आयोजन कुछ क्षणिक प्रयोजन भले ही पूरा करें, वास्तविक एवं चिरसमाधान उपस्थित नहीं कर सकते। आज या कल जब कभी भी वास्तविक, चिरस्थायी और सुदृढ़ विश्वशांति की आवश्यकता अनुभव की जाएगी और उसके लिए दूरदर्शितापूर्ण हल खोजा जाएगा तो वह हल एक ही होगा-‘मानव-प्राणी की विचार-पद्धति में उत्कृष्टïता एवं आदर्शवादिता के अनुरूप परिवर्तन प्रस्तुत करना।Ó
सद्भावना, उत्कृष्टï विचारणा, विवेकशीलता एवं सत्यनिष्ठïा के लिए जनमानस में उत्कंठा तथा श्रद्धा का सृजन करना होगा। यह आकांक्षा जितनी ही तीव्र होती जाएगी, उज्ज्वल भविष्य की संभावना उतनी ही निकट आती चली जाएगी।