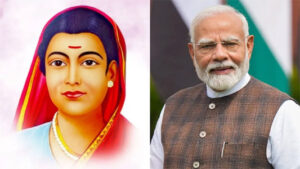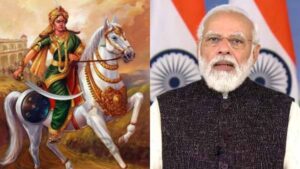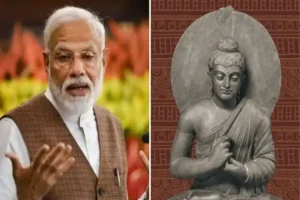किसी भी देश की तरक्की इस निर्भर करती है कि वहां के बाशिंदे किस तरह सोचते हैं। जैसे वे तर्क पर भरोसा करते हैं या अंधविश्वास पर, वे सवाल पूछने का साहस रखते हैं या भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं…साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यह फर्क ही तय करता है कि कोई समाज आगे बढ़ेगा या ठहर जाएगा।
साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति हर बात को तर्क, प्रमाण और विवेक की कसौटी पर परखता है। यह दृष्टिकोण केवल प्रयोगशाला या वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित नहीं है; यह तो रोजमर्रा के जीवन में अपनाई जाने वाली समझदारी है। जब हम किसी बात पर क्यों, कैसे और क्या सबूत हैं जैसे सवाल उठाते हैं तभी हम विज्ञान के असली अनुयायी होते हैं।
संविधान ने भी दी है वैज्ञानिक सोच की जिम्मेदारी
बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारतीय संविधान की धारा 51(ए)(एच) में हर नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक यह है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करे। यानी यह केवल कोई बौद्धिक विकल्प नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। संविधान निर्माताओं ने आज़ादी के बाद यह भांप लिया था कि अगर भारत को अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और अंधानुकरण से ऊपर उठाना है तो जनता के सोचने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। पर आज भी सवाल यह है कि क्या हम इस दिशा में सचमुच आगे बढ़ पाए हैं?
व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है वैज्ञानिक सोच
हमारा व्यक्तिगत जीवन ही समाज और राष्ट्र की नींव है। जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो उसकी सोच और निर्णय अधिक व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर यकीन करने के बजाय डॉक्टर की सलाह और प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करता है, बच्चों की शिक्षा में अंधविश्वास या रटने की जगह प्रयोग और अनुभव को महत्व देता है, किसी भी नई बात को आंख मूंदकर नहीं मानता, बल्कि तर्क और तथ्य से परखता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भय और भ्रम की जगह आत्मविश्वास और यथार्थ की समझ विकसित होती है। यह वही सोच है जो व्यक्ति को मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि सोचने वाला नागरिक बनाती है।
पारिवारिक जीवन में विज्ञान का संस्कार
किसी समाज की बुनियाद परिवार होता है। अगर परिवार में बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं दी जाती, तो वे आलोचनात्मक सोच नहीं सीख पाते। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है- ज्यादा सवाल मत पूछो! यही वह वाक्य है जो पीढ़ियों तक हमारी जिज्ञासा को कुचल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला परिवार बच्चों को जिज्ञासु बनाता है। वह बताता है कि धर्म और परंपरा का सम्मान करते हुए भी तर्क और प्रमाण का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। जब घर में विज्ञान का माहौल होता है -अंधविश्वास की जगह विश्वास का विवेक जन्म लेता है। अंधभक्ति की जगह तर्कशील आस्था आती है। डर की जगह समझदारी और जिम्मेदारी विकसित होती है। यही संस्कार आने वाले समाज की सोच तय करते हैं।
समाज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण
जब समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है, तो उसमें सुधार और प्रगति की गति कई गुना बढ़ जाती है। एक ऐसा समाज अफवाहों और दुष्प्रचार से आसानी से नहीं बहकता। झूठे धार्मिक या राजनीतिक दावों की जांच करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर प्रमाणिक और व्यावहारिक समाधान खोजता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह दृष्टिकोण एकता और विवेक का सेतु बन सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक सोच न तो जाति देखती है, न धर्म; वह सिर्फ सच और झूठ का फर्क पहचानती है। अगर कोरोना महामारी के दौर में देखें तो जिन देशों में जनता ने विज्ञान और डेटा पर भरोसा किया, वहां नुकसान कम हुआ। जबकि जहां अंधविश्वास, अफवाह और इनकार का भाव रहा, वहां नुकसान बहुत बड़ा हुआ।
लोकतंत्र की आत्मा है साइंटिफिक टेम्परामेंट
साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब यह नहीं कि हर चीज को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाए। इसका अर्थ है – हर बात को तर्क, अनुभव और प्रमाण के आधार पर समझना। यह सोच हमें झूठी खबरों, अफवाहों और विभाजनकारी विचारों से बचाती है। यह हमें सहिष्णु बनाती है, क्योंकि जब हम तर्क से सोचते हैं तो दूसरों की राय सुनने का धैर्य भी आता है। विज्ञान सिखाता है कि हर चीज को जांचो, परखो, पर किसी पूर्वाग्रह से नहीं। यही तर्क, संवाद और विवेक लोकतंत्र की आत्मा भी है।
देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दरकार
भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया को चकित किया है। हमने चंद्रयान और गगनयान भेजे, कोविड वैक्सीन बनाई, डिजिटल क्रांति का नेतृत्व किया। पर दूसरी ओर, आज भी लोग इलाज के बजाय झाड़फूंक कराते हैं, और सोशल मीडिया पर फैले छद्म विज्ञान पर भरोसा कर लेते हैं। स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन विज्ञान की सोच नहीं सिखाई जाती। विज्ञान एक विषय बन गया है, विचार नहीं। यही सबसे बड़ी कमी है।
ऐसे विकसित किया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण
जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शिक्षा, मीडिया और राजनीति में मूल मूल्य की तरह नहीं अपनाते, तब तक समाज केवल तकनीकी रूप से आधुनिक रहेगा, सोच के स्तर पर नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए यह सवाल इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें सचमुच एक तर्कशील, आधुनिक और मानवीय भारत बनाना है, तो हमें निम्न स्तरों पर काम करना होगा –
शिक्षा-स्कूलों में विज्ञान को केवल प्रयोगशाला तक सीमित न रखकर जीवन से जोड़ना होगा। बच्चों को प्रश्न पूछने, तर्क करने और प्रयोग करने की आज़ादी देनी होगी। अध्यापक को “उत्तर देने वाला” नहीं, बल्कि “जिज्ञासा जगाने वाला” बनाना होगा।
मीडिया-टीवी चैनलों और सोशल मीडिया को तथ्यों पर आधारित कार्यक्रमों और अभियानों को प्राथमिकता देनी होगी। ‘मिथक बनाम विज्ञान’, ‘फेक न्यूज़ बनाम फैक्ट’ जैसे कार्यक्रम समाज में विवेक को मजबूत कर सकते हैं। नीतियों और नेतृत्व में वैज्ञानिक सोच-नीति निर्माण डेटा और शोध पर आधारित हो, न कि भावनात्मक भाषणों पर। राजनीतिक नेताओं को विज्ञान और तर्क को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि जनता उनकी दिशा में चलती है।
समाज और परिवार का योगदान-परिवार में बच्चों को अंधविश्वास के बजाय प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए भी तर्क को स्थान दें। समाज में वैज्ञानिक उपलब्धियों और खोजों का उत्सव मनाएं — जैसे हम त्योहार मनाते हैं।
राजेश जैन