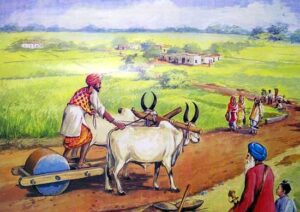उत्तर प्रदेश के कुलाधिपति ने समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पत्र जारी कर कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी तथा बायोमीट्रिक प्रणाली से इसकी निगरानी करने को कहा है। न्यूनतम उपस्थिति पूरा न कर पाने की दशा में विद्यार्थी को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। कुलाधिपति द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की संरक्षक तथा मार्गदर्शक होने के नाते विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के बारे में उनकी चिंता जायज है परंतु जमीनी वास्तविकता यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान ग्रेशम के नियम की चुनौती से जूझ रहे हैं। ग्रेशम के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों के बरअक्स कम गुणवत्ता और अपेक्षाकृत शॉर्टकट तरीके से डिग्री लेने की समानांतर व्यवस्था ने परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
उच्च शिक्षा को सर्वप्रथम चुनौती समानांतर चल रहे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों से मिल रही है। अधिकांश वन डे प्रतियोगी परीक्षाएं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती हैं जिसमें विषय की समझ तथा अभिव्यक्ति कौशल के स्थान पर तथ्यों के रटने से सफलता मिलती है। इनकी तैयारी कराने के नाम पर छोटे छोटे कस्बों में भी कोचिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। इन कोचिंग्स की कक्षाएं उसी अवधि में संचालित की जाती हैं जब उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं गतिमान होती हैं। इसके अलावा इन परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर फाउंडेशन बैच से क्रैश कोर्स तथा प्रैक्टिस सेट तक सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सहजता से उपलब्ध हैं। 2023 में रिलीज तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म ट्वेल्थ फेल भी कोचिंग व्यवस्था को सफलता के लिए जस्टिफाई करती है।
दूसरी प्रमुख चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे ‘इंस्टैंट’ ज्ञान से मिल रही है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया तथा चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स नियमित कक्षाओं के विकल्प में ज्ञान व सूचना के समानांतर तंत्र के रूप में उभरे हैं। यद्यपि यूट्यूब पर ज्यादातर विषयों पर सूचनाओं की भरमार है, फिर भी उसके द्वारा प्रदत्त जानकारी की प्रामाणिकता की जांच करने की कोई स्थापित प्रक्रिया या मेथोडोलॉजी नहीं है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों में ध्यानभंग व एकाग्रता में कमी तथा चिड़चिड़ापन जैसे मनोसामाजिक प्रभाव देखे गए हैं। एआई अभी अपनी आरंभिक अवस्था तथा प्रशिक्षण के दौर में है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ही किसी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है, अतः इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। एआई पर निर्भरता रचनात्मकता में कमी कर रही है यद्यपि इसके दुष्प्रभावों का सही सही आकलन होना अभी बाकी है। इसके अलावा किताबों तथा नोट्स के पीडीएफ की सहज उपलब्धता ने भी महाविद्यालय के पुस्तकालयों की आवश्यकता को कमतर किया है।
तीसरी चुनौती अपेक्षाकृत जटिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) के अनुरूप लागू की गई उच्च शिक्षा प्रणाली के बरअक्स प्राइवेट परीक्षा प्रणाली से है। मसलन, उत्तर प्रदेश के नैक द्वारा ‘ए’ ग्रेड प्रदत्त एक विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी की सेमेस्टर प्रणाली के साथ साथ प्राइवेट परीक्षा प्रणाली को बनाए रखा गया है, जबकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल या दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रम को लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जा रही। जहां एनईपी के अंतर्गत विद्यार्थियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखने की शर्त के साथ वर्ष भर चलने वाली सतत आंतरिक मूल्यांकन पद्धति, प्रयोगात्मक परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट परीक्षा को न्यूनतम समय में गाइड तथा कुंजियों के सहारे पास किया जा सकता है। ऐसे में केवल डिग्री पाने के लिए प्राइवेट परीक्षा एक ज्यादा सरल विकल्प होगा।
एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था में ग्लोबल और लोकल का समन्वय होना चाहिए और शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए परन्तु व्यवहार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। पाठ्यक्रम के निर्धारण, प्रवेश तथा परीक्षा के संबंध में लगातार ‘ऊपर’ से निर्देश भेजे जाते हैं और शिक्षण संस्थानों द्वारा उन निर्देशों के यथातथ्य पालन की उम्मीद की जाती है। संभवतः इस कारण ज्यादातर विश्वविद्यालयों की विद्वत परिषद तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप पाठ्यक्रमों को संशोधित नहीं किया। इसी प्रकार प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट जारी करने का अधिकार पहले महाविद्यालयों से निकाल कर विश्वविद्यालय को दे दिया गया और अब समस्त प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के स्थान पर केंद्रीकृत समर्थ पोर्टल द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश में देरी तथा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
विद्यार्थियों में यह भावना बढ़ती चली जा रही है कि डिग्री व रोजगार में सीधा संबंध नहीं है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा तीन से दस साल तक उच्च शिक्षा में लगाने के बाद भी वह अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में ही रहता है। दूसरी ओर स्टार्ट अप्स तथा रोजगार के कुछ ऐसे क्षेत्र भी उभरे हैं जिनमें औपचारिक डिग्री के अधिक ‘स्किल’ का महत्व है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ सफल उद्योगपतियों तथा सीईओ के कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बारे में प्रचारित करके उनका महिमामंडन किया जाता है। सोशल मीडिया को अपनी जानकारी का मुख्य स्रोत मान बैठी पीढ़ी ने इसे सच मानते हुए उच्च शिक्षा को उपादेय मानना कम कर दिया है।
इन सब कारणों का सम्मिलित असर है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थित घटती और औपचारिक शिक्षा के प्रति अरुचि बढ़ती जा रही है। व्यवस्था की ओवरहॉलिंग के लिए इस कम गुणवत्तापूर्ण समानांतर शिक्षा व्यवस्था पर लगाम कसनी होगी, डिग्री को रोजगार से जोड़ना होगा तथा अकादमिक व प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अन्यथा हम चाहे उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक भले ही कर लें, वैश्विक तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा।
पीयूष त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर, डी एन कॉलेज ,गुलावठी, बुलंदशहर