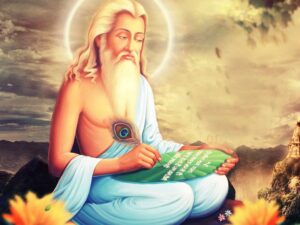आगामी 7 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति अपने पूर्वजों को भी श्रद्धा से स्मरण करने की परंपरा है। भाद्रपद मास की समाप्ति और आश्विन मास के आरंभ अर्थात ऋतु संधि के अवसर पर सर्वश्रद्धया दत्तं श्राद्धम् ( जो कुछ श्रद्धा से किया जाए वह सब श्राद्ध) कहलाता है। श्रत् नामक वृत्ति को धारण करने का नाम श्राद्ध कहलाता है। इसी श्राद्ध भाव से संबंध रखने के कारण आश्विन का कृष्णपक्ष श्राद्ध पक्ष कहलता है। इसमे परिजन अपने पुरखों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनेक लोक प्रचलित पद्धतियां हो सकती है। दुनिया भर में अपने पूर्वजों की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए कुछ करने का प्रचलन है। हमारे अपने देश के हर समाज में, हर वर्ग में पुरखों के नाम पर यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय आदि किया जाता है। यहां भूखों को भोजन कराने, जरूरतमंदों की मदद करने की प्रथा रही है। बेशक कालान्तर में कर्मकांड इतने हावी हो गये कि वह अपने उद्देश्य से इतर सक्रिय हो गई। सद्इच्छा पर दबाव हावी हो गया। अनेक बार तो ऐसा न कर पाने पर सामाजिक बहिष्कार तक की नौबत आने लगी जिससे श्राद्ध के प्रति धारणा बदलने लगी। अनेक मत, अंध विश्वास तो इसे कोरा कर्मकांड और पाखंड तक कहने लगे। इन तमाम विरोधाभासों के बीच मेरे जैसे व्यक्ति का मत है कि आज की भागम-भाग की जिन्दगी में हम स्वयं को भूल रहे हैं। न समय पर सोना, न समय पर जागना। अपने परिजनों संग कब भोजन किया था, यह भी याद नहीं। ऐसे में अपने पूर्वजों, अपने जनक -जननी,उनके साथ बिताये मधुरम पलों को स्मरण करने का समय किसके पास है।
पितृपक्ष को यदि कर्मकांड अथवा धार्मिक अनुष्ठान न भी माने तो भी अपने अतीत अर्थात् अपने पूर्वजों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए स्वयं परिवार सहित खीर-पूरी खाना अपराध नहीं हो सकता। अब यदि इसमें अपने मित्रों, के अतिरिक्त किसी जरूरतमंद को भी शामिल करते हैं तो उस पर्व का महत्व साकार होता है। किसी वृद्धाश्रम अथवा अनाथाश्रम में जाकर वहां रहने वालों की ज़रूरतें पूरी करना अथवा अपने अड़ोस पड़ोस के किसी मेधावी छात्र की मदद करते हुए श्राद्ध और श्रद्धा को वर्तमान संदर्भ में महसूस किया जा सकता है। केवल मनुष्य की नहीं, अपने परिवेश के जीवों- जंतुओं के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझने का संकल्प भी श्राद्ध और श्रद्धा को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब यदि हम परम्परा की बात करें तो यह कहा जाता है कि अपने पुरखों के निमित्त कुछ करने से वह उस दिवंगत आत्मा को प्राप्त होता है। इस बात से किस इंकार होगा कि बिना किसी दबाव, मजबूरी के सहर्ष अपने पुरखों के नाम पर पुण्य कार्य करने वाले के मन को असीम शांति मिलती है। व्यक्ति स्वयं को कृतकार्य मानने लगता है।
पुराणों में श्राद्ध की व्याख्या है। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी ऋषियों से कहते हैं- हे ऋषिवृंद ! परमेष्ठि ब्रह्मा ने पूर्वकाल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्माजी ने कहा हैः ‘जो लोग मनुष्यलोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे, उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे।’
ब्रह्म पुराण के अनुसार श्रद्धा और विश्वासयुक्त किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई जल की नन्हीं-नन्ही बूंदो से पशु-पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों को पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, वे सम्मार्जन के जल से ही तृप्त हो जाते हैं।
भारतीय संस्कृति में जन-जन का यह अटूट विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि जीवन को एक कड़ी के रूप में माना गया है जिसमें मृत्यु भी एक कड़ी है। प्रायः मृत व्यक्ति के संबंध में यह कामना की जाती है कि अगले जन्म में वह सुसंस्कारवान तथा ज्ञानवान बने। इस निमित जो कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं, उसका लाभ जीवात्मा को श्रद्धा से किए गए क्रियाकर्मों के माध्यम से मिलता है, अतः मरणोत्तर संस्कार, श्राद्ध कर्म से उन्हें तर्पण किया जाता है ताकि वे आत्माएं प्रसन्न रहे व उन्हें शांति मिले। श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक कुल 15 दिन की अवधि ‘पितृ पक्ष’ कहलाती है। इसी अवधि में पितरों के प्रति श्रद्धा के प्रतीक श्राद्धों का आयोजन घर-घर में हेाता है। श्राद्धों को लेकर एक पौराणिक घटना महाभारत काल से भी जुड़ी मानी गयी है जिसमें कहा गया है कि कर्ण प्रतिदिन स्वर्ण दान किया करते थे। उन्हें मरणोपरांत स्वर्ग में रहने हेतु ‘स्वर्ण महल’ मिला जहां प्रत्येक वस्तु सोने की थी। कर्ण इससे परेशान हो उठे। जब इसका कारण भगवान से पूछा तो पता चला कि वह प्रतिदिन सवा मन सोना दान करते थे, अन्य वस्तुओं का नहीं। यह जानकर कर्ण को बड़ा संताप हुआ व वे ईश्वर से विनती कर पंद्रह दिन के लिए पृथ्वीलोक में पुनः आए और सभी वस्तुओं का दान किया और मनुष्यों को भोजन करवाया। कहा जाता है कि इस कथा की स्मृति में ही पितरों के प्रति श्राद्ध मनाए जाने लगे।
श्राद्ध के साथ मुख्य रूप से जुड़ी व्यक्ति की श्रद्धा और भावना ही है। इसलिए आज के दिन परिवार के व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से दूर रहकर पुनीत कार्य करेंगे। श्राद्ध कर्म में खर्च किए जाने वाला धन भी ईमानदारी से कमाई किया हुआ ही होना चाहिए। अपने पितरों को पवित्र मन से तर्पण करने हेतु वर्ष में दो दिन शुभ मान गए हैं। प्रथम मृत्यु तिथि पर व दूसरे श्राद्ध के अवसरों पर उसी तिथि पर जिस दिन वह देवलोक को गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि श्राद्ध के दिनों में अपने सभी भूले-बिसरों के लिए अमावस्या का दिन सर्वाधिक अनुकूल है चूंकि इस दिन पितर हमारे काफी नजदीक होते हैं। यदि किसी बाधावश सही दिनों में श्राद्ध न किया जा सके तो एकादशी के रोज भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है जिसका पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। परिवार में तीन पीढ़ियों तक का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने का कर्तव्य पुत्र या निकट परिजन का होता है। श्राद्ध करते समय यह जरूरी है कि अपने पितरों का नाम लेकर ही श्रद्धांजलि दी जाए। साथ ही पवित्र जल हाथ में लेकर जौ, चावल तथा चंदन डालकर आह्नन हेतु कलश स्थापित कर तिल की ढेरी लगाकर उस पर दीपक जलाएं व आस-पास पुष्प रखें। दीपक आटे के ही बनाएं व उनमें शुद्ध घी ही काम में लें। सभी परिजन हाथ में अक्षत लेकर मृतात्मा का आह्वान करें व दीपक की लौ के सामने देखें व बची में (विश्वे देवास मंत्र बोलें, फिर अक्षत छोड़ दें) पितृभ्यो नमः आवाह यामि स्थापायामि का उच्चारण करें। इन मंत्रों के उच्चारण से पितर खुश होते हैं व उन्हें शांति मिलती है। भारतीय दर्शन के मतानुसार मृत्यु के पश्चात मनुष्य का स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है व उसका सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु परलोक सिधार जाती है। श्राद्ध करते समय पितरों के प्रति मौन रखने के अलावा उनकी स्मृति में जनमानस की सेवा हेतु कुछ भी पुनीत कार्य व निर्माण भी करवाया जा सकता है।
भारतीय परंपरा मनुष्य को मरणधर्मा नहीं मानती. जिसे मरना कहा जाता है, वह वस्तुतः नया जीवन पाना है। शरीर जीर्ण हो गया- छोड़ दिया। आत्मा ने नया शरीर वैसे ही पा लिया जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। अच्छी संतान अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करती है। श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह सबसे अच्छा उपाय कहा जाएगा। पुराणों में अपने पुरखों की पुण्यतिथि पर उनको जलांजलि देने का विधान है। साथ ही यह घोषित किया गया है कि पूर्वजों के शुभ कार्यों का स्मरण करके उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेने से बड़ा पुण्य मिलता है। राम ने अपने पूर्वजों को उनके कार्यों के माध्यम से ही स्मरण किया है। पुरखों के पथ पर चलना कुलव्रत का अनुसरण करना कहा जाता है। कुलव्रत का अनुसरण करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब कुलाचार उच्छिंद हो जाते हैं तो वर्णसंकरता आ जाती है।
पूर्वजों की स्मृति में आम, जामुन के फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। कुआं-बावड़ी खुदवाई जाते हैं। विद्या प्रसार के लिए विद्यालय- महाविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। यज्ञ करवाए जाते हैं। द्रव्य-यज्ञ तो संपन्न लोग ही करवा सकते हैं पर भागवत का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप आदि हर कोई कर सकता है। इसी प्रकार के शुभ कार्यों में बलिवैश्वदेव और भूखों को भोजन कराना भी आ जाता है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी दिवंगत आत्माएं कहीं न कहीं विद्यमान रहती हैं। वहां से अपनी संतान को शुभ कार्यों में निरत देखकर आशीर्वाद देती हैं। पितरों के आशीर्वाद फलते हैं।
प्राचीन ब्राह्मणवादि ग्रंथों में देवयान और पितृयाण दो मार्गों का वर्णन मिलता है। पितरों का मार्ग दक्षिणायन मार्ग कहलाता है। इस मार्ग पर चलने वाले विविध कर्मक्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करते हैं। दक्षतापूर्वक कार्य करने को वासुदेव कृष्ण ने योग कहा है- योगः कर्मसु कौशलम्। कुशलतापूर्वक वेदविहित कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। योग का मार्ग भारतीय जीवन पद्धति की मौलिक विशेषता है जिससे प्रत्येक कर्म सर्वश्रेष्ठ बन जाता है और उस पर अपनी सुविधानुसार चलकर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को जितना स्मरण किया जाएगा, उतना ही उनको अपनाने की रूचि जागेगी।
पितृपक्ष के तत्काल बाद शक्ति-साधना के लिए नवरात्र का काल आता है। शक्ति-साधना का फल विजय होता है-कर्मसिद्धि होता है। विजय-दशमी का आगमन इस विकासमय परंपरा का सूचक है। कहा गया है- जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्तित्व यो यच्छद स एव सः। गुरू परंपरा के अनुसार शास्त्राभ्यास और ज्ञानार्जन मनुष्य में दिव्यता का विकास करने वाली विधि है जबकि श्रेष्ठ कर्म करके दक्षिणायन मार्ग को अपनाना जीवन सिद्धि के द्वार खोलने वाली यज्ञ-योगमयी पद्धति है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक पितरों का स्मरण करते हुए श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास करना कोरा कर्मकांड नहीं वर्तमान युग की आवश्यकता भी है।