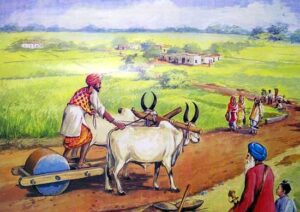उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध और असंवेदनशील विकास किस प्रकार विनाश को आमंत्रित कर रहा है। धराली की यह त्रासदी मात्र एक स्थानीय प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि हिमालय क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब निर्माण, वनों की कटाई, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध और वैज्ञानिक चेतावनियों की अनदेखी का प्रत्यक्ष परिणाम थी। यह घटना पूरे भारतीय हिमालय की उस त्रासद श्रृंखला की अगली कड़ी है जो केदारनाथ, चमोली, जोशीमठ और सिक्किम जैसी आपदाओं से लगातार बनी हुई है।
धराली में जिस बाढ़ ने दर्जनों भवनों, होमस्टे, दुकानों और होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया, वह महज आकस्मिक नहीं थी। स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, यह क्षेत्र न केवल भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है बल्कि इस गांव के नीचे से बहने वाली नदी के किनारे बनाए गए अधिकांश निर्माण फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र में स्थित थे। परंपरागत पहाड़ी घर सदियों से ढलानों पर बनाए जाते रहे हैं ताकि वे बाढ़ और भूस्खलन से बचे रहें किंतु आधुनिक पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था ने इन नियमों को ताक पर रखकर “वॉटरफ्रंट” सुविधा के नाम पर घाटी के सबसे निचले हिस्से को व्यवसायिक उपयोग में ला दिया।
धराली की त्रासदी कोई पहली चेतावनी नहीं है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में आई जलप्रलय ने लगभग छह हजार लोगों की जान ली थी। यह आपदा एक जलवायु-संबंधित तीव्र वर्षा, ग्लेशियर झील के विस्फोट और मंदाकिनी नदी के अचानक उफान का घातक संयोग थी। इसके पश्चात 2021 में चमोली जिले के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा नदी में एक हिमखंड के गिरने से अचानक बाढ़ आई जिसने निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं को तबाह कर दिया और 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस घटना में स्पष्ट रूप से ग्लेशियर के पिघलने और पर्वतीय पारिस्थितिकी के असंतुलन की भूमिका सामने आई। फिर 2023 में जोशीमठ शहर की भूमि में दरारें और धंसाव की घटनाएं हुईं जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए। वहां की वैज्ञानिक रिपोर्टों में बताया गया कि यह संकट भूमिगत जलस्रोतों में बदलाव, अनियोजित निर्माण और पर्वतीय ढालियों के अत्यधिक दोहन का परिणाम था।
केवल उत्तराखंड ही नहीं, सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र ऐसी ही आपदाओं की गिरफ्त में है। वर्ष 2023 में सिक्किम की लोनक झील फटने से अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया। यह झील एक ग्लेशियल लेक थी जो लगातार पिघलते हिमनद के कारण बढ़ती जा रही थी और अंततः अपने ही भार से टूट गई। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहते हैं। 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा ग्लेशियर क्षेत्र में हिमस्खलन से 27 पर्वतारोहियों की मौत हुई जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी पर्वतारोहण दुर्घटना थी। इससे पहले 1998 में मालपा गांव में हुए भूस्खलन में 221 लोग मारे गए थे जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री भी शामिल थे।
इन आपदाओं की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी भूमिका जलवायु परिवर्तन की है। भारतीय हिमालय में स्थित लगभग 9,575 हिमनदों में से बड़ी संख्या तेजी से पिघल रही है। शोध बताते हैं कि बीसवीं सदी के मुकाबले इक्कीसवीं सदी में हिमालयी ग्लेशियर दोगुनी गति से सिकुड़ रहे हैं। इससे पर्वतीय नदियों में अचानक जलप्रवाह बढ़ जाता है और नई-नई झीलें बन रही हैं जो कभी भी फट सकती हैं। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हिमालय में 3,000 से अधिक ग्लेशियल झीलें जोखिम की श्रेणी में हैं जिनमें से लगभग 200 झीलों से तात्कालिक खतरा है। यदि इनका विस्फोट हुआ तो घाटियों में बसे नगर और गांव जलप्रलय की चपेट में आ सकते हैं।
इसके साथ ही विकास परियोजनाएं भी समस्या को बढ़ा रही हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की समीक्षा में वैज्ञानिकों ने बताया कि पहाड़ों की कटाई अत्यंत खड़ी ढालियों पर की गई है जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस परियोजना के कारण 811 से अधिक भूस्खलन सक्रिय हो चुके हैं। पहाड़ियों को 80 डिग्री तक की ढाल पर काटा गया जो इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुसार भी अस्वीकार्य है।
साथ ही साथ वनों की कटाई ने भी संकट को और गहराया है। वनों की अनुपस्थिति में वर्षा का जल सीधा ढलानों से बहकर नदी में चला जाता है जिससे तलछट बढ़ती है और जलधाराओं का मार्ग अवरुद्ध होता है। पारंपरिक जलस्रोत जैसे धाराएं और गूलें सूखती जा रही हैं। पर्वतीय जलसंकट भी अब एक नई आपदा बन चुका है जिससे पहाड़ों के समाज को स्थायी रूप से विस्थापन की ओर धकेला जा रहा है।
इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि हिमालय कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है. यह एक “जीवित पर्वत” है जो अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है। भारत और यूरेशिया प्लेटों की टक्कर से उठे इस पर्वत की चट्टानें अभी भी आकार ले रही हैं जिसका परिणाम है कि यह इलाका भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र-चार में आते हैं। ऐसे में यहां कोई भी निर्माण कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक निगरानी में ही किया जाना चाहिए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिमाचल मामले में टिप्पणी की कि केवल राजस्व की प्राप्ति विकास का उद्देश्य नहीं हो सकती। विकास की योजनाएं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर नहीं बननी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्यों में नए निर्माण कार्यों में भूगर्भीय सर्वेक्षण, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की सहमति को महत्व दिया जाना चाहिए।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हिमालयी क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का एक वैज्ञानिक ऑडिट किया जाए। प्रत्येक सड़क, सुरंग, बांध या होटल परियोजना से पहले उसका भूगर्भीय, पारिस्थितिकीय और जलवायु प्रभाव का आकलन अनिवार्य हो। स्थायी विकास केवल तभी संभव है जब उसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी के साथ तालमेल हो।
हिमालय की चुनौतियों का उत्तर केवल निर्माण नहीं है बल्कि पुनर्चिंतन है। हमें न केवल यह तय करना है कि कहां निर्माण होना चाहिए, बल्कि यह भी तय करना है कि कहां नहीं होना चाहिए। हमें विज्ञान की बात सुननी होगी, पारंपरिक ज्ञान को महत्व देना होगा, और हिमालय को एक जैविक इकाई मानकर उसकी सीमाओं का सम्मान करना होगा। तभी धराली जैसी घटनाओं को दोहरने से रोका जा सकता है वरना यदि हमने सबक नहीं लिया, तो अगला विनाश हमारी दहलीज पर दस्तक देने में देर नहीं करेगा।