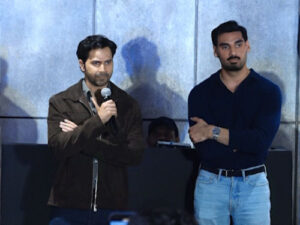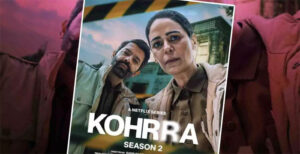अमर गायक मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, दो नाम, दो शैलियाँ, दोनों ही स्वर के साक्षात देवता । जब कभी फिल्मी गीतों में स्वर की कोमलता, भक्ति की गहराई और आवाज के दर्द की पराकाष्ठा की चर्चा होती है, वहाँ महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ स्वतः ही कानों में गूंज उठती है। एल पी , कैसेट , सीडी , डी वी डी से पेन ड्राईव का डीजिटल सफर बदलता
रहेगा पर रफी साहब और किशोर दा हर माध्यम में अपनी मर्म स्पर्शी आवाज के कारण ये दोनो महान गायक अमर बने रहेंगे । अच्छे से अच्छे गीतकार के शब्द तब तक बेमानी होते हैं, जब तक उन्हें कोई संगीतकार मर्म स्पर्शी संगीत नही दे देता और हर संगीत तब तक बेमानी रह जाता है जब तक कोई गायक उन्हें अपने गायन से श्रोता के कानो से होते हुये उसके हृदय में नही उतार देता . फिल्म बैजू बावरा का एक भजन है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इस अमर गीत के संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूंनी हैं , इस गीत के गायक मो रफी हैं । रफी साहब की बोलचाल की भाषा पंजाबी और उर्दू थी, अतः इस भजन के तत्सम शब्दो का सही उच्चारण वे सही सही नही कर पा रहे थे . नौशाद साहब ने बनारस से संस्कृत के एक विद्वान को बुलाया ताकि उच्चारण शुद्ध हो. रफी साहब ने समर्पित होकर पूरी तन्मयता से हर शब्द को अपने जेहन में उतर जाने तक रियाज किया और अंततोगत्वा यह भजन ऐसा तैयार हुआ कि आज भी मंदिरों में उसके सुर गूंजते हैं और सीधे लोगो के हृदय को स्पंदित कर देते हैं . अपने संगीतज्ञ कलाकारो के चलते यह भजन उद्घोष करता है कि संगीत सारी कट्टर पंथी सोच और संकीर्णता से परे खुद एक इबादत है , एक पूजा है ।
मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिले के कोटला गांव में हुआ था .उन्होने अपनी गायकी की बारीकियो से हिन्दी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में अपना स्थान युगो युगो के लिये सुरक्षित कर लिया . उनके समकालीन गायकों के बीच रफी साहब आवाज की मधुरता से विशिष्ट पहचान बना सके . उन्हें शहंशाह-ए-तरन्नुम भी कहा जाने लगा . 1940 के दशक में रफी मात्र अठारह बीस बरस के थे , पर तब से ही वे व्यवसायिक गायक के रूप में पहचान बनाने लगे थे , 1980 में 31 जुलाई को वे हमें छोड़ गये पर इन लगभग ४० वर्षो की गायकी के सफर में उन्होने 26,000 से अधिक गाने गाए. जिनमें मुख्यतः हिन्दी फिल्मी गानों के अतिरिक्त ग़ज़ल, मेरे मन में हैं राम मेरे तन में हैं राम, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बड़ी देर भई नंदलाला जैसे भजन,सूफी ,सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी..जैसे देशभक्ति गीत, नन्हें मुन्ने बच्चे तेरी मुठ्ठी में क्या है, जैसे बाल गीत , क़व्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गाने भी शामिल हैं. उन्होने गुरु दत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, जीतेन्द्र तथा ऋषि कपूर के अलावे स्वयं गायक अभिनेता किशोर कुमार के लिये भी फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमांचक आवाज दी .
कभी कभी किस तरह छोटी सी घटना जीवन में बड़ा मोड़ ले आती है यह मोहम्मद रफ़ी के पहले स्टेज प्रोग्राम से समझ आता है . उनका जन्म अमृतसर, के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनके बचपन में ही उनका परिवार लाहौर से अमृतसर आ गया. जब रफी मात्र सात साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की नाई की दुकान में बैठा करते थे . उधर से रोज गुजरने वाला एक फकीर मधुर स्वर में गाता हुआ निकलता था . नन्हे रफी उस फकीर का पीछा किया करते और उसके जैसा ही गाने का प्रयत्न करते .शायद वह अनाम फकीर ही उनका प्रथम संगीत गुरू था . उनकी गायकी की नकल के स्वर भी लोगों को पसन्द आते . लोग नन्हें से रफी के गाने की प्रसंशा करने लगे. रफी के बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने संगीत के प्रति उनकी रुचि को देख उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को भेजा और इस तरह रफी को विधिवत संगीत की कुछ तालीम मिली . एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक व अभिनेता कुन्दन लाल सहगल कार्यक्रम देने आए थे, श्रोताओ में रफ़ी और उनके बड़े भाई भी थे . अचानक बिजली गुल हो गई जिससे श्रोता बेचैन होने लगे .रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाय . उनको अनुमति मिल गई और बिना बिजली बिना माईक 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का यह पहला सार्वजनिक गायन था .
उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुन्दर भी वहां उपस्थित थे. उन्होने जब नन्हें रफी को सुना तो उन्होने रफी की आवाज के हुनर को पहचाना और उन्होने मोहम्मद रफ़ी को गाने का न्यौता दिया. इस तरह मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच के लिए रिकार्ड हुआ था जिसे उन्होने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था . मुम्बई तब भी फिल्म नगरी थी , देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था , ऐसे समय में युवा रफी ने फिल्मो में पार्श्व गायन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का फैसला लिया और 1946 में वे बम्बई आ गये . धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ही चुना . उन्होने जाने कितने हृदय स्पर्शी भजनो को स्वर देकर यह बता दिया कि भावना , स्वर और संगीत धर्म की सीमाओ से परे नैसर्गिक वृत्तियां हैं .
संगीतकार नौशाद जी ने “पहले आप” नाम की फ़िल्म में उन्हें गाने का अवसर दिया. और उनका फिल्मो में गायन का सफर चल निकला . नौशाद द्वारा संगीत बद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा , फ़िल्म अनमोल घड़ी, 1946 से रफ़ी को हिन्दी फिल्म जगत में प्रसिद्धि मिली. इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी फिल्मो में भी रफ़ी ने गाने गाए जो पसंद किये गये . 1951 में जब नौशाद फ़िल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होने तलत महमूद के स्वर में रिकार्डिंग करने की सोचा पर कहा जाता है कि नौशाद जी ने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से ही गाने को कहा . बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्यधारा गायक के रूप में स्थापित कर दिया . इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में लगातार कई गीत गाने को दिए .
शंकर-जयकिशन की जोड़ी को भी उनकी आवाज पसंद आयी और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना आरंभ कर दिया। शंकर जयकिशन उस समय राजकपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसन्द करते थे किन्तु शंकर जयकिशन की सिफारिश पर रफी साहब की आवाज पर भी राजकपूर ने अभिनय किया . शंकर जयकिशन की जोड़ी ने उनके कम्पोज किये गये लगभग सभी गानो के पुरुष स्वर के लिये रफ़ी साहब को ही मौका दिया. अपनी आवाज के बल पर रफ़ी साहब संगीतकार सचिन देव बर्मन , ओ पी नैय्यर ,रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलिल चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद बन गए.
उनकी असाधारण संगीत साधना के लिये उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री सहित , अनेक बार फिल्मफेयर अवार्ड आदि अनेकानेक सम्मान समय समय पर मिले . इन सम्मानो को प्रदान कर स्वयं सम्मान देने वाले ही उनसे सम्मानित हुये क्योकि रफी साहब का वास्तविक सम्मान तो यह ही है कि उनके इस दुनिया से बिदा हो जाने के वर्षो बाद भी हम उन्हें भुला नही पाते . वे मानवीय मूल्यो के प्रतीक थे .वे सहज सरल और अपने कार्य के प्रति समर्पित अनुकरणीय व्यक्तित्व थे . वे संगीत के पुजारी मात्र नही उसके प्रतिष्ठाता थे .
जब मोहम्मद रफी और किशोर कुमार का जिक्र साथ में किया जाये तो यह कहना ही पड़ता है कि दोनो एक दूसरे से बढ़कर हैं । बहुरंगी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार ऐसे कलाकार थे जिसने न सिर्फ गायकी, बल्कि अभिनय, निर्देशन और लेखन में भी अपने निशान छोड़े हैं । किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था । आभास कुमार गांगुली उर्फ़ किशोर कुमार, एक मस्ती भरी रूह थे। जहां रफ़ी साहब की गायकी दिल पर मरहम का काम करती थी, वहीं किशोर दा की आवाज़ दिल को मस्ती में झूमने पर मजबूर कर देती है । उनकी गायकी में जीवन की उमंग का संगीत है । उनके स्वर में एक अटूट ऊर्जा थी। “जिंदगी एक सफर है सुहाना”, “मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू”, “पल-पल दिल के पास” , ये सिर्फ़ गाने नहीं, पीढ़ियों की धड़कनें हैं। हर हारमोनियम सीखने वाला सर्वप्रथम जिंदगी एक सफर है सुहाना की धुन पर रीड दबाकर प्रसन्न मन से अपनी संगीत साधना में निरत होता है । किशोर दा की खास बात थी , वे कभी भी किसी एक शैली तक सीमित नहीं रहे। वे गाते नहीं थे, गानों को जीते थे। उनकी आवाज़ में नटखटपन, प्रेम, दर्द, और बेफिक्री का एक अनोखा संमिश्रण था। उनकी आवाज़ राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद जैसे हर सुपरस्टार की पहचान बन गई।
रफी और किशोर दा की तुलना नहीं, वे संगीत संगम हैं । सच ये है कि रफ़ी और किशोर की तुलना करना वैसा ही है जैसे कह देना कि चाँद बेहतर है या सूरज। दोनों की अपनी रोशनी है, अपनी छटा है। रफ़ी के गीत आत्मा में गूंजते हैं, तो किशोर के गीत होंठों पर मुस्कान बन कर थिरकते हैं। जहां रफ़ी साहब ‘मन तड़पत हरि दर्शन को आज’ जैसे भक्ति गीतों में शुद्धता की मिसाल देते हैं, वहीं किशोर दा ‘ए मेरी टोपी पलट के आ’ जैसे गीतों में हंसी का तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, पंचम दा , और एस.डी. बर्मन , सभी ने दोनों महान गायकों की प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। एक ही गायक से हर भाव गवाना आसान नहीं होता, लेकिन इन दोनों ने इसे मुमकिन बना दिया।
इन अमर गायकों में एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान की भावना दिलचस्प है । रफ़ी और किशोर दा के बीच कभी कोई ईर्ष्या नहीं थी। वे एक-दूसरे की गायकी का बेहद सम्मान करते थे। जब किशोर दा के संघर्ष के दिन थे, तब रफ़ी साहब ने उन्हें प्रोत्साहित किया और जब किशोर दा को सफलता मिली, उन्होंने कभी रफ़ी साहब को पीछे नहीं बताया। वो दौर था जब दोनों की आवाजें रेडियो पर, कैसेट पर, सिनेमा हाल में, गली-गली में गूंजती थीं । लोग दोनों को सिर आँखों पर बिठाते थे।
13 अक्टूबर 1987 को किशोर दा भी इस दुनिया को अलविदा कह गए पर क्या वे सचमुच चले गए? जब भी रेडियो पर “ये रेशमी जुल्फें” या “आज मौसम बड़ा बेईमान है” बजता है, लगता है जैसे वो यहीं कहीं हैं । हमारी सांसों में, हमारी स्मृतियों में। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में भी कोई गायक ऐसा नहीं, जो इन दोनों के प्रभाव से अछूता हो। अरिजीत सिंह से लेकर सोनू निगम तक, सबने कभी न कभी स्वीकारा है कि उन्होंने रफ़ी और किशोर दा से बहुत कुछ सीखा है।
ये एआई जनरेशन है । हमें विस्मय नहीं होगा यदि कोई साफ्टवेयर कभी फिर से इन महान गायकों की आवाज में नये गीत प्रस्तुत कर सके किन्तु यह भी सच है कि कितना भी परिष्कृत इलेक्ट्रानिक गीत संगीत हो स्वर की मौलिक लचक और बांकपन किशोर दा तथा रफी साहब की मौलिकता है । रफ़ी और किशोर न सिर्फ़ गायक थे, वे संगीत का एक युग थे , एक एहसास हैं । वे ऐसे सितारे थे जो दिन रात कभी भी ढ़लते नहीं , लगातार चमकते रहते हैं ।