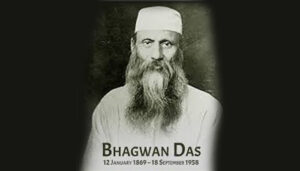डॉ.नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी
कथावाचन कौन कर सकता है और कौन नहीं कह सकता है, आजकल इस संबंध में चारों ओर से बड़ा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। इस संदर्भ में अमूमन दो वर्ग सामने आए हैं – एक वर्ग कहता है कि कोई भी कथा कह सकता है, और दूसरा वर्ग कहता है कि कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों का है। पहला वर्ग थोड़ा उदार है, लिबरल है, और कथा कहने को सबकी आज़ादी मानता है। दूसरा वर्ग दकियानूसी, जातिवादी, परंपरावादी, लकीर का फ़कीर है, वह कथा वाचन को केवल ब्राह्मणों की जागीर समझता है। इन दोनों वर्गों में कोई मेल नहीं है।साथ ही एक तीसरी बात भी निरंतर सामने आ रही है जो ‘मनुस्मृति’ की गई बीती बातों को सही सिद्ध करने में लगी हुई है। आश्चर्य है कि ऐसी बातों का जिस त्वरा के साथ प्रतिकार होना चाहिए, नहीं किया जा रहा है। वे बातें ऐसी हैं जो, जिन परम्पराओं की संवैधानिक स्तर पर तिलांजलि दी जा चुकी है जिनके कारण समाज गर्त में चला गया था, उनके ही पुनर्स्थापना की बात करती है और संविधान से संचालित इस देश में जिसे खुले तौर पर निर्लज्जता के साथ बेरोक बेटोक प्रस्तुत भी किया जा रहा है।
भारत ऋषियों का देश रहा है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। भारत का आध्यात्मिक इतिहास पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की यही आध्यात्मिक दृष्टि ही उसे विश्व गुरु बनाती है – एक ऐसी भूमि जो सृष्टि के प्रत्येक जीव का कल्याण चाहती है। इतनी ही गौरवशाली इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है जो भिन्न-भिन्न तरह से प्रकट हुई है मगर इसी मिट्टी में ऐसे तत्त्व भी मौजूद हैं जो उस विरासत को न तो समझते हैं और न ही उनका अनुकरण करने की ज़रा भी मंशा रखते हैं।
वर्तमान में जो कुछ भी भारतीय समाज में चारों ओर घटित हो रहा है, उसका अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिन-ब-दिन लोगों के बीच की खाइयाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सौहार्द मिटता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जैसे किसी भी मसले पर दृढ़ता के साथ जो बातें रखी जानी चाहिए, या तो वे रखी नहीं जाती हैं या उसे रखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं।
इस संबंध में यह भी हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को भी छोटा समझना बहुत ही घातक सिद्ध होता है क्योंकि उसका प्रतिकार या प्रतिफलन केवल इसी रूप में प्रायः फलित होगा कि जब अमुक व्यक्ति या वर्ग अवसर प्राप्त करता है तो वह उनको (जिन्होंने उसे छोटा बनाया गया या जाताया गया) छोटा सिद्ध करके ही दम लेगा। प्रतिशोध या प्रतिकार से प्रेम कभी फलित नहीं होता है।
आजकल कथावाचकों के संबंध में जो चर्चा चल रही है वह बड़ी हास्यास्पद है और यह लोगों के पास भारत के विरासत की सांस्कृतिक समझ कितनी है, इसका भी परिचय देती है। भारत की ऋषि परम्परा ने अज्ञात को अनुभव से जाना। अज्ञात इतना विराट है, इतना आलोकित है कि उसमें जीवन की सारी पीड़ा भस्मीभूत हो जाती है। सारे दंश, सारे कष्ट, अज्ञान सब मिटे जाते हैं।
अज्ञात से प्राप्त उस परम अनुभव को ऋषियों ने कहानियों में पिरोया। प्रतीकों में गढ़ा। उसे मूर्तियों में ढाला। तीर्थों में तराशा। उसे महाकाव्यों में गुथा। उसे वाणी के माध्यम से सबमें बाँटा मगर प्रश्न यह है कि ऋषियों ने जब परम का अनुभव किया तो उसे दूसरों को बताने की फ़िजूल ज़हमत में क्यूँ पड़ गए? क्योंकि इसी बताने में ही तो सारे फ़साद की जड़ मौजूद है।
इस विराट का अनुभव इतना आनन्ददायी होता है कि यह हमें समझ लेना चाहिए कि बिना बताए रहा नहीं जा सकता है। सूली पर लटका जा सकता है; ज़हर पिया जा सकता है; गला स्वयं का कटवाया जा सकता है; बस चुप भर नहीं रहा जा सकता है। इसी अनुभव को तो उपनिषदों ने – सत्-चिद-आनन्द कहा है। इसे ही तो गीता में भगवान कृष्ण ने श्रेष्टता का शिखर बताया है – जीवन के हर आयाम में श्रेष्टतम की अनुभूति।
क्या यह समझने में किसी को कोई भी कठिनाई हो सकती है कि जब भी किसी के जीवन में अच्छे अनुभव आते हैं तो वह सबके साथ बाँटना चाहता है, और अगर कटु अनुभव आते हैं, तो उन्हें छुपा लेना चाहता है। ओशो ने कहा है – “सुख फैलता है; दुख सिकोड़ता है।” इसलिए दुख में निरंतर जीने वाला व्यक्ति एक दिन जीवन से मुक्त होना चाहता है। सुख की राह पर चलने वाला फैलता जाएगा और एक दिन ब्रह्म को उपलब्ध होगा। क्योंकि भौतिक सुख की चाह भी अंततः आध्यात्मिक सुख की चाह में परिवर्तित होगी ही यदि वह चाह ठीक-ठीक मार्ग पर आरूढ़ रह जाए।
हम जानते हैं कि आदमी सामान्यतः अपने अच्छे अनुभवों को संरक्षित रखता है; बुरे अनुभवों को छोड़ता चला जाता है। तभी तो वह ज़िंदगी को जीने लायक बना पाता है। दुख में बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता है। दुख को बदलना ही पड़ता है। बुद्ध ने भी जब दुख का समग्रीभूत अनुभव किया तो उसे परिश्रम, साधना और तप से बदल लिया। और फिर उन्हें जो विराट का अनुभव हुआ उसे बाँटना शुरू किया।
क्या हमें याद नहीं कि उन्होंने चार आर्य सत्यों के उपरांत किन सूत्रों को प्रतिपादित किया था? उनका अंतिम सूत्र था – “संघम शरणं गच्छामि।” संघ क्या है? संघ में होता क्या है? संघ एक धारा के लोगों का समूह होता है – एक ऐसी धारा जो इस परम की खोज करती है; जो भौतिक से तृप्त नहीं होती है; जो दैहिक के पार देखने में लगी रहती है। संघ में लोगों का ध्यान मन से अमन की ओर निर्दिष्ट रहता है।
इस पूरी भाव-भूमि को जो अनुभव के तल पर समझता है, जीता है, और कहना जानता है वह इस विराट की कथा कह सकता है। क्योंकि अनुभव कर लेने मात्र से कहने की कला विकसित हो जाती है, ऐसा नहीं है। पढ़ लेने मात्र से पढ़ा लेना नहीं आ जाता है। क्या हमने अपनी कक्षाओं में अच्छे और खराब टीचर नहीं देखे हैं? अच्छा टीचर वह होता है जो अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाने की कला जानता है। और खराब टीचर वह होता है जो यह काम बखूबी नहीं कर पाता है।
इसलिए पढ़ तो सभी सकते हैं, पर पढ़ा सभी नहीं सकते। विराट का अनुभव भी कर तो सभी सकते हैं, मगर करा भी पाएं, यह बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे पढ़ लेने मात्र से पढ़ा लेने का कोई संबंध नहीं है वैसे ही अनुभव कर लेने मात्र से अनुभव करवाने की कला का विकसित हो जाए, इसका कोई संबंध नहीं है।
क्या हमें अब यह समझने में कोई कठिनाई है कि इस अज्ञात विराट को जिसने अनुभव कर लिया, उसे हम क्या कहेंगे? शायद इन्हें हमने ऋषि कहा है मगर क्या हम उन लोगों को भी ऋष्टि कहेंगे जो इस अनुभव से नहीं गुज़रे हैं? शायद हम ऐसे लोगों को ऋषि नहीं कहेंगे। फिर ऋषि कौन है – वह जो ब्रह्मांड को अनुभव करता है, एकत्व महसूस करता है; वह, जो शून्य है, उसमें स्वयं को पूरा निमज्जित पाता है, या वह जो सिर्फ़ इन अनुभवों की कहानियाँ कहता है और वह भी बिना स्वयं विराट के अनुभव से स्वयं गुज़रे? क्या, ऋषि किसे कहेंगे, इसे समझने में किसी को कोई कठिनाई हो सकती है?
कबीर ने ऋषि के लिए पंडित शब्द का प्रयोग किया है – “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।” ऋषि को हम पंडित भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी कह सकते हैं, सद्गुरु भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं बस वह ऋषि होना चाहिए यद्यपि हमारी परम्परा में अलग-अलग शब्दों को अलग-अलग व्याख्यायित किया गया है।
मगर इन सबके बावजूद जिसे विराट का अनुभव नहीं, जो शून्य की खोज में नहीं, क्या उसे हम ऋषि या ऋषित्व के मार्ग पर चलने वाला कभी कह सकते हैं? शायद नहीं। इस पृष्ठभूमि के साथ हमें यह समझने में क्या कोई कठिनाई है कि समाज के तल पर आज वास्तविकता में क्या घट रहा है? क्या यह किसी से छुपा है? क्या प्रभु का गीत गाने वाला सचमुच प्रभु के मार्ग पर नज़र आ रहा है? क्या प्रभु का गीत किसी सीमा रेखा में बँध सकता है, बाँधा जा सकता है? क्या प्रभु की खोज किसी वर्ग विशेष से संबंधित है यह संभव है? इसका उत्तर देने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या हमें अब कोई समस्या है यह समझने में कि कौन प्रभु की कथा कर सकता है और कौन नहीं? क्या प्रभु की कथा कहना किसी जाति विशेष से किसी भी रूप में संबंधित हो सकता है? क्या प्रभु की कथा कहना किसी को ‘ब्राह्मण’ नहीं बना देता? क्या कथा ब्राह्मण कहता है या जो कह सकता है उसे ब्राह्मण कहा जाना चाहिए? क्या है ब्राह्मण की परिभाषा?
मनुस्मृति ने तो जन्म से सभी को शूद्र कहा – “जन्मना जायते शूद्र।” मगर मनुस्मृति के इस सूत्र को छोड़कर ही अक्सर सारी व्याख्या की जाती है। तो क्या जब सभी जन्म से शूद्र हैं, तो फिर स्वयं को शूद्र से इतर समझ लेने वाले लोग कौन हैं? जन्म से तो कोई कुछ और हो ही नहीं सकता है सिवाय शूद्र होने के। कुछ और होने का कोई उपाय भी नहीं है। शायद शूद्र है, इसलिए जन्म भी हुआ है।
शास्त्रों की मानें तो ब्राह्मणों का तो जन्म होता ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है। ब्राह्मण मतलब जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो भवसागर के पार हो गया – अब न जिसकी मृत्यु है, और अब न जिसका जन्म है। इसलिए ब्राह्मण या ब्राह्मण मार्ग पर तो वही हो सकता है जो प्रभु (विराट) के प्रति अभीप्सा से भर गया हो। क्या इसके सिवाय कोई और पात्रता की ज़रूरत हो सकती है? क्या यह समझने में कोई भी कठिनाई हो सकती है कि वास्तविकता में ब्राह्मण कौन है? जन्म से तो कोई होता नहीं है; कर्म से हो सकता है। और कर्म किसी परिधि को नहीं जानता है। परिधियों में सीमित समाता है, असीम नहीं। और असीम का ही बस प्रभु से लेना-देना है; सीमित तो असीम को भी बस सीमित ही कर सकता है, करता है।
तो प्रभु की कथा कौन कह सकता है – क्या इसे समझने में किसी गलती की कोई गुंजाइश है? क्या लिबरल्स की बात ठीक है कि प्रभु की कथा कोई भी कह सकता है। क्या कोई भी किसी से भी इलाज़ करवा सकता है? क्या कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफ़ेसर से ऑपरेशन करवा सकता है? आप कहेंगे बिलकुल नहीं। मगर वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है तब भी आपका जवाब नहीं में ही देंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने समझदार तो हैं कि हिंदी का प्रोफ़ेसर सर्जरी नहीं कर सकता। तो किसी वर्ग का क्या यह कहना कि कथा कोई भी कह सकता है, सही है? उसके ऐसे कहने पर वह तालियाँ ज़रूर बटोर सकता है, वाह वाही ज़रूर लूट सकता है, मगर उसकी बात कितनी व्यर्थ है क्या इसे समझने में कोई समस्या किसी को हो सकती है? यह कहने में वह भगवान की भी जाति देख लेता है, और अमुक व्यक्ति (कथावाचक) से जोड़ देता है, इस बात की बिना परवाह किए कि और जातियों में जो लोग पैदा हैं, क्या वे विराट के अनुभव के अनुभागी नहीं हैं? मगर ये बातें उसकी सोच के दायरे से परे हैं।
दूसरा वर्ग जो वंशानुगत तरीके से कथा वाचन को एक विशेष वर्ग से संबंधित करता है, क्या उसे आप सही कह सकते है जो हर कर्मकांड को धर्म मानता है, जिसका प्रतीकों के पीछे छुपे संदेशों से कोई सरोकार नहीं होता है, या जो जन्मगत आधार पर अपनी सुप्रीमेसी को नहीं छोड़ना चाहता, उसे कायम रखना चाहता है? क्या आप कह सकते हैं कि विराट का अनुभव विभेदकारी है; यह सबको अनुभव नहीं हो सकता है? या क्या आप यह कह सकते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा या उसकी आने वली सन्ततियाँ सब डॉक्टर बनेंगी? उसकी तरह से ही इलाज़ करने के काबिल होंगी? शायद आप ऐसा नहीं कह पाएंगे?
मैं अपनी सारी बातें ‘शायद’ लगाकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बातें परम सत्य नहीं हैं, इसका मुझे ज्ञान है, और शायद इसलिए भी लगा रहा हूँ ताकि जो समाज में आज चल रहा है और जो मेरी बातों से अन्यथा है, वह भी है, इसकी जगह सदा बनी रहे। और शायद मेरे कहने से वह लाख गुना ज़्यादा ही है। मैं और मेरे जैसे कहने वाले तो कहीं हैं भी नहीं। मैं उनको भी स्पेस दे रहा है, जिनकी वजह से मैं लिख रहा हूँ। मगर सवाल यह है कि क्या वे मेरी वजह से कुछ सकारात्मक करेंगे, मेरे जैसे को जगह दे सकेंगे? ‘हाँ’ कहना कठिन है खासकर तब जब, जिस विराट के नाम पर सारा कुछ चल रहा है, उसे ही ठीक से जैसा वह है, जगह न मिल पाई हो।
तो पहली बात कि प्रभु कथा सब नहीं कह सकते; और दूसरी बात कि प्रभु की कथा सिर्फ़ वे ही कह सकते हैं जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या (किसी बुद्ध, कृष्ण, कबीर, रैदास, नानक, ओशो, कृष्णमूर्ति की तरह) प्रभु प्राप्ति की मंज़िल तक पहुँच चुके हैं। ब्राह्मण की संज्ञा सिर्फ़ उन्हें ही दी जा सकती है जो ब्रह्म प्राप्ति की राह पर चल रहे हैं या ब्रह्म जिन्हें प्राप्त हो चुका है। तीसरी बात प्रभु किसी जाति के नहीं हैं, और न किसी धर्म के। जब सब जाति, धर्म, विशेषण मिट जाते हैं, सब शून्यस्थ हो जाता है, तभी तो ब्रह्म का अनुभव होता है, तभी तो कोई ब्राह्मण कहलाने की श्रेणी अर्जित करता है अन्यथा सारे शूद्र हैं, और उनके जीवन में जब भी विवेक जन्म लेगा, तो वे ब्राह्मणत्व की ओर यात्रा करेंगे।
ब्राह्मण हो जाना इस जीवन का सबसे सुंदर, श्रेष्ठ मगर दुरूह कार्य है। ब्राह्मणत्व की उपलब्धि एक अर्जन है। यूँ ही खैरात में ये किसी को नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है वह भी सिर्फ़ ब्राह्मण होने की यात्रा में ही हो सकता है क्योंकि जो ब्राह्मण हो जाता है, वह तो वापस आता ही नहीं, आ सकता भी नहीं। मगर इन गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को समझे बिना जब बातों का कुचक्र शुरू होता है, तो कुतर्कों का जाल बुन लिया जाता है, जिससे निजात पाना कभी संभव नहीं हो पाता। यह कुचक्र आदमी आदमी के बीच केवल और केवल घृणा और वैमनस्य को जन्म देता है जिसकी परिणति बहुत भयावह होती है। क्या इन सबको हमारे चारों ओर देख पाने में कोई कठिनाई है? क्या चीज़ों को जो होना चाहिए उससे इतर होता नहीं देखा जा रहा है? क्या समाज में जो चल रहा है वह सचमुच न्याय संगत है; इसे समझने में कोई दिक्कत हो सकती है?
ठीक को ठीक से समझ लेना गलत को ठीक कर लेने का सबसे सटीक उपाय है। न कोई और उपाय था, न कोई और उपाय होगा।
इसे जितना जल्दी समझ और समझा लिया जाए, उतना ही बेहतर है वरना प्रभु की यह दुनिया निरंतर अवनति की राह पर आगे तो बढ़ ही रही है। इसे बचाना हमारा धर्म है। हम सभी को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए।