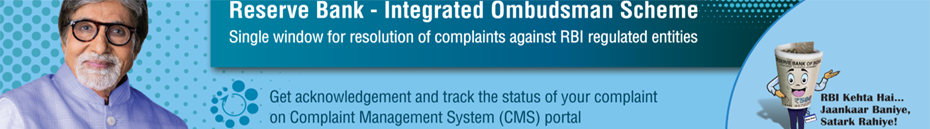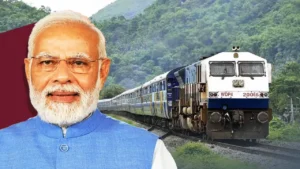भारत की अर्थव्यवस्था में आय की असमानता एक गंभीर विषय बन गई है। इससे समाज और राष्ट्र का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए आय का समान वितरण आवश्यक है। असमान आय से क्रय शक्ति प्रभावित होती है और आर्थिक असंतुलन बढ़ता है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है। सम्पत्ति चंद हाथों में सिमटती जा रही है। इसका परिणाम आम आदमी की बिगड़ती हालत के रूप में सामने आ रहा है।
यह खुशी की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और यह विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश अभी भी पीछे है। विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 140वें स्थान पर है। बढ़ती जनसंख्या और आय असमानता इसके प्रमुख कारण हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है जो वैश्विक आबादी का 18 प्रतिशत है।
वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस के अनुसार भारत में संपत्ति असमानता बढ़ी है। 1961 में 10 प्रतिशत अमीर लोगों के पास कुल संपत्ति का 44.9 प्रतिशत था जो 2023 में बढक़र 64.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार टॉप 0.1 प्रतिशत के पास 1961 में 3.2 प्रतिशत संपत्ति थी जो 2023 में बढक़र 29 प्रतिशत हो गई। भारत की गिनती विश्व के सबसे ज्यादा धन असमानता वाले देशों में से होती है। कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77 प्रतिशत भाग टॉप 10 प्रतिशत लोगों के पास है, जबकि 1 प्रतिशत सबसे अमीरों के पास 53 प्रतिशत संपत्ति है। इसके विपरीत देश के आधे गरीब लोग राष्ट्रीय संपत्ति के मात्र 4.1 प्रतिशत के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
आय असमानता के मामले में भी भारत शीर्ष देशों में है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत और टॉप 1 प्रतिशत के पास 22 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी मात्र 13 प्रतिशत रह गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के गरीब लोगों पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। कर प्रणाली में असमानता स्पष्ट है। भारत में निचले 50 प्रतिशत लोग कुल जीएसटी का 64 प्रतिशत भुगतान करते हैं, जबकि टॉप 10 प्रतिशत का योगदान मात्र 4 प्रतिशत है।
जाहिर है, आय असमानता के गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। कम आय वाले लोगों की क्रय शक्ति सीमित होने से बाजार में मांग घटती है जिससे आर्थिक असंतुलन बढ़ता है। उच्च आय वर्ग विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करता है जबकि निम्न आय वर्ग आवश्यक वस्तुओं तक सीमित रहता है। जब कम आय वाले वर्ग के लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं होती तो उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं की बिक्री घट जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रभावित होती है। आज हमारे देश के बाजारों में इसी तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है।
निम्न आय वाले लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा अनाज, दालें, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं, आवास के किराए या मरम्मत और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा पर खर्च पर खर्च करते हैं। इसके विपरीत मध्यम वर्गीय उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं के साथ-साथ कुछ विलासिता और आराम से जुड़ी स्मार्टफोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ब्रांडेड कपड़े और फैशन से जुड़ी वस्तुओं वस्तुओं और घूमने-फिरने, सिनेमा, रेस्तरां में भोजन पर भी खर्च करते हैं। इसके विपरीत भारत के सुपर रिच की श्रेणी में शामिल लोग लग्जरी वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की ओर से जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय अल्ट्रा-रिच अपनी निवेश योग्य संपत्ति का 17 प्रतिशत लग्जरी वस्तुओं में लगाते हैं जिसमें घडिय़ों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद आर्ट और आभूषण आते हैं। चौथे स्थान पर सुपर रिच लोग क्लासिक कारें खरीदते हैं। इसके बाद लग्जरी हैंडबैग, वाइन, दुर्लभ व्हिस्की, फर्नीचर, रंगीन हीरे और सिक्कों की खरीद हैं। हालांकि, वैश्विक स्तर पर, सुपर-रिच लग्जरी घडिय़ों और क्लासिक कारों के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में विभिन्न आयु समूहों में दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।
शहरों और कस्बों में कम आय के कारण लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और आवास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कम आय वाले लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आय असमानता की वजह से गरीब लोग अवसरों से वंचित हो जाते हैं। वह उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल की कमी के कारण लोग अच्छी नौकरियों और उच्च वेतन वाले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते। बड़े उद्योगों और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे व्यापारियों और कम वेतन पाने वाले श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भिन्नता के कारण कुछ वर्गों को अधिक अवसर मिलते हैं जबकि अन्य वर्ग पीछे रह जाते हैं। आय असमानता से गरीबी बढऩे और इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। गरीबी बढ़ रही है, तभी तो सरकार को 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है।
वैसे सरकार ने बीते साल दावा किया कि देश में 95 फीसदी गरीबी कम हो गई है। केवल 5 प्रतिशत लोग ही अब गरीबी की रेखा से नीचे रह गए हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एनालिसिस के आधार पर यह दावा किया था। यह सर्वे अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान 2,61,746 परिवारों के बीच किया गया। बड़ा सवाल यह है कि अगर 95 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं तो वह 81 करोड़ लोग कौन हैं जो सरकार से फ्री में अनाज प्राप्त कर रहे हैं? आखिर किन लोगों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को आगामी पांच साल के लिए बीते वर्ष जनवरी में ही आगे बढ़ा चुकी है ?
पिछले साल जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.9 करोड़ भारतीय गरीबी का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रतिदिन आय 181 रुपये (2.15 डॉलर) से भी कम है।
सरकार गरीबों को अनाज उपलब्ध करवा रही है। विभिन्न योजनाएं गरीबों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए संचालित की जा रही हैं, यह सराहनीय है। प्रत्येक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है मगर हालात तभी बदलेंगे, जब आय में असमानता खत्म होगी। अभी भारत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 140वें स्थान पर है, इसे जब तक टॉप 10 में नहीं लाएंगे, तब तक हालात बदलने की उम्मीद बेमानी है। आय असमानता दूर करने के लिए सरकार को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग अधिक योग्य बन सकें। उचित कर प्रणाली भी समय की पुकार है। संतुलित कर प्रणाली अपनाकर उच्च आय वर्ग से अधिक कर लेकर निम्न आय वर्ग को राहत दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा से भी असमानता कम करना संभव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर गरीबों को आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करना संभव है। हम शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर ध्यान देकर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं।
आय असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। यदि सरकार और नीति निर्माता इस दिशा में ठोस कदम उठाएं तो क्रय शक्ति मजबूत होगी और संतुलित एवं समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव होगा। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, ऐसे में गरीब तबके को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए नई नीतियां आवश्यक हैं। अन्यथा, भविष्य में देश के समक्ष चुनौतियां और गंभीर होती जाएंगी।
प्रो. महेश चंद गुप्ता
(लेखक प्रख्यात शिक्षा विद्, वक्ता एवं विचारक हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं।)