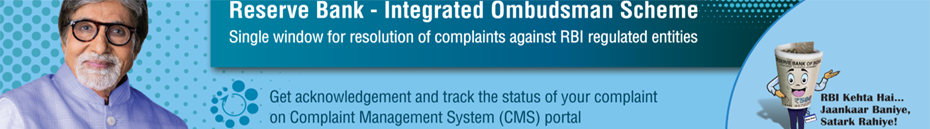अहिंसक विश्व की राह दिखा गए हैं भगवान महावीर, इसलिए हिंसा भाव त्यागिए
Focus News 10 April 2025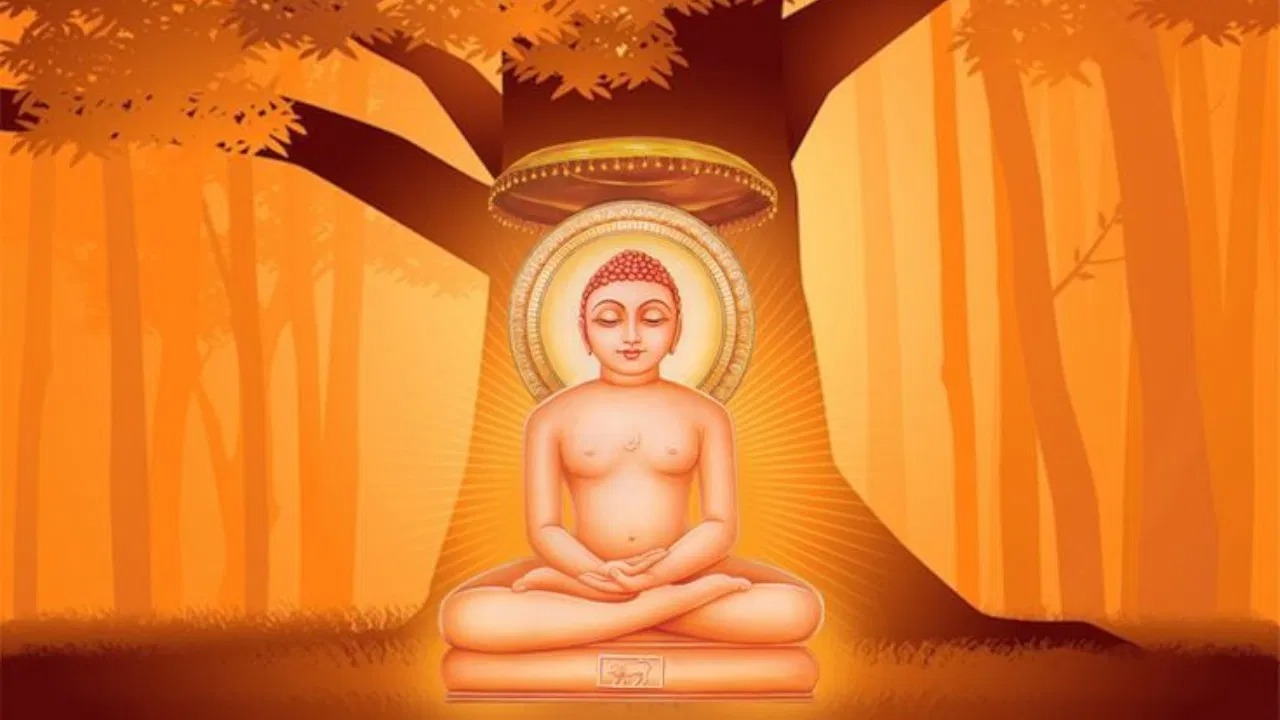
आदिकालीन जैन धर्म में समस्त जीवों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार की कामना की गई है जो व्यापक अर्थों में अहिंसा की अवधारणा को परिपुष्ट करता है। यद्यपि अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। फिर भी इसके पारिभाषिक अर्थ विध्यात्मक और निषेधात्मक दोनों बताए जाते हैं जिनका अपना महत्व है। जहाँ लोगों में सत्प्रवृत्ति, स्वाध्याय, अध्यात्मसेव, उपदेश, ज्ञानचर्चा आदि आत्महितकारी व्यवहार विध्यात्मक अहिंसा की श्रेणी में आते हैं, वहीं उनमें किसी के प्रति रागद्वेषात्मक प्रवृत्ति न करना, किसी का प्राणवध न करना या फिर ऐसी दुष्प्रवृति मात्र का विरोध करना भी निषेधात्मक अहिंसा समझा जाता है|
अहिंसा विषय के मर्मज्ञ बताते हैं कि किसी संयमी व्यक्ति के द्वारा भी यदि अशक्य कोटि का प्राणवध हो जाता है, तो भी वह निषेधात्मक अहिंसा, हिंसा नहीं है क्योंकि निषेधात्मक अहिंसा में केवल हिंसा का वर्जन होता है जबकि विध्यात्मक अहिंसा में सत्क्रियात्मक सक्रियता होती है। इसलिए यह स्थूल दृष्टि का निर्णय है,जबकि इसकी गहराई में पहुँचने पर तथ्य कुछ और ही मिलता है। चूँकि निषेध में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निषेध होता ही है। इसलिए निषेधात्मक अहिंसा में सत्प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्यात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होता है।
वास्तव में हिंसा न करनेवाला यदि आँतरिक प्रवृत्तियों को शुद्ध न करे तो वह अहिंसा न होगी। इसलिए निषेधात्मक अहिंसा में सत्प्रवृत्ति की अपेक्षा रहती है, वह बाह्य हो चाहे आँतरिक, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। सत्प्रवृत्यात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होना आवश्यक है। इसके बिना कोई प्रवृत्ति सत् या अहिंसा नहीं हो सकती, यह निश्चय दृष्टि की बात है। व्यवहार में निषेधात्मक अहिंसा को निष्क्रिय अहिंसा और विध्यात्मक अहिंसा को सक्रिय अहिंसा कहा जाता है।
जैन ग्रंथ आचारांगसूत्र में, जिसका समय संभवत: तीसरी चौथी शताब्दी ई. पू. है, अहिंसा का उपदेश इस प्रकार दिया गया है : भूत, भावी और वर्तमान के अर्हत् यही कहते हैं-किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी जंतु को, किसी भी वस्तु को जिसमें आत्मा है, न मारो, न (उससे) अनुचित व्यवहार करो, न अपमानित करो, न कष्ट दो और न सताओ। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब अलग जीव हैं। पृथ्वी आदि हर एक में भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व के धारक अलग-अलग जीव हैं। उपर्युक्त स्थावर जीवों के उपरांत न्नस (जंगम) प्राणी हैं, जिनमें चलने फिरने का सामर्थ्य होता है। ये ही जीवों के छह वर्ग हैं।
इनके सिवाय दुनिया में और जीव नहीं हैं। जगत् में कोई जीव न्नस (जंगम) है और कोई जीव स्थावर। एक पर्याय में होना या दूसरी में होना कर्मों की विचित्रता है। अपनी-अपनी कमाई है, जिससे जीव अन्न या स्थावर होते हैं। एक ही जीव जो एक जन्म में अन्न होता है, दूसरे जन्म में स्थावर हो सकता है। चाहे न्नस हो या स्थावर, सब जीवों को दु:ख अप्रिय होता है। यह समझकर ही मुमुक्षु सब जीवों के प्रति अहिंसा भाव रखे। यही श्रेयस्कर है|
इस बात में कोई दो राय नहीं कि सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए निर्ग्रंथ प्राणिवध का वर्जन करते हैं। सभी प्राणियों को अपनी आयु प्रिय है| प्रायः सबको सुख अनुकूल है और दु:ख प्रतिकूल है। जो व्यक्ति हरी वनस्पति का छेदन करता है वह अपनी आत्मा को दंड देनेवाला है। वह दूसरे प्राणियों का हनन करके परमार्थत: अपनी आत्मा का ही हनन करता है।
इसलिए आत्मा की अशुद्ध परिणति मात्र हिंसा है; इसका समर्थन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है कि असत्य आदि सभी विकार आत्मपरिणति को बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए वे सब भी हिंसा हैं। असत्य आदि जो दोष बतलाए गए हैं, वे केवल “शिष्याबोधाय” हैं। संक्षेप में रागद्वेष का अप्रादुर्भाव अहिंसा और उनका प्रादुर्भाव हिंसा है। रागद्वेषरहित प्रवृत्ति से अशक्य कोटि का प्राणवध हो जाए तो भी नैश्चयिक हिंसा नहीं होती| रागद्वेषरहित प्रवृत्ति से, प्राणवध न होने पर भी, वह होती है। जो रागद्वेष की प्रवृत्ति करता है वह अपनी आत्मा का ही घात करता है, फिर चाहे दूसरे जीवों का घात करे या न करे। इस प्रकार हिंसा से विरत न होना भी हिंसा है और हिंसा में परिणत होना भी हिंसा है। इसलिए जहाँ रागद्वेष की प्रवृत्ति है वहाँ निरंतर प्राणवध होता है।
दरअसल हिंसा मात्र से पाप कर्म का बंधन होता है। इस दृष्टि से हिंसा का कोई प्रकार नहीं होता। किंतु हिंसा के कारण अनेक होते हैं, इसलिए कारण की दृष्टि से उसके प्रकार भी अनेक हो जाते हैं। यह ठीक है कि कोई जानबूझकर हिंसा करता है, तो कोई अनजान में भी हिंसा कर डालता है। कोई प्रयोजनवश हिंसा करता है तो कोई बिना प्रयोजन के भी हिंसा कर डालता है|
वैसे तो सूत्रकृतांग में हिंसा के पाँच समाधान बतलाए गए हैं : पहला- अर्थदंड, दूसरा- अनर्थदंड, तीसरा- हिंसादंड, चतुर्थ- अकस्माद्दंड, पांचवां- दृष्टिविपर्यासदंड। मसलन, अहिंसा आत्मा की पूर्ण विशुद्ध दशा है। वह एक ओर अखंड है, किंतु मोह के द्वारा वह ढकी रहती है। ऐसे में मोह का जितना ही नाश होता है, उतना ही उसका विकास होता है। इस मोह विलय के तारतम्य पर उसके दो रूप निश्चित किए गए हैं- पहला- अहिंसा महाव्रत, और दूसरा- अहिंसा अणुव्रत। इनमें स्वरूप भेद नहीं, मात्रा (परिमाण) का भेद है।
सच कहूँ तो मुनि की अहिंसा पूर्ण है जबकि इस दशा में किशी श्रावक की अहिंसा अपूर्ण क्योंकि मुनि की तरह ही श्रावक भी सब प्रकार की हिंसा से मुक्त नहीं रह सकता है। यही वजह है कि मुनि की अपेक्षा श्रावक की अहिंसा का परिमाण यानी मात्रा बहुत कम है। उदाहरणत: मुनि की अहिंसा 20 बिस्वा है तो श्रावक की अहिंसा सवा बिस्वा है। कहने का तात्पर्य यह कि पूर्ण अहिंसा के अंध बीस हैं, उनमें से श्रावक की अहिंसा का सवा अंश है। इसका कारण यह है कि श्रावक 19 जीवों की हिंसा को छोड़ सकता है, वादर स्थावर जीवों की हिंसा को नहीं। इससे उसकी अहिंसा का परिमाण आधा रह जाता है-यानी दस बिस्वा रह जाता है। इसमें भी श्रावक उन्नीस जीवों की हिंसा का संकल्पपूर्वक त्याग करता है, आरंभजा हिंसा का नहीं। अत: उसका परिमाण उसमें भी आधा अर्थात् पाँच बिस्वा रह जाता है।
संकल्पपूर्वक हिंसा भी उन्हीं उन्नीस जीवों की त्यागी जाती है जो निरपराध हैं। सापराध न्नस जीवों की हिंसा से श्रावक मुक्त नहीं हो सकता। इससे वह अहिंसा ढाई बिस्वा रह जाती है। निरपराध उन्नीस जीवों की भी निरपेक्ष हिंसा को श्रावक त्यागता है। सापेक्ष हिंसा तो उससे हो जाती है। इस प्रकार श्रावक यानी धर्मोपासक या व्रती गृहस्थ की अंहिसा का परिमाण सवा बिस्वा रह जाता है। इस प्राचीन गाथा में इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा है : “जीवा सुहुमाथूला, संकप्पा, आरम्भाभवे दुविहा। सावराह निरवराहा, सविक्खा चैव निरविक्खा।।“ अर्थात सूक्ष्म जीव हिंसा, स्थूल जीव हिंसा, संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, सापराध हिंसा, निरपराध हिंसा, सापेक्ष हिंसा और निरपेक्ष हिंसा। इस प्रकार से हिंसा के ये आठ प्रकार हैं जिनमे से कोई भी श्रावक सिर्फ चार प्रकार की हिंसा जो क्रमशः दूसरे, तीसरे, छठे और आठवें हिंसा का त्याग करता है। अत: श्रावक की अहिंसा अपूर्ण है।
यही वजह है कि पूरी दुनिया में अहिंसा को सर्वोच्च मानव धर्म करार दिया जाता है| जो लोग उपनिषद वाक्य “जीवो जीवस्य भोजनं” का तर्क देते हुए पाश्विक हिंसा की प्रवृति को मानव समुदाय के लिए अनुकरणीय बताते हैं, वह लोग अक्षम्य अपराध कर रहे हैं| वर्तमान संघर्षरत विश्व को अहिंसा भाव से ही बचाया जा सकता है| तभी तो अधिकांश धर्मों के मूल में अहिंसा भाव को अपनाने पर बल दिया गया है| दरअसल यह एक ऐसा सर्वहितकारी कर्म है जिसके अनुशीलन में ही मानव मात्र की भलाई निहित है| जब तक मनुष्य जीव हिंसा करता रहेगा, तब तक मानवीय समाज में शांति की कामना व्यर्थ है| यह राजा का पहला दायित्व है कि वह जीव हिंसा रोके| ऐसी ही प्रेरणादायक शिक्षा दे अन्यथा उसका राजपाट भी प्रकृति क्षणभंगुर बना देगी| ऐतिहासिक आख्यान इसी बात की तो चुगली करते हैं|
इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्मः का उपदेश जनमानस को दिया है जो काल की कसौटी पर पूरी तरह से सच है | व्यापक अर्थों में देखा जाए तो मानवीय अहिंसा के भाव से समस्त प्राणियों का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है क्योंकि जब हिंसक प्राणियों के मस्तिष्क को प्रेम, करुणा और सत्य के द्वारा हिंसक विचारों से हटाकर उसमें दया का भाव पैदा किया जाता है तो अहिंसा की भावना अंकुरित होती है| इस प्रकार अहिंसक व्यक्ति बदले की भावना अथवा हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने संघर्ष के उद्देश्य में सफल हो जाता है |
यह अटल सत्य है कि अहिंसा कायरता नहीं बल्कि जीवन में सहजता से ग्रहण किया गया तथा जीवनपर्यंत चलने वाला एक मानवीय सदव्यवहार है जो सत्य व ब्रह्म स्वरूप है| इससे पशुओं की पाश्विकता भी नियंत्रित की जा सकती है| वास्तव में अहिंसा आत्मिक उन्नति का साधन है| अहिंसा के लिए कभी भी शारीरिक बल की जरुरत नहीं होती है, बल्कि नेक विचार की दरकार होती है| अहिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है| वह अपने शत्रु का भी विनाश नहीं चाहता है| क्योंकि अहिंसा के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है|
इतिहास पुराणों व भारतीय महाकाव्यों के अनुशीलन से पता चलता है कि भले ही सबसे पहले ‘अहिंसा परमो धर्मः’ का प्रयोग हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के पावन ग्रंथ ‘महाभारत’ के अनुशासन पर्व में किया गया था। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाने में जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर का अहम योगदान है, क्योंकि भगवान महावीर की मूल शिक्षा ही ‘अहिंसा’ है। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भारत की आजादी की लड़ाई में सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया और आशातीत सफलता पाई|
आम तौर पर अहिंसा का सामान्य अर्थ है- ‘हिंसा न करना’। जबकि इसका व्यापक अर्थ है- किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुँचाना। अपने मन में किसी का अहित न सोचना और किसी अन्य को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान न पहुंचाना| दूसरे शब्दों में कहूँ तो कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी प्राणी कि हिंसा न करना ही अहिंसा है, जिसका जैन धर्म में बहुत महत्त्व है। जैन धर्म के मूलमंत्र में ही “अहिंसा परमो धर्म:” (अहिंसा सबसे बड़ा धर्म) कहा गया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिये जो आन्दोलन चलाया है, वह काफी सीमा तक अहिंसात्मक था।