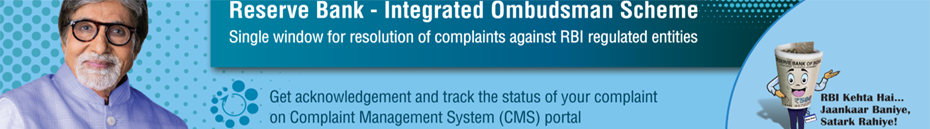यमुना भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रदूषण, अतिक्रमण और अविरल प्रवाह के अभाव में बदहाल हो चुकी है। दिल्ली में वजीराबाद वाटर वर्क्स से कालिंदी कुंज तक यमुना का लगभग 22 किलोमीटर क्षेत्र है जो गंभीर रूप से प्रदूषित है। इस प्रदूषण में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी घरेलू सीवेज की है। दिल्ली में सीवेज को शोधित करने हेतु केवल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनमें से 16 ही मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 712 मिलियन गैलन सीवेज उत्पन्न होता है जिसमें से केवल 607 मिलियन गैलन का ही शोधन हो रहा है और लगभग 184 मिलियन गैलन अशोधित सीवेज प्रतिदिन सीधे यमुना में गिर रहा है। आंकड़ों के अनुसार ही दिल्ली में औपचारिक रूप से 28 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें से केवल 17 कामन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान यानी सीईटीपी से जुड़े हैं। 11 क्षेत्रों में कोई ट्रीटमेंट प्लान ही नहीं है। जिन 17 क्षेत्रों में हैं उनमें भी क्षमता का केवल 31 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक अपशिष्ट भी लगातार यमुना में गिर रहे हैं।
ध्यातव्य है कि वर्ष 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था। भारत और जापान की सहभागिता से बनी इस योजना का उद्देश्य था- सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, कच्चे सीवेज को नदी में छोड़ने के लिए निगरानी और यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय करना आदि लेकिन यह विडंबना ही कही जा सकती है कि हजारों करोड़ रुपए का बजट लगने के बाद भी धरातल पर परिणाम लगभग शून्य है। विगत दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, बंगाल और पंजाब आदि प्रदेशों में सीवरेज संशोधन प्लांट की स्थिति को लेकर आंकड़ों के साथ यह सामने आया कि अधिकांश प्लांट क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं अथवा आवश्यकता से बहुत कम हैं. क्या यह स्थिति समूचे देश में नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में बताया गया कि नदियों के प्रदूषण पर अपेक्षा के अनुरूप अंकुश न लग पाने के लिए घरों में सीवेज कनेक्शन की कमी और परियोजनाओं को पूरा करने में हुई देरी जिम्मेदार है। विदित है कि सीवेज ढांचे को मजबूत करना, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना एवं साफ-सफाई आदि के लिए राज्य और स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं, फिर इसमें लापरवाही करने वाले निकायों अथवा राज्यों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाल ही में संसद की एक समिति ने जल परियोजनाओं में फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई है। समिति ने यह भी बताया कि दिल्ली के एक हिस्से में यमुना नदी की जीवन को बनाए रखने की क्षमता लगभग नगण्य पाई गई है।
राष्ट्रीय राजधानी में 33 निगरानी स्थलों में से 23 स्थल प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते। नदी में घुली ऑक्सीजन का स्तर दिल्ली के हिस्से में लगभग नगण्य पाया गया है. क्या यह गंभीर चिंता और चिंतन का विषय नहीं है? दिल्ली में समय-समय पर यमुना में अमोनिया बढ़ने से जल आपूर्ति बाधित होने के समाचार छपते हैं। जल संकट बढ़ने से जल माफिया सक्रिय हो जाते हैं और सामान्य व्यक्ति की आर्थिकी भी प्रभावित होती है। यह जहां एक और जीवन के लिए घातक है वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बड़ी आबादी के लिए जल आपूर्ति हेतु बड़ी चुनौती भी है, क्या इस पर गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए? इसी प्रकार एक समाचार से यह सामने आया कि वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में 58 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई जहां अब केवल दो ही सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य यमुना का पानी लाभार्थी राज्यों हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान के बीच बंटवारे के नियमन की जिम्मेदारी, न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एवं सतही एवं भू जल की गुणवत्ता की निगरानी है। प्रश्न यह है कि क्या इस रिवर बोर्ड का काम समाप्त हो गया अथवा बिना पर्याप्त सदस्यों के यह बोर्ड कैसे काम कर रहा है? वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक आदेश में यह कहा कि हरियाणा राज्य हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्यधारा में सीधे 10 क्यूसेक पानी छोड़े और वजीराबाद तक नदी का ई- प्रवाह बनाए रखे लेकिन विडंबना है कि विगत लंबे समय से वजीराबाद से आगे यमुना में उसके हिस्से का प्राकृतिक जल आ ही नहीं रहा है। यही स्थिति दिल्ली के कालिंदी कुंज से आगे भी है।
हाल ही में वजीराबाद, कश्मीरी गेट, आईटीओ, सराय काले खां और कालिंदी कुंज जाकर यमुना की स्थिति से यह स्पष्ट हुआ कि उसमें कहीं भी प्रवाह नहीं है। सर्वत्र प्रदूषण, कचरा और दुर्गंध फैली हुई है। क्या इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, यमुना रिवर बोर्ड और उससे संबंधित अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? यमुना की बदहाली के मूल में ढांचागत योजनाओं के क्रियान्वयन की कमी, नगर और स्थानीय स्तर के अधिकारियों की उदासीनता और सरकारों का लचर रवैया रहा है। कहीं केंद्र और राज्य के झगड़े तो कहीं राज्य और स्थानीय निकायों में समन्वय की कमी साफ दिखाई देती है। दिल्ली जैसे महानगर में नगरीय आबादी के अतिरिक्त एक बड़ी आबादी अनधिकृत क्षेत्र में भी रहती है। जहां न सीवेज सिस्टम है और न ही नियम- कानून। इसके अतिरिक्त दिल्ली के करोल बाग,इंदरलोक एवं शाहदरा जैसे अनेक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की अवैध फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं जिनसे रंग-रसायन एवं विषैले अपशिष्ट सीधे नालों के जरिए यमुना में आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व कामन एफ्लूएंट प्लान की कमी, उनका काम न करना, प्रदूषण की स्थिति व अतिक्रमण आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी की जवाबदेही नहीं है। कोई भी यमुना के बहाव क्षेत्र में कूड़ा कचरा व पूजा सामग्री डाल देता है। न कोई निगरानी है और न ही डालने वाले को दंडित करने के प्रावधान दिखाई देते हैं।
विगत दिनों दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने अपने नाकामी की पोल खोलता नदियों का प्रदूषण शीर्षक लेख में लिखा है कि नदियों के प्रदूषण में नौकरशाही की भूमिका पर कभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। अच्छा हो कि सरकार इस पर कोई श्वेत पत्र लाए कि नदियां क्यों प्रदूषित हैं? दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद यमुना की बदहाली को लेकर कुछ चिंता एवं चर्चा शुरू हुई है। इससे आशा ही की जा सकती है कि कुछ सुधार होगा। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नालों से प्रदूषण की हिस्सेदारी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह सामने आया है कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (59.93. प्रतिशत बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) नजफगढ़ नाले की है… इसके बाद सबसे ज्यादा 27.48 प्रतिशत प्रदूषण शाहदरा ड्रेन से जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब पर्यावरण विभाग आगे की कार्ययोजना पर काम कर रहा है।
दिल्ली अथवा किसी भी महानगर में नाले बरसाती पानी की निकासी के लिए होते हैं। आबादी का सीवेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर और औद्योगिक क्षेत्र का अपशिष्ट कॉमन एफ्लूएंट प्लान से पूरी तरह शोधित होकर ही किसी नदी में जाना चाहिए किंतु यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजधानी में शासन-प्रशासन की मिलीभगत और नियमों की अनदेखी से छोटे-बड़े सभी नालों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट बह रहा है। यमुना की बदहाली को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर योजनाएं बनें, उनका क्रियान्वयन हो एवं वे सतत चलें। साथ ही समय समय पर उनकी समीक्षा की जाए। हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में समुचित समन्वय हो। औद्योगिक क्षेत्र से भी समन्वय एवं निगरानी के प्रयास किए जाएं। नगरीय एवं अनधिकृत आबादी क्षेत्र में पर्याप्त सीवेज संशोधन प्लांट लगाए जाएं और उनकी निगरानी हो। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वे बड़े नाले जो सीधे यमुना में गिरते हैं उन पर जगह-जगह प्री फिल्टर व राक फिल्टर जैसी तकनीक से प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास किए जाएं।
स्थानीय जल स्रोतों को वर्षा एवं बाढ़ के समय भरने के लिए यमुना बहाव क्षेत्र में भू जल पुनर्भरण प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र व्यवस्था बनाई जाए। नालों के पानी को स्थान स्थान पर जलाशयों में रोकते हुए नदी की ओर जाने दिया जाए। यमुना की सफाई में जन भागीदारी एवं जागरूकता हेतु समय-समय पर सामाजिक- सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संत समाज, फिल्म जगत के एवं अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट लोग भी इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान दें। ध्यान रहे केवल चर्चा,नारों और कागजी योजनाओं से अब काम चलने वाला नहीं है। यमुना के लिए व्यापक एवं सतत कार्य योजना तत्काल लागू करनी होगी। यमुना केवल एक नदी नहीं है, यह जीवनदायिनी है। इससे प्रकृति-पर्यावरण, संस्कृति, कृषि एवं आर्थिकी भी जुड़ी है। अत: इसके पुनरुद्धार हेतु विकल्पहीन प्रतिबद्धता आवश्यक है।