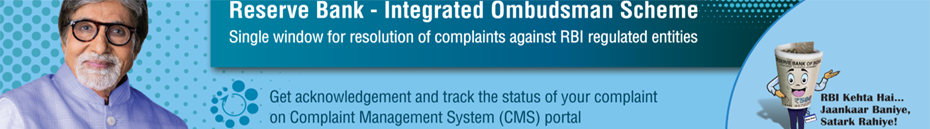हाल ही में यूनिसेफ ने ‘लर्निंग इंटरप्टेड: ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट-रेलेटेड स्कूल डिसरप्शन्स इन 2024’ रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो बताती है कि मौसम का शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में यह शिक्षा के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट बताती है कि मौसम के कारण भारत के 5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं,यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल यानी कि वर्ष 2024 में भारत ने गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारतीय मौसम विभाग ने बताया था कि यह साल 1901 के बाद से सबसे गर्म साल(2024) के तौर पर दर्ज किया गया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पिछले साल गंभीर जलवायु संकट की मार झेल रही थी। हाल फिलहाल, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है, जिसमें स्कूली बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे जलवायु संकट के खतरनाक असर को उजागर किया गया है।
दरअसल, रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है और वर्ष 2024 में दुनिया भर के स्कूल जाने वाले हर सात बच्चों में से एक बच्चा मौसमी बाधाओं(बदलती जलवायु) के कारण स्कूल में उपस्थित नहीं हो सका। शोध के अनुसार साल में गर्म दिनों की अधिक संख्या ने परीक्षा के नतीजों को भी खास तौर पर प्रभावित किया।रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दक्षिण एशिया विशेषकर भारत, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में अप्रैल महीने में हीटवेव(लू) ने शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। यह बहुत संवेदनशील है कि यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (सीसीआरआई) में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है। चिन्ता इस बात की है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश बताया गया है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में 18 देशों में जलवायु संकट के चलते स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।इस रिपोर्ट के मुताबिक, 242 मिलियन (24.2 करोड़) छात्रों की पढ़ाई जलवायु संकट की वजह से प्रभावित हुई, जिनमें 74% छात्र निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों से थे। उल्लेखनीय है कि ये बच्चे प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक के हैं।बताया गया है कि दक्षिण एशिया इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 128 मिलियन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई। वहीं अफ्रीका में 107 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, और 20 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ने की कगार पर हैं।
शिक्षा पर ही किसी देश का भविष्य निर्भर करता है। हीटवेव(लू), बाढ़, तूफान, चक्रवात और सूखे जैसी घटनाओं का असर बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है और यदि इस संकट से निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर भविष्य में भी अनेक पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यूनिसेफ ने सरकारों से यह अपील की है कि वे शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस व प्रभावी रणनीतियां बनाएं। कहना ग़लत नहीं होगा कि जलवायु या यूं कहें कि मौसमी बाधाओं का असर बच्चों की शिक्षा पर लंबे समय तक रहता है।यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा, तो वर्ष 2050 तक बच्चों के गरम हवाओं के संपर्क में आने की संभावना आठ गुनी बढ़ जाएगी। वास्तव में,इस संबंध में स्कूलों को जलवायु (मौसमी घटनाओं) के प्रति अधिक सहनशील बनाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज संपूर्ण विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अपने परवान पर है, विशेषकर विकासशील और विकसित देशों में। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इन गैसों के उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में यथेष्ट प्रयास किए जाएं। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता है।
स्कूली बच्चे जलवायु परिवर्तन जैसे कि बाढ़, सूखे और हीटवेव जैसे शारीरिक खतरों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और ये परिवर्तन उनकी शारीरिक क्षमताओं, संज्ञानात्मक क्षमताओं, भावनात्मक कल्याण तथा शैक्षिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में जकार्ता में आई बाढ़ के कारण स्कूलों तक पहुँच बाधित हुई। वहीं पर वर्ष 2019 में चक्रवात ईदाई ने मोज़ाम्बिक में 3,400 कक्षाएँ नष्ट कर दीं। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गीता ने टोंगा में 72% स्कूलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वास्तव में शिक्षा पर जलवायु प्रभावों को कम करने के लिये कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मसलन, आज स्कूली अवसंरचना को जहां मजबूत बनाने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सहायता के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। जागरूकता तो जरूरी है ही।
इतना ही नहीं,शिक्षा में निरंतरता बनी रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिये जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति बच्चों की आघातसहनीयता बढ़ाने हेतु शैक्षिक प्रणालियों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हर देश की अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना या एक्शन प्लान होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश(सौर ऊर्जा), पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पनबिजली, महासागरीय ऊर्जा, बायो एनर्जी आदि प्रचुर मात्रा में हैं और हमारे चारों ओर मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। वास्तव में, यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात् इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीनहाउस उत्सर्जन होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, ऐसे में यह स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को भी बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन – कोयला, तेल और गैस – गैर-नवीकरणीय संसाधन हैं जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। जीवाश्म ईंधन, जब ऊर्जा उत्पादन के लिए जलाए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।परिवहन उत्सर्जन में कटौती के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वृक्षारोपण की पहल काफी योगदान दे सकती है।