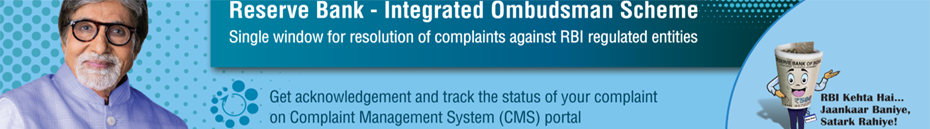युगों युगों से विश्व के विद्वानों, चिंतकों और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। हर एक देश की शिक्षा व्यवस्था उसके देशकाल, समाज, व्यवस्था और वातावरण के अनुसार रही है। कुछ विचार उस समय भी महत्वपूर्ण रहे और आगे आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। वहीं कुछ विचार समय की गति के अनुसार लुप्त होते गए। वर्तमान पीढ़ी अपने से पूर्व सही और समाजापयोगी शिक्षा के उद्देश्यों को आधार बनाकर लिख-पढ़ रही है, साथी ही समयानुसार उसमें परिवर्तन भी कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो समयानुसार शिक्षा के उद्देश्य और उसके तौर तरीकों में बदलाव देखे गए हैं और यह बदलाव भविष्य में भी होते रहेंगे।
शिक्षा निरन्तर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात जीवनपर्यन्त चलती रहती है। मानव अपने अनुभवों, भौतिक, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिस्थितियों तथा विश्व की विभिन्न घटनाओं से सदा कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षाविदों के अनुसार भी और सामाजिक जीवन के अनुसार भी जन्म लेने के साथ ही बालक में सीखने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तो बालक मां के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। महाभारत महाकाव्य में अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीखने की प्रक्रिया ही बालक को शिक्षित कर उसे शिक्षा प्रदान करके परिपूर्ण मानव बनाती है। शिक्षाविदों और विचारकों ने बालक की मानसिक वृद्धि तथा विकास की अवस्थाओं के अनुरूप औपचारिक शिक्षा को कई भागों में बाँटा है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि आयु पर आधारित शिक्षा का विभाजन तव ही उपयुक्त हो सकता है जब बालक अथवा व्यक्ति अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में अध्ययन कर रहा हो।
भारतीय समाज में शिक्षा को सदा ही अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरुकुल शिक्षा से लेकर आज तक हमने शिक्षा को विशेष स्थान दिया है। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने हमेशा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह अलग अलग तरीके से लगाएं हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भी राष्ट्र के शीर्ष स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा के समुचित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र की नवीन आवश्यकताओं तथा जनसाधारण की आकांक्षाओं के अनुरूप देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने की दिशा में समय-समय पर अनेक सार्थक प्रयास किये गये हैं। इसके साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती रही और जन सामान्य के साथ जुड़ती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में राष्ट्र के सभी नागरिकों को विना किसी भेदभाव के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा गया है कि – “भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है।”
बदलते दौर में अब शिक्षा विश्व व्यापक हो गई है। हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और वह देश दुनिया से हर एक स्तिथि में जुड़ना चाहता है। वैश्विक शिक्षा के इस दौर में अब भाषाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। सभी देश एक दूसरे देश की भाषाओं को जानना-समझना चाह रहे हैं। वैश्विक व्यापार की संरचना में भी भाषाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्वीकरण में भाषा अहम भूमिका अदा कर रही है। ऐसे में हर एक शिक्षण संस्थान वैश्विक और अपनी देशी भाषाओं को पढ़ना-पढ़ाना चाह रहे हैं। जिससे कि बच्चे भाषायी दौर में पीछे नहीं रहें। कंप्यूटर को एक विषय के साथ-साथ भाषा विषय भी मानकर पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। सही मायनों में कर्तव्यनिष्ठ एवं अधिकार-सचेत नागरिक ही देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।