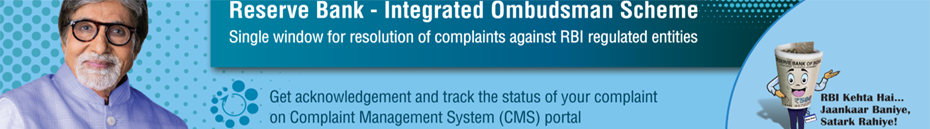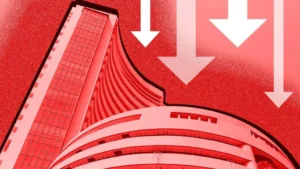प्रेमचंद केवल हिन्दी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का वह नाम है जो मानवीय संवेदना, अद्ïभुत मेधा, विश्व-बंधुत्व, समाज व राष्ट्र की समस्याओं के प्रति सचेत-आहत और प्रामाणिक रूप से कलापूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे। मात्र कुछ ही शब्दों में प्रेमचंद के विराट व्यक्तित्व और विपुल कृतित्व को समझा अथवा समझाया नहीं जा सकता। एक साधारण डाक मुंशी के घर में 31 जुलाई, 1880 को जन्मा यह बालक अपने चुनौतीपूर्ण जीवन व परिस्थितियों से तराशा गया, हिन्दी साहित्य का पुरोधा लेखक बना, महान किस्सागोई कला से युक्त सर्जक, एक व्यापक विश्वदृष्टि से भरपूर, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रवर्तक कथा सम्राट.. प्रेमचंद उनका लेखकीय नाम था जो ‘सोजेवतन’ के दमनचक्र के बाद रख लिया था। यों उनका असल नाम धनपत था, घरवाले प्यार से नवाब भी पुकारते थे।
प्रेमचंद ने न केवल साहित्य, समाज व संस्कृति से जुड़े हर मसले पर बेबाकी से हस्तक्षेप किया बल्कि समयुगीन सामाजिक, आर्थिक, साम्प्रदायिक और राजनैतिक विसंगतियों व विडम्बनाओं पर भी जमकर प्रहार किया। उन्हें अपनी जीवनसंगिनी शिवरानी देवी की भांति जेल न जा पाने का मलाल हमेशा सालता रहा, मगर उन्होंने यथाशक्ति राष्ट्रीय क्रांति में हिस्सेदारी की। गांधी के असहयोग आंदोलन के आव्हान पर एक झटके में जीवन-यापन के एकमात्र सहारे को ठोकर मार दिया। 16 फरवरी, 1921 को 21 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इससे भी कहीं पहले ‘सोजेवतन’ की प्रतियां ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909-10 में जब्त कर जला दिया जाना उनके प्रखर राष्ट्रीय बोध एवं स्वदेश प्रेमभावना का परिचायक है।
प्रेमचंद ने गांधीवादी विचारधारा को मनोकूल पाया और अपने साहित्य में उसे पोषित किया हालांकि बाद में कम्युनिज्म की तरफ उनका झुकाव हो गया था। पहले वे टॉलस्टॉय के प्रभाव में थे, फिर 1914 से 1918 के बीच गांधी से प्रभावित रहे। वे 21 दिसम्बर, 1919 को मित्र मुंशी दयाराम निगम जी को लिखे खत में अपने साम्यवाद के प्रति झुकाव को स्वीकार करते हैं, मैं करीब-करीब बोलशेंविस्ट उसूलों का कायल हो चुका हूं। 1936 तक तो वे गांधीवाद से भी मुक्त हो चुके थे।
प्रेमचंद ने गांधी द्वारा आव्हानित सभी आंदोलनों, सत्याग्रहों को कहानी-उपन्यासों में स्थान दिया। एक प्रकार से वे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी कलम लेकर उतर पड़े थे। ‘होली’ शीर्षक कहानी उनके इसी तीव्र राष्ट्रीय बोध से ओत-प्रोत रचना है, जिसमें विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को आंदोलन मूर्त हुआ है। इसी तरह उपन्यास ‘गबन’ में पात्र देवीदीन खटीक का संवाद, ‘कर्मभूमि’ में नायिका नैना द्वारा जुलूस का नेतृत्व और गोली खाकर शहीद होना, ‘रंगभूमि’ में सोफिया, सूरदास आदि पात्रों के माध्यम से उपनिवेशी सत्ता की खिलाफत आदि कई उदाहरण हैं वहीं पे्रमचंद ने कलम के जोर से अपने साहित्य में भी स्वाधीनता के संघर्ष को बल दिया।
प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को पूर्ववती रुमानी और तिलिस्म प्रधान लेखन से मुक्त कर उसे प्रौढ़, प्रगल्भ किया। उसे मानव मात्र से जोड़ा और समाज सापेक्ष किया। उन्होंने साहित्य में यह युगांतरकारी परिवर्तन किया कि पहली बार आम आदमी की वास्तविक जिंदगी को कथा में हू-ब-हू उतारना शुरू किया। हालांकि वे स्वप्नदृष्टा साहित्यकार तो थे ही, निजी जीवन में भी महत्वाकांक्षी थे, जिसका प्रमाण प्रेस लगाना..’जागरण’ (साप्ताहिक), ‘हंस’ जैसी पत्र-पत्रिकाओं को तमाम आर्थिक जंजालों के बावजूद चलाए रखना है। इसी स्वप्नदृष्टा प्रवृत्ति के कारण उन्होंने बेहतर मनुष्य और मनुष्य जीवन की कल्पना की। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के आदर्श को अपने लेखन में प्रतिष्ठित किया। एक ऐसी दुनिया का सपना देखा और दिखाने की चेष्टा की, जहां मानव श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों व गरिमा, समता की भावना के साथ सामाजिक रूप से उत्तरोत्तर प्रगति करे। इसीलिए उन्होंने अपने लेखन में आदर्श को महत्ता दी और उनका कमोवेश सारा आरंभिक लेखन आदर्शवादी दृष्टि से रचा-पचा है। किंतु आगे चलकर उन्हें यह भान हो गया कि आदर्श को चित्रित करते हुए भी उसे अभी पाया नहीं जा सकता, इसीलिए तो ‘गोदान’ से उन्होंने घोर यथार्थवाद को मान्यता दी। मृत्युशैया पर जैनेन्द्र से भी उन्होंने कहा था-‘अब आदर्श से काम नहीं चलेगा।‘ दरअसल उनका विरोध यथार्थवाद से नहीं था, वे उसके प्रकृतिवाद (नेचुरलिज्म) बोध, हालांकि ये उनका भ्रम था, के खिलाफ थे।
प्रेमचंद निडर होकर न सिर्फ लिखते रहे बल्कि उतनी ही निडरता से उन्होंने अपने द्वारा स्थापित आदर्शों को स्वयं मूर्त करने का प्रयास भी किया। समकालीन समाज में विधवा विवाह वर्जित था तो उन्होंने बालविधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। यह ठीक वही वक्त था जब वे ‘हमखुर्मा ओ हमसवाब’ का हिन्दी रूपांतर ‘प्रेमा’ लिख रहे थे। इस उपन्यास का नायक भी विधवा से शादी करता है। क्या यह मात्र संयोग था? और अगर था भी तो यह मानने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि महान व्यक्ति ही ऐसे संयोगों को धरातल पर घटित कर सकते हंै। लेकिन प्रेमचंद तो अपने जीवन को सामान्य आदमी का अतिसाधारण जीवन कहते हैं!…’मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गड्ढे तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खण्डहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी।‘ (अमृतराव- ‘कलम का सिपाही’ की भूमिका)
प्रेमचंद में आज के तथाकथित बड़े साहित्यकारों की भांति आत्मअहं लेश मात्र भी नहीं था। कितनी विनम्रता से इस युगांतरवादी लेखक ने अपने समग्र जीवन और साहित्य को इस रूपक में बांध दिया है, ‘एक सीधा-सादा, गृहस्थी के पचड़ों में फंसा हुआ तंगदस्त मुदर्रिस, जो सारी जिंदगी कलम घिसता रहा…मैं तो नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल हूं। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज पैदा हो जाती है, बस इतनी-सी बात है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है, उन हवाओं का है जो मेरे भीतर बजी।‘ अमृतराव के अनुसार-‘जो हवाएं उनके भीतर बजी,वहीं उनका साहित्य है, हमारे आपके दु:ख-सुख का साहित्य।‘
प्रेमचंद ने अपने सृजनात्मक साहित्य के साथ ही विचारात्मक गद्य में भी मनुष्य की जातीय संकीर्णता खासकर हिंदुओं की अतिवादी धर्मांधता व आडम्बरों पर तीखा विरोध दर्ज किया। ब्राह्मïणवाद की कुटिलताओं पर उनके शब्द थे ‘इन पुजारियों और पंडों को मैं हिंदू जाति का अभिशाप समझता हूं, यही हमारे पतन का कारण हैं।‘ प्रेमचंद ने समकालीन समाज की प्रत्येक विकृति व रूढि़ पर डटकर लिखा, उनकी पैनी लेखनी की नोंक के नीचे से समयुगीन समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं जो न गुजरा हो…पूरी निर्भीकता और बेलाग अंदाज में उन्होंने एक जागरूक सर्जक के रूप में युगांतरवादी भूमिका निभाई। प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर लिखा-‘साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति को दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप से निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए वह…संस्कृति का खोल चढ़ाकर आती है।…अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति, अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति,…संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं।‘ ‘जागरण,15 जनवरी, 1914 अंक’
पंूजीवाद पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा-‘संपत्ति ने मनुष्य को क्रीतदास बना दिया है।…हम संपत्ति के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं।…जब तक संपत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, तब तक संपत्ति-व्यक्तिवाद का अंत न होगा संसार को शांति नहीं मिलेगी।‘
उनका कहना था कि- ‘जब तक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता।‘ (राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता)।
‘प्रेम की वेदी’ में नायिका जेनी के जरिये वे वास्तविक धर्म के स्वरूप में प्रेम को मान्य करते हंै, ‘खुदा का धर्म प्रेम है और मैं इसी धर्म को स्वीकार करती हूं। शेष धोखा है।‘ उनकी संवेदना प्रत्येक वर्ग और उसके निम्नतर व्यक्ति के जीवन से सीधे संपन्न-संबद्ध थी। यह किसी हद तक कहा जा सकता है कि स्त्री समानाधिकार और स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए भी कहीं-कहीं शायद वे उसकी सीमाओं को लेकर संशयग्रस्त थे और परिवार के अंदर ही उसकी विविध भूमिकाओं को प्रतिष्ठित करने के पक्षधर थे। हो सकता है, इसके पीछे उनके अपने संस्कार रहे हों। उनकी नारी दृष्टि पूर्णत: यथार्थवादी तो नहीं, वहां वे भावुकता और आदर्शवाद का सहारा लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ‘जालपा, धनिया, सिलिया, सोफिया, नैना और निर्मला आदि नारी पात्रों द्वारा उन्होंने स्त्री मुक्ति और उसके स्वावलंबन के महत्वाकांक्षी विद्रोहिणी चरित्र को वे सामने लाए। ‘नैराश्य’, ‘शूद्रा’, ‘आभूषण’, ‘देवी’, ‘सौत’, ‘निर्वासन’ आदि कई कहानियों में नारी के समर्थ चरित्र को उभारा गया है। ये कहानियां इस बात का प्रमाण है कि पे्रमचंद स्त्री को बराबरी के मसले को अहमियत देते हैं। ‘निर्वासन’, (‘चांद’ पत्रिका, जून 1924 अंक) सशक्त रचना है, जहां पति मेले में बिछुड़ी अपनी पत्नी को त्याग देता है, यह लांछन लगाकर कि वह उसके किसी ‘काम’ की नहीं रह गई है। स्त्री में यहां अपने अधिकारों को लेकर बेचैनी दिखाई देती है।
गौरतलब है कि गांधीजी और प्रेमचंद का क्रमश: भारतीय राजनीति व साहित्य की भूमि पर अवतरित होने का समय एक ही है। प्रेमचंद ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के काल में लेखनकर्म शुरू किया। जो कार्य स्वाधीनता संघर्ष के अगुवा बनकर गांधी जी कर रहे थे, वही काम अपनी कलम के जरिए साहित्य में प्रेमचंद करते रहे। गांधीवाद के प्रभाव में उन्होंने आरंभ में आदर्शवादी-सुधारवादी रचनाएं लिखीं जैसे सौत, पंचपरमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, जुलूस, ईदगाह, अलग्योझा आदि।
बाद में उन्हीं की कलम ने समसामयिक जीवन की क्रूर सच्चाइयों को पेश करना शुरू किया और वह यथार्थ न केवल तब का मौलिक यथार्थ था, वरन् वह आज भी हमारे देश के अधिकांश गांवों की वास्तविकता है। जो उन्होंने लिखा, वह सबकुछ तो भारतीय ग्रामों का सर्वकालिक इतिहास है। उनकी ‘सवासेर गेहूं’, ‘पूस की रात’, ‘कफन’, ‘सद्ïगति’ , ‘मुक्तिमार्ग’, ‘ठाकुर का कुआं’ जैसी कई कहानियां… समाज में तब व्याप्त रूढिय़ों, महाजनी परंपरा, ब्राह्मणपंथी शोषण, दलित-दमन आदि सभी ज्वलंत समस्याओं को रेखांकित करती हैं।
प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य को परम्परागत, प्रमुखतया सामंती सोच वाली लेखकीयधारा व दृष्टि को तोड़कर एक नई मानवतापूर्ण दृष्टि और विचार को प्रश्रय दिया। सर्वहारा व आम आदमी के अति साधारण जीवन को पहली बार केन्द्र में लाए, सृजन का सरोकार समाज और दीन-हीन नागरिकों को बनाया और न केवल कथ्य बल्कि शिल्प के तौर पर भी उन्होंने यथार्थ को रचा-गढ़ा। प्रेमचंद कहते थे कि ‘मंै उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र मानता हूं।‘ वे साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य राजनीति का अनुगामी नहीं वरन्ï उसके आगे मशाल लेकर चलता है। प्रेमचंद ने साहित्य के उद्ïदेश्य को लेकर साफ कहा था कि-‘साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं।…साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाभिक और स्वाधीन बनाता है, दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्ïदेश्य है।‘ (साहित्य का उद्ïदेश्य कुछ विचार) उन्होंने बताया कि, ‘(साहित्यकार), जो दलित है, पीडि़त है, वंचित है… चाहे वह व्यक्ति हो या समूह…उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है।‘ (प्रेमचंद कुछ विचार)-
उनका पहला हिंदी उपन्यास ‘सेवासदन’ था जो कि 1918 में आता है, यहीं से हिंदी साहित्य का भी नया युग शुरू होता है, जिसे ‘विकास युग’ की संज्ञा दी गई। प्रकाशचन्द्र गुप्त ने प्रेमचंद के महत्व को इन शब्दों में रेखांकित किया है, ‘हिंदी उपन्यास का इतिहास लगभग प्रेमचंद की कला का इतिहास है।‘ आलोचक रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के प्रदेय को इस प्रकार बताया है, ‘उन्होंने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाया है, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरव दिया है।…जिन विशेषताओं को उन्होंने अपने कथा साहित्य में झलकाया है, वे हमारी जनता की जातीय विशेषताएं थी।‘ (प्रेमचंद और उनका युग,)।
पे्रमचंद से बढ़कर भारतीय जनचेतना, बल्कि और स्पष्ट कहें तो ग्रामीण चेतना व जनपक्षधरता से परिपूर्ण कोई दूसरा लेखक नहीं मिलता। उन्होंने अपने समकालीन और आगे की पीढ़ी के लेखकों को इसी लोकचेतना व लोकधर्मिता से जुडऩे की प्रेरणा दी।
8 अक्टूबर, 1936 को पैतृक गांव लमही में ही इस युगांतरकारी लेखक का देहावसान हुआ। ‘मंगलसूत्र’ (अपूर्ण) उनकी मृत्यु के बाद 1948 में प्रकाशित हुआ। अमृतराय ने सटीक कहा है कि ‘उनका जीवन कलाकार का नहीं, किसान का था, जिसके हाथ में कुदाल की जगह कलम थी।‘