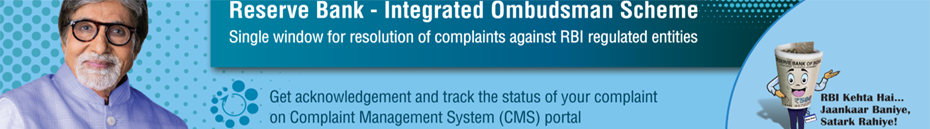भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के अभ्युदय काल को नवयुग कहा जा सकता है। जिस समय बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ उस समय धर्मों के आडंबर एवं हिंसा का समावेश हो चुका था। यज्ञों में धर्म के नाम पर पशुबलि दी जाती थी। साथ ही समाज में कई तरह की कुरीतियों ने जन्म ले रखा था। ऐसे में स्वाभाविक था लोगों का एक नए धर्म के प्रति आकर्षित होना, क्योंकि इस धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने सामान्य जनमानस को यह बताने की कोशिश की कि हिंसा का रास्ता छोड़ो, बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। बुद्धम् शरण शरणम् गच्छामि, धम्म शरणम् गच्छामि सघम् शरणम् गच्छामि। जीवन पानी के बुलबुले के समान है। हिंसा देवी-देवताओं को खुश करने के लिए हो या राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए छेड़ा गया युद्ध हो, इससे राजा सम्राट तो बन सकता है, जमीन के टुकड़े पर शासन कर सकता है, लेकिन वहां के लोगों के दिलों पर नहीं। हिंसा, हिंसा होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कुछ ऐसा ही था कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ से भिक्षु बने गौतम बुद्ध का उपदेश। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े, लगभग 2500 साल पहले के इतिहास को कागज के टुकड़े पर समेटना आसान नहीं होगा, फिर भी एक कोशिश तो की जा सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह बच्चे द्वारा परछाई को पकडऩे की….। वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) के आते ही तथागत के जीवन से जुड़ीं उन तीन घटनाओं (जन्म, ज्ञान और निर्वाण) और उनसे जुड़े उन स्थलों की स्मृति ताजी हो उठती है, जो साक्षी रहे हैं, उन लम्हों के। जी हां! हम बात कर रहे हैं, कुशीनगर की, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के उन अंतिम क्षणों से रहा है, जब उन्होंने अपना आखिरी उपदेश यहां पर दिया था। अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर प्रसिद्ध यह बौद्ध स्थल पूर्वी उ.प्र. के जिला मुख्यालय गोरखपुर से 51 किमी. की दूरी पर स्थित है। इसके चारों तरफ फैली प्राकृतिक हरियाली, परिंदों का कलरव। कितना अच्छा लगता है, वर्तमान के चौखट पर खड़े हो अतीत की तरफ झांकते हुए। वक्त की चादर के नीचे सिमटे इस प्राचीन भारत की गौरवमयी धरोहर की पहचान सर्वप्रथम प्रसिद्ध अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता अलेग्जेंडर कनिघम ने सन्ï 1861-62 ई. में की थी। कालांतर में इस स्थल पर पड़े समय की चादर को समेटा सन्ï 1877-80 ई. में एस.सी. कलाईकल ने। सन्ï 1904-07 में जेपी एच फोगल एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में पं. हीराचंद शास्त्री ने। इन विद्वानों का अथक परिश्रम रंग लाया और धरती के नीचे दबा सदियों पूर्व का इतिहास परत-दर-परत खुलता चला गया, जो आज समूची दुनिया के सामने भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में रेखांकित है।
भारतीय इतिहास में मल्लराजाओं की राजधानी रही कुशीनगर के नामकरण के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। डॉ. राजबली पाण्डेय की पुस्तक गोरखपुर जनपद के क्षत्रिय जातियों का इतिहास के अनुसार इस स्थल को भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है। वक्त के हाथों जमींदोज हुआ कुशीनगर अपने वैभव काल में कई राजवंशों की राजनैतिक गतिविधियों को अपने आंचल में समेटे हुए भगवान बुद्ध के निर्वाण का साक्षी भी रहा है।
कुशीनगर की पुरातात्विक खुदाई के समय जो महत्वपूर्ण स्थल प्रकाश में आए उनमें से अति महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध की निर्वाण मुद्रा में मिली लगभग 6.10 सेमी लंबी प्रतिमा। जिस मंदिर के अवशेष में यह प्रतिमा मिली थी, उसकी लंबाई 47 फीट 6 इंच और चौड़ाई 32 फीट थी तथा इसकी दीवारें 10 फीट मोटी थीं। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक गर्भगृह मिला था, जिसका परिमाप 35 फीट 7 इंच तथा बीच का भाग 15 फीट था। वर्तमान मंदिर का निर्माण भी इसी मंदिर की नींव पर किया गया है। जमीन से लगभग 2.74 मीटर उंचे चबूतरे पर स्थित यह मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के केंद्र में स्थित है भगवान बुद्ध की लेटी हुई विशालकाय प्रतिमा जो अब तक की मिलीं प्रतिमाओं में शायद एकमात्र ऐसी बुद्ध प्रतिमा है। यहां से प्राप्त एक अभिलेख से प्राप्त होता है कि इस प्रतिमा का निर्माण हरिबल स्वामी नामक बौद्ध भिक्षु ने पांचवीं शताब्दी में कराया था। इस स्थल के गौरव का बखान चीनी यात्री हृबेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में किया है।
कुशीनगर की खुदाई के फलस्वरूप यहां से राजभवनों के अवशेष, दस बौद्ध विहार, कुछ स्तूप मंदिरों एवं बौद्घ मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। जो इस स्थल के वैभव की दास्तान सुनाते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर के ठीक पीछे उचक-उचककर झांकता-सा प्रतीत होता, अपने अतीत के गौरव पर इतराता छत्र युक्त दिखाई देता बेलनाकार यह स्तूप यहां का मुख्य स्तूप है। बताया जाता है कि इसी स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ई. पूर्व 483 में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कुशीनगर के मल्लराजाओं ने चिता भस्म को रखकर इस स्तूप का निर्माण कराया था। चीनी यात्री हृबेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस स्तूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह स्तूप 200 फीट ऊंचा था तथा इसकी निर्माण शैली अत्यंत उच्च कोटि की थी। इसी के आसपास बौद्ध मंदिर एवं विहार थे। मुख्य स्तूप के पीछे पूरब की दिशा में मन्नत स्तूपों के खंडहरों के बीच लगभग 15 फीट ऊंचा एक चबूतरानुमा स्तूप दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्ति के बाद तथागत के शिथिल शरीर को दो शाल्व वृक्षों के नीचे छह दिनों तक लोगों के दर्शनार्थ रखा गया था और यहीं से उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर के उत्तरी द्वार से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी शवयात्रा निकाली गई थी, जिसमें राजपरिवार और बौद्ध भिक्षुओं सहित साधारण लोगों ने भी भाग लिया। महापरिनिर्वाण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है माथाकुंवर मंदिर। मंदिर के ठीक सामने बौद्ध विहारों के ध्वंसावशेष दृष्टिïगोचर होते हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि कुशीनगर आगमन से पूर्व भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर विश्राम करते हुए अपना अंतिम उपदेश दिया था। माथाकुंवर मंदिर में तथागत की काले रंग की एक प्रतिमा भू-स्पर्श की मुद्रा में स्थापित है। सन्ï 1876 ई. में कलाईकल द्वारा माथाकुंवर टीले की खुदाई के दौरान काले पत्थर पर 23 पंक्तियों का खुदा हुआ एक शिल्प लेख प्राप्त हुआ था, जिससे पता चलता है कि कलचुरी शासकों ने इस प्रतिमा का निर्माण कराया था।
माथाकुंवर से लगभग 150 किमी. की दूरी पर स्थित है रामभार स्तूप। दूर से किसी पर्वत-सा दिखने वाले ईंटों से निर्मित इस स्तूप के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर को जलाया गया था। इस स्तूप की खुदाई पं. हीरानंद शास्त्री के दिशा-निर्देशन में 1910 में की गई थी। सन्ï 1861 में जब कनिंघम ने इस विशालकाय स्तूप का सर्वेक्षण किया था, तब इसकी ऊंचाई 49 फीट थी। चीनी यात्री हृबेन सांग ने इसके बारे में लिखा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थल को स्थायी रूप देने के लिए उनके संस्कार स्थल पर एक बड़े स्तूप का निर्माण कराया था। वर्तमान समय में कुशीनगर की आध्यात्मिक आभा में चार चांद लगाते विभिन्न देशों के कई बौद्ध मंदिर मौजूद हैं। वर्तमान में कुशीनगर को और भव्यता प्रदान करने के लिए पुरातत्व विभाग उत्तरप्रदेश पर्यटन एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहित बौद्ध भिक्षु भदंत ज्ञानेश्वर लगातार प्रयासरत हैं। यहां पर चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों के बौद्ध मंदिरों, ऐतिहासिक खंडहरों के अलावा कुशीनगर की खुदाई से मिलीं ऐतिहासिक विरासतों को संजोए राजकीय संग्रहालय भी हैं, जो इतिहास के प्रति रुचि रखने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। विश्व बंधुत्व का संदेश देता यह पुरास्थल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र है।
कब और कैसे पहुंचें: कुशीनगर (कसियां) गोरखपुर से 51 किमी की पूर्व देवरिया जनपद से 35 किमी उत्तर एवं पडरौना जिला मुख्यालय से 20 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इन तीनों नगरों से बस या निजी वाहनों से पहुंचने की उत्तम व्यवस्था है। प्रमुख बौद्ध स्थल होने के कारण यह देश के लगभग सभी टूरिस्ट सेंटरों से जुड़ा हुआ है। रेलमार्ग द्वारा भारत के किसी भी हिस्से से आप गोरखपुर पहुंच सकते हैं। यह यहां का निकटतम रेलवे स्टेशन है। पर्यटन के हिसाब से उपयुक्त मौसम फरवरी से मार्च तक रहता है। यहां ठहरने के लिए महंगे से महंगे होटलों से लेकर बिडला धर्मशाला तक उपलब्ध है। जहां पर्यटक अपनी सुविधानुसार रह सकते हैं। यहां की भाषा भोजपुरी और हिंदी है। वैसे अंग्रेजी भी बोली और समझी जाती है।