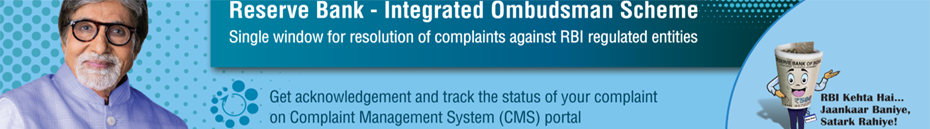भारतीय संस्कृति ने पारिवारिक जीवन को एक उच्च स्तरीय योगाभ्यास कहा है। योग साधना का अर्थ है अपरे सीमित और संकुचित व्यक्तित्व को असीम और विराट चेतना से एकाकार कर देना। गृहस्थाश्रम सीमित से असीम की ओर अग्रसर होने के क्रमश: आगे बढ़ाने का अभ्यास करने के लिए ऋषियों द्वारा प्रणीत एक प्रयोगशाला है। प्राचीनकाल में अधिकांश ऋषि विवाहित ही होते थे। आश्रमों में ऋषि-मुनि ऋषिकुमारों को पढ़ाते थे तो उनकी पत्नियां ऋषि कन्याओं को शिक्षा देती थीं। हमारी संस्कृति के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन और प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक धर्मकृत्य है।
इस धर्मकृत्य को संपन्न करते हुए ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विस्तार आरंभ करता था और परिवार के अन्य सदस्यों तक अपनी आत्मभावना की परिधि को व्यापक बनाता था। स्वाभाविक ही है कि विवाह के उपरांत व्यक्ति का क्षेत्र और व्यापक बन जाता है तथा उसमें स्त्री, पुत्र, पति, संतान, स्वजन, सगे-संबंधी, पड़ोसी और घर के पशु-पक्षी तक सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार विवाहित स्त्री या पुरुष यदि विवाह बंधन के मर्म को समझें तो क्रमश: अपनी उन्नति की ओर बढ़ते चलते हैं। दूसरों के लिए अपने को भूल जाने की, अपने स्वार्थ को कम करने तथा परिवारजनों की हित चिंता को महत्व देने की, अभ्यास साधना से ही गृहस्थ साधक आगे बढ़ सकते हैं और शनै:शनै: तुच्छता को महानता में, संकीर्णता को उदारता में परिणित करने चल सकते हैं।
भारतीय मनीषियों ने विवाह जैसे पवित्र धर्मकृत्य से और भी कई महान उद्देश्यों की पूर्ति की कल्पना की थी। मानव प्रकृति की निरंकुश प्रवृत्तियों को संयमित करने, प्रकृति द्वारा आयोजित सृष्टि क्रम के विस्तार को सुव्यवस्थित रूप देने, समाज में स्वस्थ वातावरण बनाने जैसे प्रयोजन भी इस धर्मकृत्य के साथ जोड़ रहे थे। एक कुरुप और बेडौल आकार के पत्थर को मूर्तिकार जिस प्रकार छैनी और हथोड़ी लेकर सुंदर मूर्ति बनाने में संलग्न होता है और अपने अन्तस की मूर्ति को पाषाण शिला में साकार कर देता है, उसी स्तर की साधना गृहस्थ धर्म की कल्पना करते समय आवश्यक समझी गई होगी और उस माध्यम से उस साधना को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया होगा। प्रकृति के निरंकुश आवेगों को संयत करने का उपाय भी इस प्रकार किया गया, जिनका निर्बाध प्रकटीकरण मनुष्य को पशु और असभ्य जंगली बना सकता है। उन आवेगों के साथ ही परिष्कार और शोधन की छैनी चलाकर मनुष्य की असंस्कृत चेतना को सुंदर आकार भी देने का सहज क्रम बनाया गया।
अन्य साधनाओं में लगे साधकों में अहंकार का भाव भी जल्दी आ सकता है परंतु गृहस्थ एक ऐसा योगाभ्यास है,जिसमें सब कुछ सहज ढंग से चलता रहता है और साधक निरहंकार होकर अपने पति-बच्चों, स्वजन, संबंधियों में अपनी आत्मा का दर्शन करता रहता है। संभवत: इसी कारण मनीषियों ने गृहस्थाश्रम को चारों आश्रमों से महत्वपूर्ण और उनका मुख्य केंद्र बनाया।
महर्षि वशिष्ठ कहते हैं: गृहस्थ एव पजते, गृहस्थ स्तप्यते तप:। चतुर्णामाकश्रमणा तु गृहस्यस्तु विशिष्यते। वशिष्ठ स्मृति 8/14
अर्थात- गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी है, इसलिये चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका सिरमौर है। गृहस्थ ही वास्तविक यज्ञ करते हैं।
वेदमूर्ति पं. श्री राम शर्मा आचार्य का कथन है-‘गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है।’
संतानोत्पत्ति तो विवाह का एक छोटा सा उद्देश्य है। वस्तुत: तो इस योग का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व की अपूर्णता को जीवन साथी के व्यक्तित्व से पूरा करना है। संसार में रहने वाला प्रत्येक मानव अपूर्ण है। किसी व्यक्ति में कोई गुण अधिक है तो किसी गुण का अभाव है। विशेषत: स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व की विशेषताएं तो भिन्न ही हैं और उसमें विशिष्ट गुणों का अभाव भी भिन्न है। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद स्त्री और पुरुष अपने स्वभाव के विपरीत गुणों को एक-दूसरे से मिलाकर एक संपूर्ण व्यक्तित्व का सृजन करते हैं। दोनों का संयोग समाज की इकाई बनाता है और वह इकाई ही सम्मिलित रूप से समाज को आगे बढ़ाती है।
यह एक मान्य और स्वयंसिद्ध सिद्धांत है कि दो भिन्न या विपरीत गुणों वाली वस्तुएं एक-दूसरे में जल्दी घुल-मिल जाती हैं और एक संपूर्ण इकाई का सृजन करती हैं, शक्ति का उत्पादन करती हैं। विद्युत की दो विपरीत धारायें मिलकर करंट पैदा करती हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वस्तु का आकार दोनों मिलकर चराचर, जगत को स्थिर रखते हैं। आग और पानी का संयोग वाष्प शक्ति उत्पन्न करता है। सृष्टि नियन्ता की रचना ही ऐसी है कि उसमें दो विपरीत गुणों, विभिन्न विशेषताओं में भाई-चारे और साझेदारी के संबंध शीघ्र ही स्थापित हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष की चारित्रिक, स्वभावगत, व्यक्तित्व की और शरीर की भिन्न-भिन्न विशेषताएं एक-दूसरे से आबद्ध होकर संपूर्ण मनुष्य की सर्जना करती हैं। यदि व्यक्तित्व के समग्र विकास की उपेक्षा कर दाम्पत्य जीवन को क्षुद्र प्राकृतिक आवेगों तक सीमित रहने दिया जाये तो गृहस्थाश्रम की सारी महिमा, गरिमा नष्ट होकर रह जाती है। लौकिक भाषा में यदि गृहस्थ धर्म का मूल्यांकन किया जाये तो यही प्रतीत होगा कि गृहस्थी स्त्री और पुरुष का सम्मिलित साधना क्षेत्र है। कहा भी गया है कि गृहस्थी की तुलना साझे की दुकान से की जाती है। इसके दो साझेदार हैं स्त्री और पुरुष। साझे की दुकान तभी सफल होती है, जबकि साझेदार एक-दूसरे के स्वभाव, प्रकृति, गुण-दोष, आवश्यकता और विशेषता को समझते हों। एक-दूसरे का संपर्क और अपने साथी के स्वभाव के अवगत न होने के कारण साझे को दुकान जिस प्रकार चलना मुश्किल हो जाती है, उसी प्रकार पति-पत्नी एक-दूसरे को समझकर अपने व्यवहार की रीति-नीति निर्धारित न करें तो कलह, विग्रह और क्षति जैसे अनर्थ ही उत्पन्न होंगे।
सफल दाम्पत्य जीवन जीने वाले महापुरुषों के पारिवारिक जीवन का यदि अध्ययन किया जाये तो विदित होगा कि वे अपने जीवनसाथी को सुख और शांति देने के लिए अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छाओं को बलिदान करने की नीति अपनाते रहें हैं। स्वार्थ त्याग और जीवनसाथी की हितचिंता में संलग्न रहते हुए ही औरों के लिये भी त्याग करने की भावना का विकास होता है।
गृहस्थ क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, इसीलिए नहीं कि वह उदारता, स्वार्थ, त्याग की भावनाओं को नष्ट करता है और माया-मोह में बांध लेता है वरन् महानता और विकास की गति इसलिये अवरुद्ध हो जाती है कि लोग दाम्पत्य जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते और पत्नी, बच्चों की सेवा, उनके लिए सुख-साधनों की व्यवस्था को ही सद्गृहस्थ होने की इतिश्री मान लेते हैं। इस रीति-नीति को अपनाने वाले व्यक्तियों की परिवार के संबंध में स्पष्ट मान्यता यही होती है कि पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता एक स्थान पर रहें। साथ-साथ खायें-पीयें और एक-दूसरे को सुख-दुख में मदद करें। परिवार में भरण-पोषण कर लेने भर ही से पारिवारिक कत्र्तव्यों का निर्वाह हो जाता है यह मान्यता पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण है। थोड़े से लोगों के एक साथ रहने, साथ-साथ खाने-पीने और आपस में उठने-बैठने से ही परिवार नहीं बन जाता। साथ-साथ रहना ही परिवार कहलाता तो होटलों और धर्मशालाओं में कई व्यक्ति एक साथ रहते हैं, वहां एक साथ एक हॉल में खाते हैं।
परिवार के संबंध में अपनी मान्यता यह होनी चाहिए कि घर की ईंटें ही परिवार नहीं हैं। किसी परिवार के आधे लोग भले ही भिन्न-भिन्न देशों में रहें, हम उन्हें एक आदर्श परिवार कह सकते हैं। यदि उसके सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और संवेदना से सूत्र संबंध हों तो। पारिवारिक जीवन का प्राण ही प्रेम और परस्पर का सद्भाव है। यदि परिवार में सभी सदस्य परस्पर सद्भाव संपन्न हों, आपस में एक-दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हों, सौजन्यता, बलिदान और सेवा की वृत्ति हों तो वह परिवार आदर्श हो सकता है। परिवार साम्राज्य में इन आदर्शों की स्थापना पति और पत्नी के सम्मिलित प्रयासों द्वारा ही हो। वे शासक और शासिका हैं। इन आदर्शों की स्थापना स्वयं अपने जीवन में उनकी स्थापना करते हुए की जाये तो कौन कह सकता है कि घर-गृहस्थी मायाजाल है, बल्कि वह तो मोक्ष की, आत्मविकास की और आत्मकल्याण की सहज साध्य साधना है।