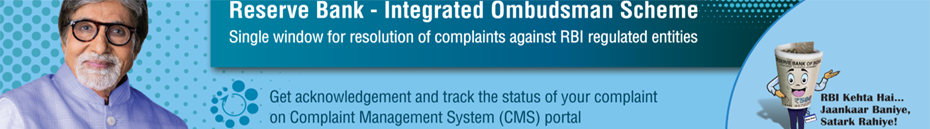कृमि-कीटकों द्वारा पहुंचाई जाने वाली विविध हानियों को देखकर मनुष्य को क्रोध आना स्वाभाविक है। वह उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, सो भी उचित है, पर भूल यहां होती है कि वह आवेश कृमिनाशक दवाओं के निर्माण तक सीमित होकर रह जाता है। इन दिनों अगणित कृमिनाशक दवाएं निर्मित हो रही हैं। उन्हें बनाने, खरीदने में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है पर उनसे क्षणिक लाभ होता है। तत्काल तो कुछ कीड़े मर जाते हैं, पर जो बच जाते हैं, वे तेजी से अपनी वंशवृद्धि करके अपने पूर्वजों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और मारने वालों से कस-कसकर बदला चुकाते हैं।
विविध प्रकार से क्षति पहुंचाने वाले कीटकों के संंबंध में इन दिनों बहुत शोध हो रहा है। मारक रसायनों का भी आविष्कार हो रहा है। यह उत्साह देखने-समझने ही योग्य है।
कपड़े नष्ट करने वाले कीड़ों की चार जातियां भारत में पाईं जाती हैं। 1. टीनिया पेलिओनेल, 2. टीनिओला विसेसिनिया, 3. ट्राइर्काफेगा एव्रप्लेटा, 4. वारखौसिनिया स्यूडोंप्रटेला।
इन चारों के अंडे-बच्चे ही कपड़ों को अधिक नष्ट करते हैं। बड़े होने पर वे उतनी अधिक हानि नहीं पहुंचाते।
ये कीड़े सीलन और गंदगी के उन स्थानों में पनपते हैं, जहां स्वच्छ हवा का प्रवेश भली प्रकार नहीं होता है। गंदगी और सीलन के संयोग से अनेक स्तर के कीड़े पनपते हैं और घर में जैसी वस्तुएं अथवा परिस्थितियां पनपने के लिए मिलती हैं, उसी के अनुकूल वे अपना आकार-प्रकार, रहन-सहन एवं क्रियाकलाप विनिर्मित कर लेते हैं। अन्न, कपड़ा, पानी, दूध, लकड़ी आदि जो कुछ उनके सामने आता है, उसी से निर्वाह करने की उनकी आकृति और प्रवृत्ति बन जाती है। इस मूल उद्गम कारण पर ध्यान न दिया जाए और केवल कीटनाशक दवाओं पर ही निर्भर रहा जाए तो काम चलने वाला नहीं है। उन्हें जहां भी अवसर मिलेगा, जो भी वस्तु कीटनाशक दवा के बिना मिलेगी, उसी पर कब्जा करेंगे और एक न सही, दूसरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। यही खाद्य पदार्थों के सहारे पेट में आ पहुंचते हैं और तरह-तरह के रोगों के कारण बनते हैं।
हानिकारक घरेलू कीड़ों में से ऊपर कपड़े काटने वालों की चर्चा की गई है, पर यह न समझना चाहिए कि उनकी हानि का क्षेत्र इतना ही सीमित है। जूएं, चीलर, खटमल, पिस्सू, मक्खी, मच्छर आदि के रूप में वे जन्मते और बढ़ते हैं। उनकी असंख्य जातियां ऐसी हैं, जो आंख से दिखाई नहीं पड़तीं पर हानि उतनी ही करती हैं, जितनी कि मक्खी-मच्छर आदि।
डी.डी.टी., सिलकोफ्लूराइड, क्लोरोडेन जैसे कीटनाशक रसायनों के छिड़काव से ये कीड़े या तो भाग जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, किंतु यह असर तभी तक रहता है, जब तक उन उपचारित कपड़ों को धोया न जाए। धूप और हवा का प्रभाव भी इन रसायनों का असर घटा देता है। इस दशा में छिड़काव बार-बार करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी खोज की जा रही है, जिससे कपड़ा-गोदामों में कई वर्ष तक इन कीड़ों से बचाव की निशर््िचतता हो सके।
रसायनशास्त्री हेरिक और डॉ. फे्र ने इस प्रयोजन के लिए कितने ही रसायन तैयार किए हैं। उनमें से किसकी उपयोगिता कितनी है, इसका प्रयोग-परीक्षण चल रहा है। अब तक के निष्कर्षों से इस कार्य के लिए चिरपरिचित नेफ्थलीन की अपेक्षा नई औषधि पैराडाइक्लोरी-बेंजीन अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है।
वस्तुएं अपने आप नहीं सड़तीं। वायुमंडल का प्रभाव उन्हें सड़ाता है। जहां की जलवायु सडऩ उत्पन्न करने में सहायक नहीं होती, वहां चीजें मुद्दतों तक यथावत सुरक्षित बनी रहती हैं। दक्षिण अफ्रीका के समीप एक छोटा सा द्वीप है-‘इचामोईÓ यहां पहुंचने पर प्राय: 150 वर्ष पूर्व मरे मुरदे ऐसी स्थिति में पाए गए, मानों वे अभी-अभी मरे हों। इस द्वीप की मिट्टी में मछलियां मरी पड़ी हैं। उनके द्वारा उठने वाली गैसें सडऩ को रोकती हैं। मैक्सिको का एक पर्वतीय क्षेत्र ‘नोयान जुमाटोÓ इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है कि वहां की विचित्र हवा के कारण न तो कोई वस्तु सूखती है और न सड़ती है। इस क्षेत्र के रहने वाले अपने मृतकों को कपड़े पहनाकर पहाड़ी गुफाओं में बैठा देते हैं और वे मुद्दतों तक ऐसे ही समाधि लगाए संतों की तरह बैठे रहते हैं।
अफ्रीका के ‘अंकोलाÓ क्षेत्र का एक भाग ऐसा है, जहां बनाया हुआ भोजन बहुत समय तक खराब नहीं होता। वहां के लोग एक बार भोजन बनाकर रख लेते हैं और उससे महीनों काम चलाते हैं।
धु्रव प्रदेश इस दृष्टि से और भी अधिक आश्चर्यजनक है। इंग्लैंड का एक अन्वेषक दल दक्षिणी धु्रव संंबंधी शोध करने के लिए सन् 1842 ई. में कैप्टन कौस के नेतृत्व में वहां गया था। मौसम की प्रतिकूलता के कारण उसे वापस लौटना पड़। इस दल का एक तंबू और उसमें कुछ खाद्य पदार्थ वहां छूट गए। सन् 1911 ई. में नार्वे के अन्वेषी रोल्ड एमंडसन जब वहां गए तो 70 वर्ष बाद भी वे वस्तुएं पूर्णत: सुरक्षित और उपयोग के लायक पाई गईं।
अमेरिका का एक पर्वतारोही विल्सन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने सन् 1934 ई. में आया था। लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही वह रास्ते में ठंड से अकड़कर मर गया। दूसरे साल एक दूसरा अन्वेषक दल एरिक सिंपटन के नेतृत्व में उधर पहुंचा तो उसे पूर्ववर्ती यात्री का शव पूर्णत: सुरक्षित मिल गया।
आर्कटिक हिमक्षेत्र मेंं प्रागैतिहासिक काल के कितने ही दुर्लभ प्राणी गड़े हुए पाए गए हैं। इनमें दो हजार वर्ष पूर्व मरा एक वेरेसोविका जाति का पशु भी था, जिसका मांस इस स्थिति में बना हुआ था कि उसे खाया जा सके। रूस के शोधकर्ताओं ने पांच हजार वर्ष पुराना एक सरीसृप हिम प्रदेश में इस स्थिति में पाया कि उसका शवच्छेद करके उस प्राणी की शरीर-रचना को भली प्रकार जाना जा सका।
सह्य, सुखद एवं उपयुक्त वातावरण मेें न केवल शरीर ही स्वस्थ रहता है, वरन पेड़-पौधे तक अधिक विकसित होते और फलते-फूलते हैं।
उत्तरप्रदेश में पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय से प्रकाशित ‘फारमर्स डाइजेस्टÓ पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण खोजों से यह सफलता मिल गई है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटाकर पौधों को दोगुनी तेजी से उगाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण खोज स्टेनफोर्ड कैलिफोर्निया की कारोनगी संस्था के सहयोग से सफल हो सकी है।
सामान्यत: वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21 प्रतिशत होती है। उसे घटाकर 5 से 9 प्रतिशत कर दिया गया तो पौधे दूनी तेजी से उगे और फल-फूल देने में आश्चर्यजनक वृद्धि संभव हो सकी।
यों अधिक ठंड भी उपयोगी नहीं पर अधिक गरमी का वातावरण भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं पड़ता। बड़े आदमी हीटर, कूलर और एअरकन्डीशंड यंत्रों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से सहने योग्य, वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उसमें प्रकृतिप्रदत्त समरसता और जीवनदायिनी शक्ति कहां रहती है।
यदि हम सचमुच जिंदगी से प्यार करते हैं और स्वास्थ्य-संपदा के मूल्य से परिचित हैं तो धनी या बड़े आदमी बनने का लोभ छोड़कर हमें स्वच्छ जलवायु का जीवन अपनाना चाहिए।