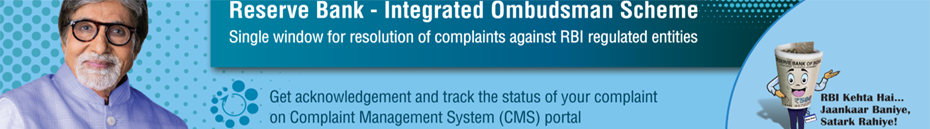प्रात:कालीन भ्रमण के लिए घने अंधेरे उठना मेरी प्राथमिकता रहा है, जिसे मैंने अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया है। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका था। मैंने कंबल छोड़ा, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुआ और सड़क पर आ गया। आस-पास कोई खुली जगह न होने के कारण खाली पड़ी सड़कों पर तेज कदमों से चलना ही भ्रमण की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए काफी है। सो करना मजबूरी भी है। शरीर में रक्त का संचार सही रखने और शरीर को दुरस्त रखने के लिए इसे सामान्य व्यायाम की संज्ञा जो दी गई है। उस दिन सुबह के चार बजे थे। मंदिर से कुछ महिलाओं के स्वर सुनाई दे रहे थे। मंदिर के द्वार से भीतर झांका तो देखा दस-बारह महिलाओं का समूह है, जो दीपक जलाकर पूजा कर रहा है। मैं अपने शीघ्र उठकर घूमने को ही औरो से उत्तम मानता था, किंतु महिलाओं ने मेरा भ्रम ही तोड़ दिया कि मुझसे पहले वह बिस्तर छोड़कर नहा-धोकर पवित्र स्थल पर आ बैठी हैं। यह क्रम लगभग पंद्रह दिन चला। घर में पत्नी से चर्चा की तो वह तपाक से बोली- तुम नास्तिक क्या जानो पूजा पाठ में कितनी शक्ति है। घने अंधेरे उठकर महिलाएं अवश्य ही लक्ष्मी का व्रत अनुष्ठïान कर रही होंगी।
अपने शरीर को कष्टï देकर ऐसे अनुष्ठïानों का लाभ भी कुछ होता है? मैंने पत्नी पर प्रश्र दाग दिया तथा उसकी प्रतिक्रिया जानने हेतु उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी थीं।
अजीब आदमी हो। व्रत और अनुष्ठïान किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं? पत्नी ने सहजता से कहा।
घने कोहरे उठकर मंदिर में जाना, पूजा करना, शरीर को कष्टï देना, आखिर कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है।
तुम जानबूझकर किसी की आस्था का मजाक उड़ा रहे हो, जो उचित नहीं है। पत्नी झल्ला गई, महिलाएं कोई भी अनुष्ठïान अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करती। व्रत के पीछे उनकी धारणा यही होती है कि परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो।
मैंने पत्नी से बहस करना उचित न समझा। अपने कार्यों में जुट गया। सुबह से शाम तक शहर की सड़कों पर भाग-दौड़ में पता ही नहीं चलता कि सुख-चैन कहां छूटता जाता है। व्यापार में लेन-देन, उधार-नकद, माल की शिकायत, महंगा-मंदा, धर्मादा, कमीशन और न जाने ऐसे ही कितने शब्द जुड़ते चले जा रहे है। हर वस्तु की गुणवत्ता, मांग-पूर्ति का नियम और न जाने कैसी-कैसी संविदाओं से जूझना पड़ता है। यही तो भौतिकता को गले लगाने का अंजाम है। बाप-दादाओं के समय में भी व्यापार होते थे, मगर इतनी मारा-मारी नहीं थी, झूठ-फरेब, धोखेबाजी नहीं थी। ईमानदारी में जो सुकून था, उसके अब दर्शन भी नसीब नहीं है। शुक्र है कि सुबह का भ्रमण जारी है, अन्यथा शरीर को भी ना-नुकर करने में देर न लगती। वह भी देनदार व्यापारी की तरह तकाजे पर मना करने, आगे की तारीख रखने से बाज नहीं आता। जब तक जान में जान है, शरीर को भरपूर साथ निभाना ही चाहिए। अन्यथा कब श्वांसों की डोर टूट जाए। मगर इससे डरता ही कौन है… जिसे देखो वही आपाधापी, लूट-खसोट में लगा हुआ है। एक भूख-सी है,जो उसके अस्तित्व को ही निगले जा रही है। भूख से अधिक खाने की फिराक में यह देख ही नहीं पा रहा है कि किस-किसका हक हजम कर रहा है। वैचारिक उथल-पुथल मेरे मानस पटल पर उभरकर जैसे मेरी चिंतन सामथ्र्य पर प्रश्रचिन्ह खड़ा कर रही थी।
एक अरसे बाद दोपहर को घर पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। बाजार में एक युवा व्यापारी असमय कालग्रस्त हो गया। माता वैष्णों देवी के दर्शनों हेतु पांच मित्र सुबह ही घर से चले थे। तेज गति से चल रहे यातायात में उनकी जीवन गति थम गई। उन्हें आभास ही नहीं हुआ, सभी कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। सीमेंट के खंभों से लदे ट्रक से पीछे से टक्कर लग गई। क्रूरकाल उन्हें देवी दर्शन के बहाने ही घटनास्थल पर ले गया था। परिजनों ने सुना तो स्वयं को लुटा-पिटा अनुभव करने लगे। भिड़ंत इतनी भयानक थी, कि कोई नहीं बचा। बाजार में सूचना आते ही शोक की लहर फैल गई। बाजार बंद हो गया। सप्लाई एवं तकाजे का कोई अवसर ही पास न था, सो घर लौट आया। पत्नी का व्रत था, सो दोपहर भोजन की समुचित व्यवस्था न थी। मैंने पुन: पत्नी पर व्यंग्य बाण किया- माता की भक्ति भी व्यर्थ चली गई। इतनी हृदयविदारक घटना घटित हुई है।
पत्नी चिहुंकी- नि:संदेह बुरा हुआ। किंतु इसमें माता का क्या दोष, विधाता की इच्छा से ही सृष्टिï चल रही है। उन सभी की मौत विधाता ने इसी प्रकार रची होगी, अन्यथा कई बार भयानक भिड़ंत में चकनाचूर गाडिय़ों में व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आती।
यानी कहीं मेरी बात चलने नहीं दोगी। मैं तो कहता हूं कि खाया-पिया ही शरीर के साथ रहेगा। सो जब तक दम में दम है खाओ-पियो और आनंद से रहो। मैं सहज भाव से कह गया।
पत्नी भोजन की व्यवस्था में जुट गई। उसके व्रत, अनुष्ठïानों ने उसके शरीर को इतना जर्जर कर दिया कि उसे चलते हुए चक्कर आने लगे थे। कई बार अच्छे चिकित्सक के पास चलने के लिए कहा तो उसने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया- शारीरिक कष्टï झेलकर यदि परिवार में समृद्धि आती है, तो मुझे समस्त कष्टï स्वीकार है।
पत्नी के सम्मुख मेरी कुछ न चली, एक बारगी तो उसने मेरे भोजन को भी संतुलित कर दिया। बिना तला भोजन देकर कहने लगी-शरीर स्वस्थ रखना है तो सादा भोजन कीजिए। घर में यदि कुछ गर्म बोलने की धृष्टïता की तो पत्नी का करूण स्वर उभर आया- तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है उस पर परिवार का भी अधिकार है। सो अपने लिए नहीं, परिवार के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अब तो मेरे पास कोई विकल्प शेष ही नहीं बचा, जो जीभ के स्वाद के लिए चटपटे और जायकेदार भोजन की फरमाइश करता।
ये पत्नियां भी अजीब होती हैं। पूरे परिवार का दर्द जैसे अपने आंचल में ही छिपाये रहती है। समाज में अपने परिवार की साख बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करतीं। कभी फाके में समय काटती हैं, कभी एक धोती में महीनों बिता देती हैं, किंतु किसी को कानोकान भनक भी नहीं लगने देतीं। यकायक कुछ प्रसंग मेरी आंखों के सम्मुख तैर गए।
एक शाम को मेरा सिर भारी था। जैसे दिमाग की नसें फटने की आतुर हों, तनिक-सी भनक लगते ही पत्नी सिर दबाने बैठ गई। दर्द निवारक बाम के साथ तब तक सिर दबाती रही, जब तक कि मैंने उसे इंकार नहीं किया। तिस पर बार-बार यही दुहाई-इतना मरने-खपने की क्या आवश्यकता है। आराम से घर का गुजारा चल रहा है, रोटी ही खानी है। जिसके लिए भगवान का दिया बहुत कुछ है। फिर इतनी दौड़भाग क्यों?
मैंने पत्नी को समझाया- पगली… सिर्फ रोटी खाने भर से दुनियादारी निभाई जा सकती तो ठीक था। समाज में रहने के लिए एक स्तर बनाकर रहना भी अनिवार्य होता है। जो बिना धन के संभव नहीं है।
कल ही तुम किस्सा सुना रहे थे न… एक युवा व्यापारी अपने साथियों सहित कैसे कूच कर गया। क्या पैसे से उसका शरीर जीवित किया जा सका? पत्नी का प्रश्र तर्कसंगत था।
फिर भी…कष्टï में रहने की कल्पना भी तो नहीं की जा सकती? मैंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
ठीक है, परिश्रम करो, किंतु परमात्मा का स्मरण अवश्य करो। जिसे तुम भाग्य कहते हो, वह विधाता की सृष्टिï का ही चमत्कार है। पत्नी किसी ज्ञानी संत की भांति मुखर थी।
तुम्हारी हर बात, मैं स्वीकारने हेतु तैयार हूं, सिर्फ इतना बता दो… पूजा पाठ क्यों किया जाता है। मंदिर-मस्जिद क्यों बनाए जाते हैं? मैंने अपना बेतुका प्रश्र पत्नी से किया।
इसमें भी कोई बड़ी बात है… परम शक्ति की आराधना के लिए जिस स्थान का प्रयोग किया जाता है, वही मंदिर है या अन्य कोई पूजा स्थल है। पत्नी सहजता से कह गई।
यह मेरे प्रश्र का उत्तर नहीं है। तुम जब भी खाली होते हो, ऐसे ही बेतुके प्रश्र करके दिमाग खराब करते हो। भक्ति और विश्वास मन के विषय है, मगजपच्ची के नहीं। पत्नी झल्ला गई।
अच्छा भाग्यवान… एक कड़क चाय तो पिला दो… तुमसे बहस करना अच्छा लगता है…। मैं पत्नी की ईश्वर के प्रति श्रद्घा भावना का सम्मान करते हुए खीज मिटाने लगा।
हां… कड़क चाय पीकर कलेजा फूंक लो। एक गिलास गर्म दूध कर देती हूं। पत्नी ने मेरे स्वास्थ्य की चिंता की।
तुम परमात्मा पर विश्वास करती हो न… फिर खान-पान की वस्तुओं में भेद क्यों कर रही हो। यदि मुझे स्वस्थ रहना है तो जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पुन: तर्क दिया।
फिर पागलपन सवार हो गया….प्रकृति ने अपने आंचल में एक से एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ संजोए हैं। फिर बनावटी पदार्थों से लगाव क्यों रखा जाए… सृष्टिï का विनाश ही इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर से बड़ा समझने लगा है। उसके उपहारों में मीन मेख निकालकर अपने प्रयोग कर रहा है, ऐसे में सभी प्रयोग सफल हों, कैसे कहा जा सकता है? पत्नी, प्रकृति और ईश्वर के अनमोल उपहारों की उपलब्धता को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रही थी तथा उनके अस्तित्व की पहचान आश्चर्य के रूप में कराना चाहती थी।
मैं बार-बार विषय पर आना चाहता हूं और तुम हो कि मुझे प्रकृति के गूढ़ रहस्य से बार-बार उलझा देती हो…। मैंने तर्क दिया।
अपनी परिभाषाओं से सिद्धातों से बहस कीजिए… तुम्हारी धीर गंभीर बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती…। पत्नी ने चर्चा समाप्त करने के उद्देश्य से कहा।
मगर मुझे तो तुमसे बातें करने में आनंद आता है…। मैंने चुटकी ली।
बातें करने में या लड़ाई की भूमिका बनाने में…।
मतलब? मैं चिहुंका।
आदमी लोग तो घर से बाहर ही ठीक हैं। समाज की व्यवस्था अच्छी ही थी, कि पति आजीविका के लिए घर से बाहर रहे और पत्नी घर में बाल-बच्चों की देखभाल करे।
मगर आजकल तो सभी कुछ उल्टा हो रहा है… पत्नियां दफ्तरों में काम कर रही हैं और पति घर की देखभाल? मैंने अपना पक्ष रखा।
सब प्रकृति की व्यवस्थाओं में दखलंदाजी है। पत्नी ने अपना पक्ष रखा। फिर भटक गई। तुम्हारी पसंद की चाय बना लाती हूं वरना तुम्हारी बातें मेरा दिमाग खाली करके ही रहेंगी। पत्नी किचिन में चली गई।
मैं हंसे बिना न रह सका। पत्नी का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां कहीं तर्क की सामथ्र्य कम होती प्रतीत होती है, वहीं वह किचिन का रूख करके चर्चा का पटाक्षेप कर देती है।
थोड़ी ही देर में पत्नी चाय बना लाई। बड़ी बेटी ट्यूशन पढ़कर लौट आई, बेटा कहीं सड़क पर गिर पड़ा। जिसके घुटने छिल गए। पेंट भी फट गई। उसे देखते ही पत्नी उसे डांटने लगी-देखकर नहीं चला जाता क्या?
अरे! अब इसे डांटने से क्या लाभ… यह ईंट-पत्थरों का शहर है… यहां गांव की धरती तो नहीं है कि गिरकर भी चोट न लगे।
यहां भी आप अपने पागलपन से बाज नहीं आ रहे हैं। पत्नी ने मुझे डपटा।
पागलपन क्या… इसे भी विधाता की मर्जी कहिए ना… कि विधाता ने चोट लगा दी।
चोट विधाता ने नहीं, व्यक्ति के कुकर्मों ने लगाई है… व्यक्ति ने ही अपने हस्तक्षेप से प्रकृति से खिलवाड़ किया है। हरियाली समाप्त करके कांक्रीट के जंगल उगा दिए हैं, फिर उसका परिणाम तो भुगतना ही है…। पत्नी का तर्क अकाट्य था, जिस पर बहस करना उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। जिस पाप विषयक बिंदु पर मैं धर्म और मंदिर को जोडऩा चाहता था, उस विषय की भूमिका ही नहीं बन पा रही थी। मैं बार-बार पुस्तक में लिखी दो पंक्तियों पर अपना चिंतन मुखर करना चाहता था, जिसमें रचनाकार ने पाप का परिचय दिया था तथा कहा था- न जन्म लेता। अगर धरा पर, धरा बनी ये मसान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती।
पत्नी बेटे की मरहम पट्टी में लगी थी। पूरा परिवार बेटे की चोट पर पीड़ा का अनुभव कर रहा था। पत्नी का सेवाभाव बार-बार उस धरती का अस्तित्वबोध कराने में समर्थ प्रतीत हो रहा था, जिसे रत्नगर्भा कहा जाता है। जिसका समूचा समर्पण मानव उत्थान के लिए ही है।
तभी मोबाइल की घंटी घनघनाई। मित्र का फोन था, कह रहा था- हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास चलना है, अपने भाग्य की लकीरें बंचवानी है।
मैं ठहाका मारकर हंसा- मित्र, भाग्य की लकीरों में कुछ नहीं है… जो है जैसा है, भोगते जाओ… इसी में सबकी भलाई है।
पत्नी पास खड़ी झल्ला रही थी-फोन बंद करो… कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर के बहुत से काम निपटाने है, आज घ्रर में हो तो राशनपानी की व्यवस्था कर दो। मैं सामान की लिस्ट देती हूं… जाकर बाजार से ले आओ। मैंने आज्ञाकारी पति की भांति चुपचाप पत्नी का आदेश स्वीकारने में ही भलाई समझी और सामान की फेहरिस्त लेकर बाजार का रूख किया।