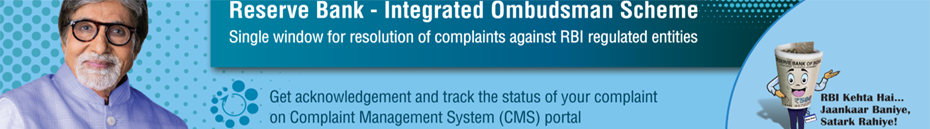अगर अंधेरा न होता तो उजाले को कौन पहचानता। अगर अंधेरा न होता तो उजाले का महत्व को हम समझ ही न पाते। रोशनी जीवनदायिनी है-शायद यही समझने-जानने के लिये अमावस्या की रात को दीपों से रोशन किया जाता है। दीपावली अर्थात प्रकाशोत्सव। इस पर्व के साथ कथा-पुराणों या इतिहास की कितनी ही घटनाएं क्यों न जुड़ी हों, किन्तु सत्य तो यही है कि दीपक जलने से अंधेरा मुंह छिपा लेता है। यह दीप ज्ञान का भी हो सकता है, जो अज्ञानता को दूर करे। यह दीपक संघर्ष का भी हो सकता है, जो जीवन को नई दिशा दे, तूफानों से लडऩे की हिम्मत दे और निरन्तर आगे बढऩे का मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन आज परिदृश्य बदल गया है- भ्रष्टïाचार, स्वार्थ और अवमूल्यों की ऐसी विषैली हवा चल पड़ी है, कि हमारे गौरवमय इतिहास, संस्कारों और आदर्शों के दीये बुझ गए हैं। रोशनी फैलाने का अपना कर्तव्य वह बखूबी निभा रहा है, किन्तु हमारी आंखे उजाले को देखने की अभ्यस्त ही नहीं रह गई हैं। शायद इसीलिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था।
धूप कहा ऐसा तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा।
भागने को न मिली जब राह, आदमी के भीतर आ बसा।
दीपावली को अगर मानवीय सभ्यता के इतिहास के नजरिये से देखें, तो साफ होता है कि असभ्यता व अंधेरे के खिलाफ इंसानी मुहिम की कई-कई सदियां बीत चुकी हैं। पर आज हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ नजर आ रहा है, क्या वह वाकई उजाला है। फैज के शब्दों में कहें, तो ये दाग-दाग उजाला, ये शब, गुजीदा सहर। उजालों में इतने भारी-भारी दाग, उजालों के वेश में आते अंधेरे, इस वर्ष की दीपावली का इससे अलग मंजर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा भी काला हो चुका है यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा काली अर्थव्यवस्था की शक्ल में हैं। काली लक्ष्मी, उजली लक्ष्मी का भेद वैसे भी खत्म ही हो चला है। गौर से सोचिए, कहीं आसपास के गहराते अंधेरे का बड़ा कारण यही न हो?
स्वतंत्रता संग्राम से विरासत में मिले कुछ मूल्यों के चलते काली लक्ष्मी व उजली लक्ष्मी का भेद लंबे अर्से तक रहा। काली लक्ष्मी का रोल राजनीति, व्यवसाय व आम आदमी की जिंदगी में था, पर काफी दबी ढकी, सिकुड़ी-सहमी शक्ल में। अब तो काली लक्ष्मी खुलकर दौड़ रही है। उजली लक्ष्मी सहमी-सिकुड़ी हालत में है और पूरे समाज में यह स्थिति स्वीकार कर ली गई है। धन-धान्य, सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदंड बन गया। लक्ष्मी का चेहरा काला हो या उजला? यह सवाल अप्रासंगिक हो गया। ठीक इसी बिंदु पर आकर लगता है कि इस गहराते अंधेरे में सब बराबर के हिस्सेदार हैं। व्यक्तिगत आचार-विचार में हमने इतनी कालिखों से समझौते किए हैं कि रोशनी की सामूहिक भावना सिर्फ फ्राड बनकर रह गई है। ऐसा एकदम से नहीं हुआ। यह धीमी प्रक्रिया कई बरसों से चलकर इस परिणति तक पहुंची है।
दीपावली का एक ओर जो चेहरा सामने आया है, वो विशुद्ध कारोबारी है। उसका आस्था, परंपरा, पूजन से कोई वास्ता नहीं। दौलत की मोटी तह के जमाने में ही इस चेहरे का तंत्र छुपा है। इससे ऐसी मान्यता शक्ल अख्तियार कर रही है कि दीवाली पकवानों और पूजन का पर्व नहीं, बल्कि लेन-देन और जनसम्पर्क बढ़ाने का त्यौहार है। सत्ता के दलालों, साहबी संपर्कों के जरिए लोगों के जायज-नाजायज काम करने का ठेका लेने वाले तथाकथित छुटभैये नेताओं और जनसम्पर्क के जरिए ही आजीविका (शानदार जिंदगी) कमाने वाले लोगों के लिये यह पर्व कुछ अलग है। लक्ष्मी पूजन या असत्य पर सत्य की विजय के उल्लास का नैतिक संदेश देने वाले पर्व की अपेक्षा उनके लिये यह ऐसा सुनहरा अवसर है, जिसे मिठाई के डिब्बे, फलों की डलियों, सूखे मेवों की टोकरियों, सीलबंद (ताकि गारंटी रहे) विदेशी शराबों-सिगरेटों के कार्टरों और अन्य विदेशी उपहारों की मार्फत विशुद्ध जनसंपर्क को शुद्ध लाभ में बदला जा सकता है। साल भर बेसब्री से इस पर्व का इंतजार करता यह वर्ग सत्ता व पहुंच के ठिकानों की फेहरिस्त बनाने में लगा रहता है, ताकि लक्ष्मी के प्रवाह की निरंतरता के लिये इन आकाओं का पूजन किया जा सके।
विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना था कि जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं। मिल्टन ने कहा कि लम्बा और कठिन है वह मार्ग जो नर्क से प्रकाश की ओर जाता है। प्रकाश की ओर जाने वाले रास्ते की कठिनाईयों से घबराकर ही हमने दीपक अपने पीछे रख लिया है। हमें सुविधाओं में जीने की आदत पड़ गई है। हम जनसेवा को भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझने लगे हैं। हमारी नयी पीढ़ी पश्चिम की हवा के साथ उड़ती चली जा रही है। आखिर क्यों? जनसेवा को व्यापार बनाने वाले को पुरुषोत्तम राम कौन थे समझाएं भी तो कैसे? हर रोज तो सीता का अपहरण होता है। स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिये। वह धरती में कैसे समा जाए। उसकी तो बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और रावण का कुछ भी नहीं होता। रावण की मुखबिरी करने के लिये कोई विभीषण भी सामने नहीं आता, क्योंकि विभीषण पहले ही सत्ता के हाथों बिक चुका होता है।
आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बदहाल अर्थव्यवस्था है जिसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलेगी। मुद्रास्फीति ने सरकार के सारे दावों को दरकिनार कर विकास के सारे रास्तों को रोक दिया है। नतीजन आम आदमी के सामने दो जून रोटी की जुगाड़ कर पाना आसमान से तारे तोडऩे के समान है। मध्यम वर्ग इस महंगाई का सबसे बड़ा शिकार हुआ है। आय के सीमित साधनों के चलते सपनों का ताना-बाना जो बुन रखा था, वह तार-तार हो गया हैं। इन हालात में वह संतान को खासकर बच्चों को झूठी दिलासा भी नहीं दे सकता क्योंकि उसे भविष्य में आर्थिक भंवर के जाल से निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। उसकी हालत तो उस आदमी जैसी है जिसे यही नहीं पता कि उसे करना क्या है? उसकी आंखों की रोशनी पता नहीं कहां लोप हो गई है। सोच तो उसे इस बात का है कि दीपावली की औपचारिकता वह निभाए तो कैसे निभाए। उसके लिये भी तो कुछ चाहिए। महंगाई के इस तरह दुनिया के दूसरे नम्बर के आबादी वाले सबसे बड़े देश में स्थायी रूप से बस जाने का ही नतीजा है कि आज मेहनत-मजदूरी करने वाला आदमी, निम्र आय वर्ग वाला आदमी, प्राइवेट फर्मों दुकानों-फैक्ट्ररियों में और ट्रस्टों में तनख्वाह के नाम पर कागज के चंद टुकड़ों पर सब्र करने वाले आदमी के लिये त्यौहार एक समस्या ही नहीं एक अभिशाप बन चुका है। वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि साल में कोई त्यौहार नहीं आए। पैसे से खाली क्या वह दीपावली के इस त्यौहार पर अपने परिवार में खुशहाली ला पाएगा? क्या वह बच्चों की सूनी आंखों में चमक ला पाएगा और क्या वह घर में उस दिन रोशनी कर पाएगा? यदि नहीं तो वह दीपावली वाले दिन परिवार सहित अंधेरे बंद कमरे में खुद को और त्यौहार को ही कोसता रहेगा और यह प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर यह त्यौहार ही न आए। गौरतलब है कि मालिक या फर्म के द्वारा दिए गए एक मिठाई के डिब्बे से उसकी आंखों में न तो चमक आएगी और न त्यौहार के प्रति खुशी का अंदाज, जिसकी उसने कभी कल्पना की थी।
आखिर विचारणीय यह है कि यह त्यौहार किनके लिये है? महंगाई के दौर में यह तो निश्चित ही है कि यह त्यौहार आम आदमी के लिये तो कतई नहीं है। फिर बाजारों की चमक-दमक दुकानों की सजावट, फुटपाथ को पार कर आधी सड़क घेरकर लगाई गई दुकानों पर लगी अनगिनत रंगों की मिठाईयां, जगह-जगह लगे लुभावने बैनर और बड़े-बड़े शोरूम आखिर किसके लिये हैं? निश्चित है कि यह सब लुब्बा-लवाब पैसे वाले धनपतियों, कालाबाजारियों, नए-नए दरबारियों, विधायकों, सांसदों, राजा की तरह जिंदगी गुजारने वाले मंत्रियों, दलालों, ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों, डाक्टरों और इंजीनियरों के लिये हैं। जाहिर है कि उपरोक्त महानुभावों के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में महंगाई का इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनके लिये तो रोज त्यौहार ही है। इनकी संतानों के चेहरों पर तो वैसे ही चमक बरकरार रहती है। देखा जाए तो उनके बच्चे का तो रोजाना का खर्चा ही इतना होता है जो कल्पना से परे है।
प्रकाश की खोज में कदम बढ़ाते हुए मानव ने अपनी अंतसंज्ञा को ही लौ के रूप में बाहर प्रतिष्ठिïत किया है। दीपावली के दिन पंक्तिबद्ध दीपमाला हमें संकेत करती है निरन्तर प्रकाशमय होने के लिये, दीप्ति, कान्ति और उज्जवलता को अपनाने के लिये। क्षण-क्षण जलता हुआ, न्यून होता हुआ स्नेह पुकार-पुकार कर कहता है, मुझे जलती हुई यह लौ पिये जा रही है। काल, अन्तर के तत्वों को, समाप्त करने में लगा हुआ है। इस दीपावली पर यह सवाल अपने-आप से करना बहुत प्रासंगिक लगता है। जवाब पूरा-पूरा न भी मिलता हो, पर नाउम्मीदी पूरे तौर पर अपना असर नहीं जमा पाती। गहराते अंधेरे, काली लक्ष्मी के बढ़ते असर के बावजूद उजाले पूरी तौर पर गायब तो नहीं हुए है। आपके-हमारे बीच लाखों लोगों की जिंदगी में ईमानदार संघर्ष की शक्ल में उजाले, बहुत कमजोर ही सही मौजूद तो हैं। उजालों को पूरे तौर पर मिटा पाना शायद संभव भी नहीं हो पाए। कमजोर होती रोशनी का मतलब यह नहीं कि अंधेरे पूरी तरह जीत गए। इस तरह से सोचा जाए तो कुछ उम्मीद-सी बंधती नजर आती है। जिंदगी की लौ गहरी होती दिखाई देती है। कहीं रास्ते पर जिंदगी को चलाने की जिजीविषा दिखाई देती है। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। घुप्प अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी वह फर्क तो बताती है, जो रोशनी और अंधेरे में है। यह फर्क ही अंधेरे के खिलाफ लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण औजार बनता है। इसीलिए जितना कुछ उजाले की शक्ल में है, उसे भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में यही तो संबल है। जीवन-शक्ति है, जीवन की जिजीविषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जिजीविषा रहेगी, तो जीवन रहेगा। जीवन रहेगा तो उसे बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं रहेंगी। इसलिये लगातार गहराते अंधेरे में घिरकर उजालों को खत्म मानना व्यर्थ है।
जब तक रोशनी की एक किरण भी बाकी है, तब तक अंधेरों की पूरी विजय नहीं मानी जा सकती हैं। महाभारत में भी कहा है जब अन्धकार तमाम मुखौटे लगाकर भीतर घुस रहा हो तो दीये जलाने की कोशिश करो। माना कि कोई दीपाधार नहीं, तेल चुक गया, कोई बाती पूरना नहीं जानता, पूरने के लिये कहीं कपास नहीं, विश्वास नहीं, कैसे ज्योति जलेगी, तब भी दीये जलाने की कोशिश करो। सच्चाई को दीवट बनाओ, जो भी सच्चाई तुम्हारे भीतर है, उसी को गढ़-गूंथ कर सीधा-टेढ़ा दीवट बनाओ, अपने तप को तेल बनाओ, अपने नि:स्वार्थ या स्वार्थ परिश्रम को तल बनाओ, अपने भीतर कुछ न कुछ बची हुई संवेदना को बाती बनाओ और विश्वास करो कि तुम्हारी कर्म-वृत्ति ही तुम्हारी ज्योति होगी। किसी को शाप देने की जरुरत नहीं, किसी को कोसने की जरुरत नहीं, आक्रोश की आवश्यकता नहीं, अपनी सीमित सुरक्षा की चिन्ता नहीं। जो अन्धकार घिर रहा है और जैसी आंधी-पानी से हम त्रस्त होकर अपने घरों में अन्धकार के पहले ही घुस आए हैं आश्वस्त होकर उस स्थिति में यही दीया हमारा आलोक बनेगा।
हमने ऐसे दीये इतिहास में कई बार जलाये हैं और फिराक के शब्दों में इतिहास के खंडहरों में कुछ टूटे-से दीये रखे होंगे। उन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। ऐसी खंडहरी सम्पदा के देश, अब भी तुम दीये जला सकते हो। उठो, जाओ और बाती जलाओ।