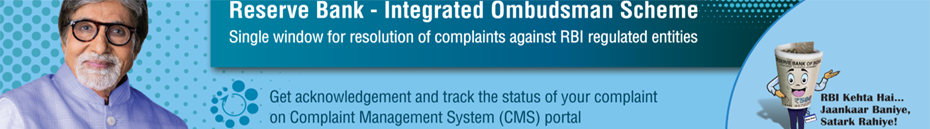दीपक गढ़े कुम्हार ने
श्रम न रचे अभंग
माटी जगमग हो गई
छू किरणों के अंग
देती गई दिवालियां
ऐसी भी सौगात
बिना पंख सपने उड़े
जैसे हाथों हाथ।
– दिनेश शुक्ल
माटी के दीप सा सोंधा उजियारा बिखरा रहे हैं ये दोहे। पता नहीं इस बरस की यह दीवाली सारी दुनियां को कौन से सौगात दे जायेगी। बारूद की महक से झुलसती मानवता आतंकवाद को नष्टï करने की प्रतिबद्वता। सारी दुनियां जैसे दु:स्वप्न में जी रही है।
चाहे जो हो। कुम्हार ने ”अपनी माटी’ के दिये गढ़ दिये हैं। खेतों से आए ताजे कपास की बोनी से बातियां बनाई जा रही है। घानी तो मर चुके हैं पर एक्सपेलर के तेल की धार जीवित है। महालक्ष्मी पर्व में दीपक जला कर ”तमस’ के पेट में प्रकाश का चीरा डालना है। तमस से लडऩे और प्रकाश की यात्रा का संकल्प लेने वाला यह भारतीय पर्व ”तमसो मा ज्योर्तिगमय’ की वैदिक रीतियों का आडम्बर रहित प्रतिबद्वता का त्यौहार है। अमीरों की अट्टालिकाओं में लटके हुये सतरंगी झालरों के बीच झुग्गी-झोपड़ी में जल रहे मिट्टी के अकेले-दुकेले दीप कभी शर्मिंदा नहीं होते बल्कि यह स्थापित करते हैं कि ”अंधेरे से लड़ाई का संकल्प’ उनके हिस्से का ”धर्मयुद्घ’ है। अट्टालिका के बाहर भीतर सजी-धजी महालक्ष्मी चारों ओर स्वयं को तलाशती हुई जब थक जाती है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि अंधेरे से लड़ाई का दौर तो कब का समाप्त हो चुका है। दूर कहीं झोंपड़ों में ”जिजी विशाम:’ लोगों के बीच माटी का दीपक जीवन के दैन्य और समाज में गहरे चीकट अंधेरे से युद्घरत दिखाई पड़ता हैं।
हमारे अपने गढ़े अंधेरों की कई-कई पर्तें हैं। हम अपने अंधेरों में कृत्रिम प्रकाश की झालरें टांग कर यह प्रदर्शित करने का दंभ भरते हैं कि हमने अंधेरे को पछाड़ दिया है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम अपने हाथों लाखों पर्त अंधेरों के रचते हैं। और उनके ऊपर रोशनी के झालर टांग कर एक कृत्रिम युद्घ में लग जाते हैं। अगर भूले से भी हमें मिट्टी का कोई दीपक दिख जाये और वह हमें जलते हुये मिल जाये तो, हममें उससे आंख मिलाने का साहस नहीं होता है। माटी के दीपक से तो वही आंख मिला सकेगा जिसकी जड़ें माटी में गहरे तक गई हों। अमरबेल की तरह रोशनी की झालरों में लटके हुये लोग बिजली के चकाचौंध अंधेरों के साथ मिलकर अमावस की लड़ाई में ”आतंकवादी’ की सी भूमिका गढ़ते दिखाई पड़ते हैं। धरती के भूगोल में जहॉं-जहां अंधेरा है, वहीं-वहीं रोटी, गरीबी और बीमारी से बिलबिलाते लोग दिखते हैं। धरती साफ-साफ दो फांकों में बंटी दृष्टिगोचर होती है। परंतु उसके ऊपर झालर डाल देने यह समझ नहीं आता कि किसकी लड़ाई किसके साथ है।
भूख से, गरीबी से, अशिक्षा से मारा जाने वाला आदमी ”आम आदमी’ होता है। वह चाहे अफगान हो, इराकी हो या कश्मीरी आवाम हो। गरीब और अशिक्षित दुनिया के आम आदमी की लड़ाई को ”वल्र्ड ट्रेड सेंटर’ के हादसे ने ”विश्व बाजार’ की लड़ाई बना दिया। बिन लादेन ने मुस्लिम समाज को अंधेरे की खाईयों में फेंककर अशिक्षित और गरीब बने रहने पर विवश किया। बदले की कार्यवाही को ”जिहाद’ बताकर उन्माद में बदल दिया। इन अंधेरों को गहरा करने के लिये यूरोप के बाजार आसमान पर छा गये।
भारत में एक नये तरह का अंधेरा है। ”महालक्ष्मी’ की पूजा धान की बालियों से करने वाले किसान शायद ”गरीबी की पूजा करते चले आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में ”सुरहुत्ती देवारी’ के रूप में मनाये जाने वाली दीपावली को ”काछन चढऩे’ वाले हैं। मड़ई बाजारों में रौनक आने लगी है। गेंदे के गोल-गोल मोदक जैसे फूल ”राउताही’ के लिये ”सम्हर’ रहे ग्वाले की पगड़ी पर मटक रहे हैं। पैर के घुंघरू और कमर तथा बाजूबंद में गुथें कौडियों के माले कभी-कभी, लाठी कभी खांडे के साथ ताल मिलाते हैं। धान के पके खेतों की मेड़ों पर, मड़ई मेले की छाती पर, निर्दोष उत्साह और यौन चपलता से सराबोर उछलता कूदता छत्तीसगढ़ का यह ”देवारी सौंदर्य’ कहीं बिला न जाये आज के तुगलकी अंदाज में।
”सुरहुत्ती देवारी’ यही कहते हैं छत्तीसगढ़ में दीपावली के पर्व को। भाषा विज्ञान का जानकार, तो नहीं हंू परंतु बचपन से, जबसे इस ‘शब्द’ से परिचय हुआ है, इन दो शब्दों के पीछे, जलती-बुझती टिमटिमाती रोशनी की कतार मुझे दिखती है। दूसरे क्या अनुभव करते हैं, मैं नहीं जानता। ”सुरहत्ती देवारी’ का आना, जैसे गांव-गंवई की गलियों में कीचड़ का सूख जाना। बरसात में टूटे भहराये, उखड़ी-पुखड़ी दीवालों पर मिट्टी, जिसे जो मिला, पोतकर दीवाल को नया करने में लग गये। दरवाजों पर अरण्डी या नीम का तेल चढ़ा दिया। घर के भीतर गरीबी तो है पर खेतों में धान की बालियां, बरछे में गन्ने की कलगी, बाड़ी में अभी-अभी उग रहे, ”साग-भाजी’ का तरोताजा सौन्दर्य, सब मिल कर गरीबी के मलिन चेहरे पर संतोष और मुस्कान का छिड़काव कर जाते हैं। लक्ष्मी के ड्योढ़ी तक आने में देरी है। वह अभी ”खेत-खारÓÓ को अपना दुलार दे रही है। आश्विन की क्वांरी हवा झपाटे से कूदती-फांदती गांव के किनारे तक आती है। और किशोर-किशोरियों के गाल थपथपा कर फिर कछार की ओर भाग लेती है। गेंदे के गोल-गोल पीले-पीले फूल आंगन में मुस्काने लगे हैं। बरसात में बियाई बछिया, गली में अपने बछड़े को देर तक पुचकारती है। तालाबों का जल शांत हो गया है और पानी में डूब गये कमल के, नये पत्ते, नये फूल खिलने लगे हैं। शीत आने के पहले थोड़ा गदरा लें, फिर गल जायेंगे।
”सुरहुत्ती देवारी’ आने का अर्थ है, दोनों समय भोजन बनने की आशा। दशहरा के दिन माई के चौरे पर नये अनाज का भात बना और गांव भर में प्रसाद बंटा। मां के प्रसाद के बाद भला भूख का जोर चलने वाला है। अधपके धान की बालियों की ”चिरैया’ घर के आंगन की दीवाल पर लटका दिये हैं। चिडिय़ां आ कर चुग-चुग जाती हैं। पहले चिरई-चुरगुन अपना पेट भर लें, फिर किसान की बारी।
एक झूला बनाया है कुमारी और सौभागिनी बालांयें उसमें एक मिट्टी का बना तोता बैठाती हैं। झूले के चारों ओर गोल बनाकर ताली दे-दे कर गा रही हैं। मिट्टी का तोता जिसे यहां ”सुवा’ कहते हैं, वह ”नारी पीड़ा’ का साक्षी पक्षी है।
”सुरहुत्ती देवारी आगे
मोर सुवा ना
कब सुनबे मोरे जी के
पीर
रे सुवना कब सुनबे
मोरे जी के पीर’
बरसात बज्र की तरह था। खेती-पाती बिगड़ जाने के कारण मरद काम धंधे की तलाश में परदेश चले गये थे। कह गये थे फसल कटने के समय, ”सुरहुत्ती देवारी’ तक लौट आयेंगे। बच्चे औरत बुढ्ढे सब अपने-अपने ढंग से रास्ता निहार रहे हैं। चार पैसे लेकर आयेंगे तो ”देवारी’ के दीप जलेंगे। मन में बिछोह की पीड़ा और गीतों में मिलने की उत्कंठा है-”सुवा’ झूले में झूल-झूल कर नारी मन की पीड़ा का साक्षी बना है। गीत में आता है ”सुवना तिरिया जनम झन दे’ । पीड़ा से व्याकुल बाला अपने स्त्री जन्म को कोसती है। सारा जीवन बिछोह की पीड़ा झेलते गुजरता है।
गांव के जीवन में बिछोह और पीड़ा स्थायी भाव है। भूख और गरीबी तो है ही, बिछोह और पीड़ा उनके संगी है। ईंट भट्ठों में ईंट बनाता मजदूर या शहर की सड़कों पर रिक्शा ठेला खींचता, श्रमिक, उनकी आंखों के पीछे छोटा सा गांव होता है और पैरों पर शहर की पथरीली सड़कें। गांव की माटी रात दिन, तीज त्यौहारों में आने वाले अपने लाड़लों के स्वागत करने पंथ निहारा करती है। सुवा, बिरही बालाओं की पीड़ा को सुनता है। खेत-खार पोखर सब सज-धज कर स्वागत की तैयारी में लग गये हैं। ”सुरहत्ती देवारी’ के रूप में आये या ”दिया-दियारी’ के रूप में आये, लक्ष्मी का यह त्यौहार शहरों में भारी-भरकम कृत्रिम सज-धज के साथ आता है। इसका आगमन इतना खर्चीला होता है कि अच्छे से अच्छा खाता-पीता आदमी अपने को कंगाल महसूस करने लगता है। वर्षों पहले प्रेमचंद जी ने जिस ”महाजनी सभ्यता’ पर अपना लेख लिखा था, वह लेख बरबस बारबार याद आता है। सजी-धजी दुकानों और सामानों का अम्बार लुभाता है और हमें अपनी कंगाली का बेहूदा आभास कराता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें कतई आवश्यकता नहीं, वे हमारे जीवन के लिये जरूरी लगने लगती है। यह भी अहसास होता है कि इनके बिना हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व ही व्यर्थ है।
दो प्रकार के अहसास हैं। एक यह कि मैं अपने घर में हं। खाने-पीने की कमी नहीं है। मध्यम किस्म का सम्मानित जीवन जी रहा हंू परंतु दीपावली के समय सड़क पर निकलंू तो अपने और अपने रहन-सहन को कंगाल महसूस करूॅ। मेरी हैसियत बनाने के लिये मुझे बहुत कुछ करना होगा। सौ पचास पैकेट मेवे बांटने होंगे। छपे हुए दन्नाटेदार शुभकामना पत्र भेजने होंगे। जरूरी न हो तो भी घर में धनतेरस को अंट-संट सामान खरीद कर लाना होगा। पेट में पचाने की शक्ति नहीं है फिर भी मिठाई खाने-खिलाने के रस्म करने होंगे। कपड़े चाहे जरूरी न हो पर घर में सबके लिये कुछ नये कपड़े तो आने ही चाहिये। बच्चों को दीवाली का मजा फटाकों के बिना कहॉं आता है। मित्रों के बीच स्थापित होने और अपने को विशिष्टï बताने का समय तो यही होता है। पर मेरी हैसियत ऐसी नहीं है। पिछले दस वर्षों से अनुभव कर रहा हंूॅ कि मैं अपने मित्रों के बीच ”दीपावली’ के समय कदम मिला कर चल नहीं पा रहा हॅंू। वे नव धनाढ्य हैं। ठेकों और ट्रान्सफर उद्योग आदि से अपार धन के स्वामी बन गये हैं। उन्हें दीवाली पर सराफ से लेकर हलवाई तक की दुकान पर जाना है, परंतु हम है कि प्रगति के दौर में अपनी प्रतिभा की सीमा में बंधे हैं। यह एहसास त्यौहारों पर घर के परिजन अवश्य करा देते हैं। मित्र भी महसूस करते हैं कि यह आदमी समय की रफ्तार में बिल्कुल अनफिट है।
यह उपलिब्ध है, मेरे शहर में होने की। दूसरा एहसास है, गांव का, घर में सब खाली हैं, पर लक्ष्मी आने वाली है, यह एहसास ही दीवाली है। यह उम्मीद, यह आशा, जो टिमटिमा रही है, खेतों में, कछारों में, यह सुरहुत्ती की तरह ”बंग-बंग’ जलने वाला एहसास ही दीवाली है, मेरे गांवों की। कुछ नहीं है, पर उम्मीद की मस्ती में भर कर ”रावत नाचा’ हो रहा है। गांव के चरवाहे और यादव सज-धज कर गेंदे के फूल गजरे से सजे-धजे नाच रहे हैं। ”मातर जगा’ हो रहा है। फिर ”मड़ई’ होगी। किसान के घर जा कर असीसेगे-
”जुग-जुग जिवै तोरे नाती पोता
भरे धान तोर कोठी,
लक्ष्मी ले तोर कोठा संवरै
दूध घीव अउ रोटी’
इन असीसों से भरे, मुहावरों से भरे गीतों से भरे, नाचते-गाते लोगों के बीच गांव में जो दीवाली आती है उसका यह जीवंत एहसास। क्या हुआ घर में कुछ नहीं है तो,? फलने-फूलने और लंबी उम्र जीने का आशीष तो है। इन आशीषों से सारा दु:ख दूर हो जाता है। सारी गरीबी दूर हो जाती है।
आत्मीय अनुभवों का खजाना लेकर जब दीवाली आती है गांवों में तो, मेरा मन शहर की गलियों में कंगाल की तरह भटकने लगता है और छटपटाता है गांव की ओर जाने के लिये। क्या करूंॅ मैं अपने ग्रामीण परिवेश में उन अनुभवों का, जिन्हें गांव में महसूसा है। गांव में सांप बिच्छू है, गांव में संक्रामक बीमारियां हैं, गांव में अशिक्षा है, गांव में अभाव है। इस सब के बावजूद गांव के लोग गांव में ही संतुष्ट हैं। वे शहर में बसना नहीं चाहते। रोजगार के लिये जाना उनकी मजबूरी है। शहर में जीते हुये, वे अपने अधूरेपन की पीड़ा लगातार भोगते हैं यह एहसास तो गांव का उजड़ा हुआ कोई ”आदमीÓÓ ही करेगा। तमाम बातों के बावजूद लोकगीत, गांव के तीज त्यौहार, गांव के रिश्ते-नाते, गांव के खेत-खलिहान, गांव के नदी पोखर, गांव का अछूता सौन्दर्य झूठा नहीं हो जाता। तमाम प्रदूषण के बाद भी गांव, गांव है और उसकी मौलिकता समाप्त नहीं हो जाती।
”सुरहुत्ती देवारी’ के कंधों पर बैठकर आये, चाहे लाला जी की नई पोथियों पर पधारे या साहबों के मंहगे मिठाई मेवों के पैकैटों में सजे। इतना तय है कि दीवाली के दिन ”लक्ष्मीÓÓ जी दरवाजे-दरवाजे दस्तक देती है। आपके मेरे दरवाजे भी आयेंगी और जरूर आयेंगी।